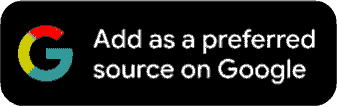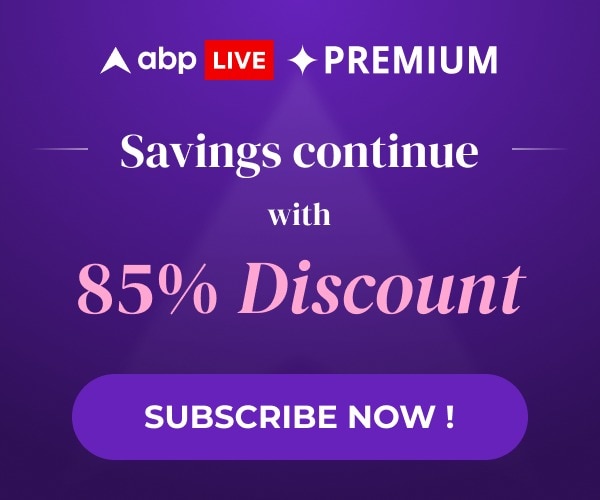एक महाशक्ति का अपमानजनक अंत : रन, अमेरिका, रन

द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर जापान, जर्मनी और इटली को हराने वाले अमेरिका ने उसके बाद कोई युद्ध या लड़ाई नहीं जीती. कोरिया और वियतनाम के बाद मध्यपूर्व में भी कोई स्पष्ट नतीजे नहीं आए. अमेरिका ने कदम वापस खींचे. अब वह अफगानिस्तान से भी लड़खड़ाते हुए लौटा है. लेकिन इससे चीन को क्या कोई सबक मिलता है?
अफगानिस्तान तालिबानियों के हाथों में पहुंच चुका है और अमेरिका अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए लड़खड़ा रहा है. न्यूयॉर्क टाइम्स में लगी हेडलाइन यह बात चीख-चीख कर कह रही है और इसकी गवाही टेलीविजन और मोबाइल फोन की स्क्रीन पर उभरने-चमकने वाली तस्वीरें भी दे रही हैं. अमेरिकी कैसे अपनी दुम पैरों के बीच दबा कर भाग रहे हैं! संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन टेलीविजन पर बाइडेन प्रशासन द्वारा अचानक वहां से अपनी फौजों को वापस बुलाने के फैसले का बचाव कर रहे थे और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही, वह थीः यह साफ तौर पर साइगॉन नहीं है. उन्होंने लोगों की स्मृति से उस सुस्पष्ट तथ्य को अलगाने का जोरदार प्रयास किया, जिसमें दर्ज है कि अमेरिका को 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम में अपमानित होना पड़ था, जब वियतनामी सेना ने वहां कब्जा कर लिया था और अमेरिका ने साइगॉन शहर से अपने दूतावास के कर्मचारियो को निकालने की मांग की थी. उसकी तब की शक्ति का अंदाजा इस तथ्य से हो जाता है.
आज फिर वही ऐतिहासिक तस्वीरें हैं, जब अमेरिका का खेल खत्म हो गया है और उसके हेलीकॉप्टर अपने लोगों और दुश्मनों के अनुसार ‘सहयोगियों’ को वहां से निकालने की उड़ानें भर रहे हैं. वे उन्हें हवाई अड्डे के उन सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे हैं, जहां की परिधि में अमेरिकी रक्षा सेनाएं अभी तैनात हैं. तब दुश्मन दुष्ट कम्युनिस्ट थे और आज ये खूंखार इस्लामी आतंकी हैं. मगर यह अमेरिका है, जो एक बार फिर अफरातफरी के स्थल से भाग रहा है. उस अराजकता से, जो उसने खुद पैदा की थी.
द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद प्रतिष्ठित सैन्य महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका को एक और जबर्दस्त हार मिली है. हमें इस नकारात्मकता को छोटा करके नहीं देखना है. कई जानकार इस जोर के झटके को धीरे-से लगा बताने में लगे हैं. कुछ इसे मात्र ‘शर्मनाक’ बता रहे हैं और बाकी कह रहे हैं कि यह अमेरिकी ‘प्रतिष्ठा’ को लगा धक्का है. कुछ का कहना है कि यह असल में अमेरिकी सेना की नाकामी है. यह सब कुछ सही है लेकिन बात इससे भी आगे जाती है कि यह अफगानिस्तान में अमेरिकी युग की समाप्ति भर नहीं है. यह कहना पर्याप्त नहीं होगा कि अमेरिकी वहां से निकलने को प्रतिबद्ध थे और बाइडेन तथा उनके सलाहकार यह सही अनुमान नहीं लगा पाए कि अफगानी सेनाएं आखिर कब तक तालिबान को टक्कर दे पाएंगी.
इस नजरिये से देखें तो वर्तमान ‘मान-भंग’ की जिम्मेदारी रणनीतिक सोच की नाकामी और बाइडेन के पूर्ववर्ती प्रशासकों की नीतियों के कार्यान्वयन में विफल रहने की बनती है, हालांकि अनेक अमेरिकी इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि ऐसे में ‘खरबों डॉलर’ वहां क्यों नष्ट कर दिए गए. बीते 20 साल में लड़े गए युद्ध की यह कीमत बताई जा रही है, जिसमें विशाल अमेरिकी सेना की गतिविधियों के खर्च के साथ एक देश को बनाने की कोशिशें शामिल हैं. ऐसे देश को बनाने की कोशिशें जिसे आतंक से मुक्त करके असभ्य-कबीलाई स्तर से ऊपर उठ कर ‘स्वतंत्र राष्ट्र’ बनाया जा सके. यह विचार अपने आप में सैन्यवादी संस्कृति के संपूर्ण अज्ञान को दर्शाता है. सैन्यवादी संस्कृति बर्बरता का ही रूप है, जो अमेरिकी विदेश नीति के साथ उसके आजादी के लिए कथित प्यार वाले चरित्र में भी अंतरनिहित है.
क्रूर सत्य तो यही है कि द्वितीय विश्ययुद्ध में अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों द्वारा जापान, जर्मनी और इटली की फासिस्ट शक्तियों पर विजय के बाद यूएस ने कोई सीधा युद्ध नहीं जीता. कोई छोटी लड़ाई तक नहीं जीती. कोरियाई युद्ध (जून 1950-जुलाई 1953) एक गतिरोध पर खत्म हुआ, जिसमें शस्त्रों को लेकर संधि हुई और इसके कड़वे नतीजे आज तक सामने आ रहे हैं. वियतनाम में अमेरिकियों को लगा कि उन्हें वह ‘जिम्मेदारी’ लेनी चाहिए, जिसे फ्रेंच तेजी से बढ़ते कम्युनिस्ट खतरे के विरुद्ध ज्यादा समय तक नहीं निभा पाएंगे. फिर दो दशक बाद, जिसे इराक में उन्होंने एक जोखिमविहीन झंझट मात्र समझते हुए सद्दाम हुसैन को अपदस्थ करने के लिए बम गिराए थे, वह कुछ वर्षों तक खिंचा और अंततः इराकी तानाशाह को हकीकत में एक गड्डे से बाहर खींच कर निकालते हुए उसे फांसी के तख्ते तक उन्होंने पहुंचाया.
मगर पूरी प्रक्रिया में इस देश को उन्होंने न केवल खंडहर में तब्दील कर दिया बल्कि वहां लोकतांत्रिक सुधारों को लागू करने की महत्वाकांक्षा में पूरे पश्चिमी एशिया (या फिर मध्य पूर्व) को प्रभावित किया. जबकि उन्हें खुद अपने देश में लोकतांत्रिक सुधारों के लिए बहुत कुछ करना है, जहां श्वेतों में श्रेष्ठता भाव और विदेशियों को नापसंद करने वाले हथियारवादी संगठन खुली आंखों से दिखाई देते हैं. उधर, सीरिया में पश्चिम में पढ़े-लिखे बशर अल-असर के अत्याचारों के आगे सद्दाम हुसैन की इराक में करतूतें छोटी दिखाई देती हैं. लीबिया में गृहयुद्ध जारी है. अमेरिका ने इस बीच लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी को धराशायी कर दिया लेकिन इसका खामियाजा अमेरिकी विदेश नीति को भुगतना पड़ा. इस गड़बड़ी भरे पूरे प्रकरण में भले ही रूस और सऊदी अरब की भूमिका भी रही हो, लेकिन जो हुआ उसमें अरब विश्व पूरी तरह उलझ गया है.
अब, इस सबके अंत में यह बीस साल की कहानी है जिसमें अमेरिकी सैनिक देखत-देखते कुछ ही दिनों में शस्त्र कबाइलियों के सामने हथियार डाल रहे हैं. कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि अमेरिका ने शीत युद्ध जीत लिया हैः अगर सोवियत संघ के विघटन के तीस साल बाद ऐसा हो गया है तो यह एक सार्थक सवाल है कि ‘गर्म’ युद्ध को जीतने के बजाय ‘ठंडा’ युद्ध जीतने के क्या निहितार्थ हो सकते हैं.
अब एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सैन्य शक्ति, भले ही वह कितनी ही भारी-भरकम क्यों न हो, उसकी अपनी सीमाएं होती हैं और निश्चित ही उसका एक दायित्व भी होता है. इस प्रकरण में दूसरों के सीखने के लिए भी सबक हैं, खास तौर पर चीन के लिए. किसी को भी इतिहासकारों द्वारा अक्सर प्रेम से और कभी बहुत उम्मीद भरे स्वर में कही जाने वाली ‘इतिहास के सबक’ की बात को कम नहीं आंकना चाहिए. अमेरिकी कभी भी अपनी सैन्य पराजय को पूरी तरह स्वीकार नहीं करेंगे और उनके मिलिस्ट्री जनरल केवल यही सबक लेंगे कि भविष्य में कभी अपना एक हाथ पीछे बांध कर युद्ध के मैदान में नहीं उतरेंगे. भविष्य में उनके आतंकवाद विरोधी अभियानों का फोकस इस बात पर होगा कि वे किस तरह गुरिल्ला युद्ध लड़ते हैं. ऐसे गुरिल्ला, जिन्हें कोई राष्ट्र अपना नहीं मानता. अल-कायदा, तालिबान, आईएसआईएस और अन्य जेहादी संगठनों के विरुद्ध जंग की कहानियों में यह तत्व शामिल था. मगर इन सब बातों में यह तथ्य कहीं रेखांकित नहीं हो सकता कि भारी सैन्य शक्ति अनिवार्य रूप से लाभदायक ही साबित होती है. जैसा कि कभी हुआ करता था.
कोरिया, वियतनाम, इराक और अफगानिस्तान के विरुद्ध अमेरिका के युद्धों के बरक्स जर्मनी पर अमेरिका की जीत में कभी यह बात साफ तौर पर नहीं बताई गई कि दोनों की संस्कृति समान थी. वे दुनिया में ‘पश्चिमी संस्कृति’ के झंडाबरदार थे. इसका साफ आशय है कि अमेरिकी सेनाएं जर्मनी के सामने या जर्मनी में अजनबी या पराई नहीं थी. यही बात अफगानिस्तान में तालिबान पर लागू थी. सामान्य अफगानों द्वारा तालिबान को नापसंद करने को लेकर पश्चिमी मीडिया में बहुत कुछ प्रकाशित होता रहा. मगर तालिबान जोर देता रहा कि अफगानिस्तान में पश्तूनों, ताजिक, हाजरा, उज्बेकों और अन्य जातिय समूहों के बीच मतभेदों के बावजूद उनकी संस्कृति एक ही है. यह बात वहां के असंख्य जातिय समूहों और राजनीतिक पार्टियों के लिए सदा अमेरिका के विरुद्ध केंद्रबिंदु बनी रही. तालिबान की वापसी के बाद वहां की राजनीति, विदेश नीति, भौगोलिक रस्साकशी, सैन्य रणनीति और ऐसी बातों का आकलन ही पर्याप्त नहीं है. उसे लेकर विचार करने की कई अन्य बातें भी हैं, जिन पर मैं बाद में विस्तार से लिखूंगा.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)