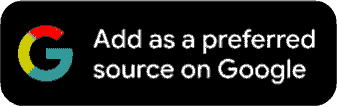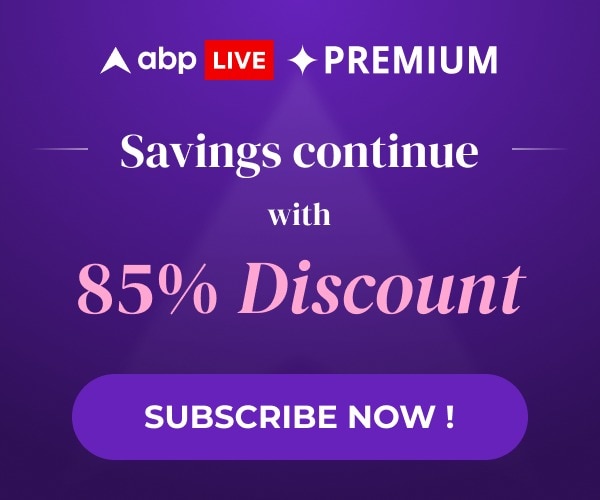Opinion: जाति का फेर और राजनीतिक दाँव-पेच, बिहार में कब बहेगी विकास की धारा, बदहाली की ज़िम्मेदारी है किसकी

बिहार, भारत के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक है या कहें सबसे पिछड़ा राज्य ही है. यह टैग वर्षों से बिहार के साथ जुड़ा है. पिछले सात दशक में बिहार में तमाम राजनीतिक दलों की सरकारें आयीं. सरकारें बदलती रहीं. तमाम नये नेताओं ने बतौर मुख्यमंत्री प्रदेश के शासन व्यवस्था की कमान संभाली. सब कुछ बदला, लेकिन बिहार की किस्मत नहीं बदली.
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में राजनीति का ढर्रा कमोबेश वैसा का वैसा ही रहा है. पिछले सात दशक में देश के दूसरे राज्यों में राजनीतिक का ढर्रा समय, तकनीक और ज़रूरत के हिसाब से बदलते रहा है. इसकी वज्ह से कम या ज़ियादा बाक़ी राज्यों में विकास की एक समानांतर धारा भी समय के हिसाब से बहती रही है.
बिहार में जाति आधारित राजनीति
इसके विपरीत, बिहार में राजनीति अभी भी घूम-फिरकर उसी ढर्रे पर की जा रही है, जैसा दशकों पहले से होता आ रहा है. वो ढर्रा है, पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर आधारित राजनीति. बिहार की सत्ता में हमेशा ही बदलाव तब हुआ है, जब किसी पार्टी या नेता ने जातिगत हिसाब-किताब से जुड़े समीकरणों को अपने पक्ष में कर लिया हो. बिना किसी लाग-लपेट के यह कहा जा सकता है कि पूरे देश में बिहार एक ऐसा प्रदेश है, जहाँ की राजनीति पर जाति सबसे ज़ियादा हावी रही है. बाक़ी राज्यों में भी राजनीति पर जाति का प्रभाव दशकों से देखा जाता रहा है, लेकिन जिस हद तक बिहार में पूरी-की-पूरी राजनीति ही जाति के इर्दि-गिर्द घूमते रही है, वैसा किसी और प्रदेश में नहीं हुआ है.
विकास के पैमाने पर सबसे नीचे बिहार
राजनीति पर जाति के इस कदर हावी होने का ही नतीजा है कि बिहार विकास के पैमाने पर लगातार पिछड़ते चला गया. यह लोकतंत्र की सच्चाई है कि जहाँ भी जातिगत राजनीति का सबसे ज़ियादा बोल-बाला रहेगा, उस प्रदेश को ख़म्याज़ा के तौर पर विकास की बलि देनी ही होगी. बिहार के साथ यही होता आया है और जो हालात पिछले कुछ महीने से बने हैं, भविष्य में भी इसके बदस्तूर जारी रहने की पूरी गुंजाइश है.
जब राजनीतिक रोटियाँ जातिगत आग पर अच्छी तरह से पकती रहती हैं, तो फिर विकास की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है. इसका जीता-जागता सबूत बिहार है. जाति के समीकरणों को साधने के लिए जातिगत भावनाओं को हमेशा चर्चा का विषय बने रहना बेहद ज़रूरी है. बिहार के तमाम बड़े-बड़े नेता इस बात को भलीभांति जानते थे या जानते हैं. इतिहास गवाह है कि दशकों से बिहार में हर पार्टी के नेताओं ने बड़े स्तर पर इस काम को ब-ख़ूबी अंजाम दिया है.
80 के दशक तक कांग्रेस का दबदबा
बिहार की राजनीति पर एक समय या कहें 80 के दशक तक कांग्रेस का दबदबा था. बीच-बीच में जन क्रांति दल, शोषित दल, सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी की सरकार भी चंद दिनों या चंद महीनों के लिए रही हैं. संविधान लागू होने के बाद हुए पहले विधान सभा चुनाव से ही कांग्रेस ने बिहार में तथाकथित अगड़ी जाति को अपना सबसे बड़ा मोहरा बनाया.
बिहार में कांग्रेस से जो मुख्यमंत्री हुए हैं, उनके नाम पर ग़ौर करते हैं. बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिन्हा थे, जो आज़ादी के बाद से 31 जनवरी 1961 तक इस पद की ज़िम्मेदारी संभाली. उनके अलावा कांग्रेस से दीप नारायण सिंह, बिनोदानंद झा, कृष्ण बल्लभ सहाय, भोला पासवान शास्त्री, हरिहर सिंह, दारोगा प्रसाद राय, केदार पांडे, अब्दुल गफूर, जगन्नाथ मिश्र, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येन्द्र नारायण सिन्हा अलग-अलग समय पर मुख्यमंत्री बने. भोला पासवान शास्त्री तीन बार और जगन्नाथ मिश्र भी तान बार मुख्यमंत्री बने. जगन्नाथ मिश्र बतौर कांग्रेस नेता आख़िरी मुख्यमंत्री थे. उनका आख़िरी कार्यकाल 6 दिसंबर 1989 से 10 मार्च 1990 था. उसके बाद बतौर जनता दल नेता लालू प्रसाद यादव प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं.
1990 तक अगड़ी जातियों का दबदबा
कांग्रेस की ओर से बने मुख्यमंत्रियों के नाम पर ध्यान दें, तो अधिकांश अगड़ी जाति से आने वाले नेता थे. जब तक बिहार की राजनीति पर अगड़ी जाति का दबदबा क़ायम रहा, कांग्रेस की सत्ता भी कमोबेश बरक़रार रही. यह वो दौर था जब बिहार में चुनाव मतलब हिंसा और बूथ क़ब्ज़ा हुआ करता था. उस ज़माने में बिहार में अगड़ी जातियों के ख़ौफ़ की वज्ह से कई इलाकों में पिछड़े वर्ग के लोग बूथ तक नहीं पहुँच पाते थे. कांग्रेस अगड़ी जातियों को अपने साथ बनाए रखने में कामयाब होते रही. कुछ वर्ष को छोड़ दें, तो इस रणनीति के माध्यम से कांग्रेस 80 के दशक तक विकास की अविरल धारा बहाए बिना बे-ख़ौफ़ बिहार की सत्ता पर विराजमान रही.
बीच-बीच में जन क्रांति दल, शोषित दल, सोशलिस्ट पार्टी और जनता पार्टी की भी सरकार आयी. महामाया प्रसाद सिन्हा की अगुवाई में मार्च 1967 से जनवरी 1968 के बीच क़रीब 11 महीने जन क्रांति दल की सरकार रही. फिर 28 जनवरी 1968 से 22 मार्च 1998 के बीच तक़रीबन दो महीने शोषित दल की सरकार रही, जिसमें 5 दिन के लिए सतीश प्रसाद सिंह और बाक़ी बचे दिनों में बी.पी. मंडल (बिंधेश्वरी प्रसाद मंडल) मुख्यमंत्री रहे. यही बाद में मंडल कमीशन के अध्यक्ष भी बने थे. फिर बिहार में 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 के बीच 163 दिन सोशलिस्ट पार्टी की सरकार रही, जिसमें कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री रहे. बिहार में 24 जून 1977 से 17 फरवरी 1980 के बीच तक जनता पार्टी की सरकार रही, जिस दौरान अलग-अलग समय पर कर्पूरी ठाकुर और राम सुंदर दास मुख्यमंत्री रहे.
1990 के दशक तक कांग्रेस के दबदबे वाली अवधि के दौरान जो बीच-बीच में कुछ महीनों या साल के लिए दूसरे दलों की सरकार रही, उसका आधार भी कमोबेश जातिगत समीकरण ही रहा था. हालाँकि उस दौरान अगड़ी जातियों के प्रभाव की वज्ह से इनका कार्यकाल बेहद ही सीमित रहा.
1990 से जातिगत समीकरणों का नया कलेवर
बिहार की राजनीति में 80 के दशक से तीन नेताओं का प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ने लगता है. ये नाम हैं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राम विलास पासवान. तीनों ही जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से निकले नेता माने जाते हैं. तीनों नेताओं ने राजनीति की शुरूआत सामाजिक न्याय और प्रदेश में अगड़ी जातियों के वर्चस्व को चुनौती देने के नाम पर शुरू किया था. क़रीब दो दशक तक ये तीनों नेता एक ही दल में रहे. जनता दल..इन तीनों नेताओं का मुख्य आधार रहा. बिहार में इन तीनों ने मिलकर कांग्रेस की राजनीति को चुनौती देने का मन बनाया. व्यवहार के धरातल पर यह तभी संभव था, जब प्रदेश की राजनीति में अगड़ी जातियों के प्रभुत्व को नेस्तनाबूद किया जा सके.
इसके लिए लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और राम विलास पासवान ने बिहार में अगड़ी जाति बनाम पिछड़ी जाति की लड़ाई को हवा दी. लालू यादव के लिए यादव तबक़ा, नीतीश कुमार के लिए कुर्मी-कोइरी और राम विलास पासवान के लिए पासवान समुदाय कोर वोट बैंक बन गया. अगड़ा बनाम पिछड़ा के समीकरण को साधते हुए फरवरी 1990 में हुए विधान सभा चुनाव में जीत हासिल कर जनता दल ने कांग्रेस को प्रदेश की सत्ता से बेदख़ल कर दिया.
जाति को साधकर सत्ता पर नज़र
इसके साथ ही बिहार में जातिगत राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया. इसका स्वरूप चुनाव दर चुनाव बदलता रहा, लेकिन सत्ता पर आसीन होने के मूलमंत्र का आधार जाति ही रहा. नीतीश कुमार ने 1994 में लालू प्रसाद यादव से राह अलग कर ली. लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर जुलाई 1997 में राष्ट्रीय जनता दल या'नी आरजेडी की रखी. नीतीश कुमार के नेतृत्व में समता पार्टी और बाद में जनता दल यूनाइटेड या'नी जेडीयू ने बिहार की राजनीति में प्रभाव बढ़ावा शुरू किया. वहीं राम विलास पासवान ने भी दुसाध समुदाय को कोर वोट बैंक बनाते हुए नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी या'नी एलजेपी के ज़रिये अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को साधने में जुट गये. तब से लेकर अब तक एलजेपी का वोट बैंक इस तबक़े से आगे नहीं बढ़ पाया है.
लालू प्रसाद ने यादव समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ तब़के के साथ ही दलित और मुस्लिम वोट बैंक को अपना आधार बनाकर लगातार 1990 से 2005 के बीच लगातार डेढ़ दशक तक अपने परिवार को बिहार की सत्ता का मुखिया बनाकर रखा. नीतीश कुमार की राजनीति कुर्मी-कोइरी के आधार वोट बैंक के साथ ही बीजेपी से गठजोड़ की वज्ह से फलने-फूलने लगी.
बिहार में बीजेपी की राजनीति के फलने-फूलने का मुख्य कारण कांग्रेस का कमज़ोर होना रहा. प्रदेश में तथाकथित अगड़ी जातियों का कांग्रेस से मोहभंग हुआ. उनमें से अधिकांश धीरे-धीरे बीजेपी के समर्थक बनते गये. यह परिपाटी विधान सभा चुनाव के नज़रिये अभी भी जारी है.
विकास की जगह जातिगत समीकरणों पर ध्यान
नीतीश कुमार ने 2005 में बीजेपी के साथ मिलकर आरजेडी के जातीय समर्थन का तोड़ निकाल लिया. उसके साथ ही प्रदेश में जेडीयू युग की शुरूआत होती है, जो बदस्तूर अभी तक जारी है. इसमें नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता और प्रदेश के राजनीतिक हालात का बड़ा योगदान रहा है. नीतीश कुमार की राजनीतिक दूरदर्शिता कोई उनका अपना कौशल नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से जातिगत समीकरणों पर आधारित दूरदर्शिता है.
बिहार की राजनीति में एक विडंबना या कहें विरोधाभास है, जिसका नीतीश भरपूर लाभ उठाते रहे हैं. प्रदेश में कांग्रेस बेहद कमज़ोर स्थिति में है, तो उसकी बात करनी बेमानी है. दरअसल बिहार में पिछले 33 साल से राजनीति की तीम मुख्य धुरी रही है. लालू प्रसाद यादव परिवार, नीतीश कुमार और तीसरी धुरी बीजेपी है. बाक़ी चाहे राम विलास पासवान की पार्टी हो या कोई और छोटी-मोटी पार्टी, इन सबका अस्तित्व सहायक के तौर पर ही रहा है और ये किसी पाले में जाकर ही थोड़ा बहुत कुछ करने का माद्दा रखते हैं. अतीत और वर्तमान में जो हालात रहे हैं और हैं, उसमें तो आरजेडी और बीजेपी के बीच गठजोड़ होने की संभावना कभी नहीं रही. दूसरी ओर नीतीश कुमार पाला बदलने की राजनीतिक दूरदर्शिता में माहिर रहे हैं. वे आरजेडी में भी जा सकते हैं और बीजेपी का दामन भी थाम सकते हैं, पिछले 18 साल का अनुभव यही कहता है.
सत्ता के लिए पाला बदलते रहे हैं नीतीश कुमार
नीतीश कुमार क़रीब 18 साल से बिहार की राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं. उसका कारण यह है कि उन्हें भलीभांति पता है कि बीजेपी-आरजेडी एक साथ नहीं आ सकते हैं. इस परिस्थिति का लाभ उठाकर वे बार-बार पाला बदलते रहते हैं, कम सीट लाने के बावजूद मुख्यमंत्री बने रहने की शर्त को मनवाते आए हैं. 2005 से जब-जब नीतीश कुमार को लगा है कि उनके हाथ से सत्ता फिसल सकती है, अचानक ही वे पाला बदल लेते हैं. पिछले एक दशक में हम यह बार-बार होते देख चुके हैं. 2005 से ही यह तय है कि बिहार की राजनीति में न तो आरजेडी, न ही जेडीयू और न ही बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाने की हैसियत में हैं. भविष्य में ऐसा हो जाए, उसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन फ़िलहाल यही स्थिति है.
अकेले दम पर जेडीयू की राजनीतिक हैसियत कम
राजनीति पर जाति के पूरी तरह से हावी होने का ही असर है कि बिहार में दो तरह की संभावना या गठबंधन बन जाने पर उस गठबंधन को हराना बेहद मुश्किल हो जाता है. या तो जेडीयू-बीजेपी एक पाले में या फिर जेडीयू-आरजेडी एक पाले में हो. इन दोनों में से कोई भी एक हो गया, तो फिर जीत उसी गठबंधन की होगी. अक्टूबर 2005 से जितने भी चुनाव हुए हैं, ऐसा होते हुए हमने देखा है. चाहे विधान सभा चुनाव हो या फिर लोक सभा सभी चुनाव, यह समीकरण काम करते हुए दिखा है. 2005 और 2010 के विधान सभा चुनाव में बीजेपी-जेडीयू साथ थी, तो जीत आसानी से मिल गयी थी. वहीं 2015 के विधान सभा चुनाव में जेडीयू-आरजेडी साथ थी, तो इस गठबंधन से बुरी तरह से बीजेपी हार गयी थी. एक बार फिर से 2020 के विधान सभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी साथ आती हैं, तो आरजेडी के लिए इस गठबंधन को मात देना मुश्किल हो जाता है.
यही अगर जेडीयू, बीजेपी और आरजेडी तीनों ही अलग-अलग रहकर चुनाव लड़ती है, तो इसमें जेडीयू की हालत बेहद ही पतली हो जाती है. यह हम सबने 2014 के लोक सभा चुनाव में देखा था, जब जेडीयू न तो बीजेपी के साथ थी और न ही आरजेडी के पाले में थी. उस चुनाव में जेडीयू महज़ दो लोक सभा सीट पर ही जीत पाती है और उसका वोट शेयर भी 8% से ज़ियादा गिरकर 16 फ़ीसदी से नीचे चला जाता है.
जेडीयू का जनाधार तेज़ी से कमज़ोर हुआ है
20 मई 2014 से 22 फरवरी 2015 को छोड़ दें, तो नीतीश कुमार बिहार में नवंबर 2005 से मुख्यमंत्री हैं. बीच वाली अवधि में भी उनकी ही पार्टी की सरकार थी. इन सबके बावजूद एक सच्चाई है कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का जनाधार बिहार में तेज़ी से कम हो रहा है. इसका एक बड़ा कारण यह है कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी फिर से जातिगत समीकरणों को साधने में कामयाब होती दिख रही है. उसके साथ ही पिछले एक दशक में बीजेपी का भी जनाधार प्रदेश में बढ़ा है. 2020 के विधान सभा चुनाव में तो बीजेपी के साथ गठबंधन होने के बावजूद नीतीश कुमार की पार्टी को महज़ 43 सीटों पर जीत मिली थी. इस ख़राब प्रदर्शन की वज्ह से जेडीयू बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन गयी.
जाति आधारित आरक्षण के तहत नया दाँव
हालाँकि नीतीश अगस्त 2022 से आरजेडी के साथ हैं. लेकिन उनको एहसास हो गया कि पुराने ढर्रे के हिसाब से जेडीयू के राजनीतिक जातिगत जनाधार की दीवार अब बेहद कमज़ोर हो चुकी है. प्रदेश में बीजेपी का प्रभाव भी बढ़ रहा है. ऐसे में नीतीश की राजनीति की प्रासंगिकता को बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो गया था कि प्रदेश में जाति के जिन्न को फिर से हवा दी जाए. इसके लिए नीतीश-तेजस्वी की सरकार ने पहले जातिगत सर्वे का सहारा लिया. उसके बाद उस सर्वे के नतीजों को आधार बनाकर अब जाति आधारित आरक्षण का नया दाँव चला है.
इसके तहत आनन-फानन में प्रस्ताव तैयार किया जाता है. इस प्रस्ताव से जुड़े विधेयकों को 9 नवंबर को बिहार विधान सबा से मंजूरी भी मिल जाती है. इसके तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्गों (ईबीसी) और अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण की वर्तमान सीमा 50% बढ़ाकर 65% करना है. इनके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण भी शामिल है. इस तरह से कुल आरक्षण 75% हो जाता है. इससे प्रदेश की शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरिओं में इन वर्गों के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ जायेगा. एसटी के लिए वर्तमान आरक्षण दोगुना हो जायेगा. एससी के लिए आरक्षण 16 बढ़कर 20 प्रतिशत हो जायेगा. ईबीसी के लिए आरक्षण 18 से बढ़कर 25 फ़ीसदी हो जायेगा.वहीं ओबीसी के लिए आरक्षण 12% बढ़कर 15% हो जायेगा.
सबसे अजीब बात यह है कि आरक्षण बढ़ाने से जुड़े प्रस्तावों को विधान सभा से सर्वसम्मति से मंजूरी मिली है. या'नी इसमें बीजेपी की भी सहमति है. यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसका विरोध करना किसी दल को चुनाव में नुक़सान पहुंचा सकता है क्योंकि हर दल को पता है कि बिहार में वोटिंग का सबसे मुख्य आधार जातिगत समीकरण है. कोई भी दल इस नुक़सान का ख़तरा मोल लेना नहीं चाहता है. जबकि बिहार सरकार के आरक्षण के इस प्रस्ताव की संवैधानिकता की परीक्षा होनी ही बाक़ी है. यह निश्चित है कि बिहार सरकार की इस कवायद को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ज़रूर दी जायेगी. ऐसा हुआ तो इसका भविष्य भी अभी सुनिश्चित नहीं है.
जातिगत राजनीति का नया कलेवर
लेकिन एक बात ज़रूर सुनिश्चित है कि पहले से ही सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर जातियों में बँटे बिहार के लोग फिर से जातिगत राजनीति के नये कलेवर में फँसने के लिए पूरी तरह से तैयार किये जा रहे हैं. विशुद्ध राजनीतिक मंशा को पूरा करने के लिए जातिगत सर्वेक्षण और उसके आधार पर आरक्षण सीमा बढ़ाने का शिगूफ़ा खड़ा किया गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है. जबकि हर राजनीतिक दल और उसके तमाम बड़े नेताओं के यह बात भलीभांति पता है कि अभी भी बिहार के हर इलाके में ख़ासकर ग्रामीण इलाकों में जाति विद्वेष व्यावहारिक तौर से किस कदर व्याप्त है.
विकास आँकड़ों का मोहताज नहीं होता
पिछले 33 साल से बिहार की सत्ता पर लालू प्रसाद परिवार या नीतीश कुमार का ही क़ब्ज़ा है. उसके बावजूद कोई सरकार अगर कहें कि मुझे विकास करने के लिए, कल्याणकारी योजनाओं का लागू करने के लिए किसी जातिगत आँकड़े की ज़रूरत है, तो यह प्रदेश की जनता के नज़रिये से हास्यास्पद ही कहा जायेगा. पार्टियों के लिए जातिगत सर्वेक्षण और आरक्षण सीमा बढ़ाने का शिगूफ़ा भविष्य के नज़रिये से ऐसा राजनीतिक हथियार है, जहाँ प्रदेश में विकास की अनदेखी करने की पूरी छूट मिल जायेगी.
जातियों में उलझाकर राजनीति करना आसान
जातिगत सर्वेक्षण और आरक्षण सीमा बढ़ाने को हम कह सकते हैं कि प्रदेश को नये सिरे से जातिगत राजनीति के नये कलेवर में झोंकने की कोशिश है. बिहार की बदहाली से जुड़े सवालों, राजनीतिक और सरकारी जवाबदेही से बचने की एक ऐसी तरकीब है, जिस पर कोई सवाल भी नहीं पूछेगा. पिछले कुछ महीनों से बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, उससे प्रदेश की राजनीति को जातिगत भँवर में नये सिरे से उलझाया जा रहा है. नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ ही बीजेपी भी इसमें बराबर की भागीदार है.
प्रदेश की बदहाली की जवाबदेही किसकी है?
अभी बिहार की दयनीय स्थिति को लेकर सवाल पूछने का वक़त था. चंद महीने बाद ही बिहार के लोग लोक सभा चुनाव में मतदान करेंगे और उसके बाद अक्टूबर-नवंबर 2025 में प्रदेश की सत्ता के लिए मतदान करेंगे. आज़ादी के बाद से ही बिहार विकास के हर पैमाने पर पीछे क्यों खड़ा है. बिहार सबसे ग़रीब राज्य है. साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़ा है. प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की स्थिति कितनी बदतर है, यह बिहार के हर परिवार को अच्छे से एहसास है. हेल्थ फैसिलिटी के पैमाने पर भी हम देश के बाक़ी राज्यों की तुलना में काफ़ी पीछे हैं. प्रति व्यक्ति आय के मामले में बेहद पीछे हैं. चाहे शिक्षा के लिए हो, चाहे नौकरी या नौकरियों तैयारियों के लिए हो, यहाँ तक की मज़दूरी की बात हो, बिहार का कमोबेश हर परिवार पलायन का दर्द लंबे समय से झेलते रहा है.
सरकारी और तमाम तरह के आँकड़ों से तो बिहार की बदहाली सामने आती ही रही है. हालात उन आँकड़ों से भी ज़ियादा ख़राब हैं, बिहार का निवासी होने के नाते यह मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ. दलगत समर्थन की भावना को दरकिनार कर दिया जाए, तो बिहार के अधिकांश लोग इस बात को स्वीकार करेंगे.
राजनीतिक विमर्श जाति के इर्द-गिर्द ही क्यों?
सवाल ये सारे हैं, जिनका जवाब तमाम पार्टियों और नेताओं को देना चाहिए. लेकिन आज़ादी के साढ़े सात दशक बाद भी बिहार में राजनीतिक और सरकारी सवालों के साथ ही राजनीतिक विमर्श का मुद्दा जाति और जाति आधारित आरक्षण ही बना हुआ है. जातिगत समीकरणों को साधना ही चुनाव में जीत और राजनीति के फलने-फूलने की गारंटी हो जाए, तो फिर विकास की धारा ऐसे दलों के लिए नुक़सान का सबब हो सकता है, जिनकी राजनीति का आधार ही जातिगत वोट बैंक हो. बिहार में तमाम पार्टियों ने इस पहलू का आज़ादी के बाद से ही ख़ास ख़याल रखा है. तभी तो विकास की कसौटी पर बिहार सबसे निचले पायदान पर है.
बदहाली के लिए सभी दलों की बनती है जवाबदेही
बिहार की बदहाली के लिए सिर्फ़ कोई एक दल ही ज़िम्मेदार नहीं है. कांग्रेस ने क़रीब चार दशक तक प्रदेश की सत्ता संभाली है. 1990 से आरजेडी और जेडीयू की सत्ता है. बीजेपी की भी ज़िम्मेदारी कम नहीं बनती है क्योंकि 2005 से अब तक बीजेपी भी नीतिश सरकार में तक़रीबन 12 साल हिस्सेदार रही है. अब तो जिस तरह से नीतीश-तेजस्वी सरकार ने पिछले कुछ महीनों में बिहार में जाति की चिंगारी को जिस तरह से हवा दी है, उससे इतना तय है कि आने वाले कुछ दशक में भी विकास की बाट जोहने की बेबसी ही बिहार के लोगों की मजबूरी बनी रहेगी. इस मजबूरी से बचने का एकमात्र रास्ता यही है कि बिहार के लोगों को सही मायने में राजनीतिक दूरदर्शिता दिखानी होगी. बिहार के लोगों को जाति के जंजालों में फँसे बिना राजनीति दलों के नेताओं से प्रदेश की बदहाली पर और विकास पर ही बार-बार सवाल पूछना होगा.
आख़िर बिहार में विकास हुआ किसका?
आज़ादी के बाद से ही तमाम नेताओं ने बिहार में प्रदेश और यहाँ के लोगों के विकास की सिर्फ़ बात की. लेकिन बिहार का वास्तविक तौर से विकास कभी हो नहीं पाया. हम लगातार बाक़ी राज्यों के मुक़ाबले पिछड़ते ही गये. जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के बाद जितने भी नेता बाद में बिहार की राजनीति में उभरे, उन सभी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई की दुहाई देते-देते अपना राजनीतिक और पारिवारिक उन्नति ज़रूर सुनिश्चित कर लिया. इसके एवज़ में बिहार और बिहार के लोगों का विकास हो या नहीं, इससे उनका कोई ख़ास वास्ता नहीं रहा. सवाल यह भी उठता है कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में सही मायने में जिनका विकास होना चाहिए था, बिहार में आर्थिक तौर से उन का विकास हुआ या नहीं. जिनको आधार बनाकर सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उनकी कमोबेश कुछ ख़ास नहीं बदली है, लेकिन राजनीतिक दलों और उनके नेताओं की स्थिति में ज़रूर ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ आया है.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ़ लेखक ही ज़िम्मेदार हैं.]