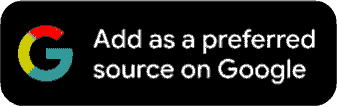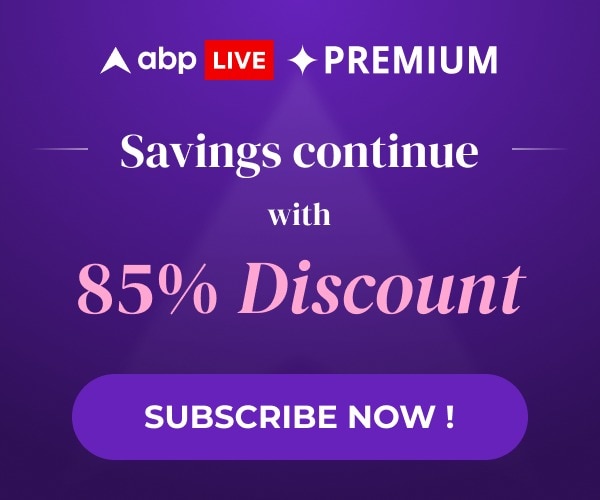भारतः अपनी तलाश करता हुआ एक मुल्क
.

भारत आज जब अपनी आजादी की 74वीं सालगिरह मना रहा है, फिर एक बार इस बात पर रोशनी डालने का अनुकूल समय है कि उपनिवेशवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई की विरासत में मिली ऐसी किन बातों को उसने सहेज कर रखा है, जिन्होंने उसे औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाई थी. स्वाभाविक है कि देश के मानस में इस समय कुछ इतर अहम मुद्दे हैं. कोरोना वायरस की आग देश के अधिकांश हिस्सों में धधक रही है और साफ हो चुका है कि तमाम राज्यों समेत देश की सरकार ने इसे रोकने के लिए जो कोशिशें की थीं, वे अपार्यप्त साबित हुईं.
इस वायरस से पैदा हुए हालात में करोड़ों लोग बेरोजगारी के चक्रव्यूह में धकेले जा चुके हैं. मगर इस बीच कई लोग 2019 में अयोध्या की राम जन्मभूमि पर आए सर्वोच्च अदालत फैसले के बाद देश के प्रधानमंत्री द्वारा किए गए ‘भूमि पूजन’ से हर्षोल्लास में डूबे हैं, तो कई चकित हैं. सैद्धांतिक रूप से वह देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं. लेकिन जिस भव्यता से यह कार्यक्रम हुआ इससे किसी राजा के राज्याभिषेक द्वारा हिंदू गौरव की स्थापना को महसूस किया गया. वह भी ऐसे दौर में जबकि एक महामारी सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ी है. वास्तव में इससे हमें वर्तमान सत्ता की प्राथमिकताओं की खबर मिलती है.
पश्चिम के इतिहासकारों ने बीसवीं सदी के इतिहास के पहले हिस्से को सामान्य रूप से विश्व युद्धों और दूसरे को शीत युद्ध के रूप में रेखांकित किया. लेकिन हम द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद के चार दशकों को समझें तो दुनिया कुछ अलग ढंग से विघटित होती हुई नजर आती है. भारत और इंडोनेशिया के पश्चात कई देश एक के बाद एक आजाद हुए. अफ्रीका ने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी और औपनिवेशिक उत्पीड़न की बेड़ियों से खुद को मुक्त किया. इसमें संदेह नहीं कि विश्व इतिहास में भारत ने अपनी आजादी का संघर्ष बहुत अनूठे ढंग से किया.
इसकी वजह भी बहुत साफ थी : महात्मा गांधी. वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के शिल्पकार थे. उन्होंने बड़े जनसमूह को अपने अहिंसा के विचारों से आंदोलित किया. ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें हिंसा की कोई जगह नहीं थी. मगर उनके सिद्धांतों को वे लोग नहीं समझ सकते जिन्होंने अहिंसा को सिर्फ ‘तकनीक’ तक सीमित मान लिया. गांधी ने राजनीति में नैतिकता के ऐसे ऊंचे मानक स्थापित किए, जिन्हें भविष्य में शायद की कभी कोई स्पर्श कर सके. ये मानक तो भारतीय नेताओं की वर्तमान नस्ल की समझ से भी परे हैं.
कई लोग भारत की स्वाधीनता की लड़ाई के सूत्र को 1857 के ‘स्वतंत्रता संग्राम’ से जोड़ते हैं. वीर सावरकर ने इसे भारतीय स्वातंत्र्य का पहला संघर्ष कहा था. मगर पारंपरिक इतिहासकार भारत की आजादी के संघर्ष की गणना 1885 से करते हैं, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी. इतिहास का एक पक्ष यह है कि यही कांग्रेस गांधी के सामने आदर्श की तरह थी, जब उन्होंने 1912 में अफ्रीका में उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी. इसी कांग्रेस को देख कर ही 1914 में ईस्ट अफ्रीकन इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना की गई थी. 20 साल तक साउथ अफ्रीका में रह कर जब गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे, तो ऐसा नहीं था कि वह तत्कालीन भारतीय राजनीति में पैदा हुए किसी शून्य को भरने आए थे. उन दिनों भारत में बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले (महाराष्ट्र), बिपिन चंद्र पाल, सी.आर. दास (बंगाल) और लाला लाजपत राय (पंजाब) की तूती बोल रही थी.
वास्तव में आश्चर्यजनक यह था कि मात्र अगले चार साल में गांधी तेजी से भारतीय राजनीति में सितारे की तरह उभर कर आए. गांधी से वैचारिक मतभेद रखने के बावजूद उनका सम्मान करने वाली, उनकी समकालीन सोशलिस्ट और नारीवादी नेता कमलादेवी चट्टोपाध्याय की यह बात गौर करने लायक है कि गांधी के भारतीय राजनीति में प्रवेश के साथ ही उनसे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण संघर्ष हुआ था, वह जैसे गुमनामी में खो गया.
उस दौर में भले ही कमलादेवी की बात को बहुत तवज्जो नहीं दी गई मगर बाद में इस बात को मानने वालों की संख्या भारत में बढ़ती गई और गांधी पर हमले भी हर दिशा से होने लगे. यह कहना गलत नहीं होगा कि उपनिवेश विरोधी संघर्ष के देश में और भी मोर्चे थे. गरम पंथियों का गदर आंदोलन भले ही कम समय के लिए अस्तित्व में रहा परंतु इसमें शामिल क्रांतिकारियों ने दुनिया के अन्य राष्ट्रों से हाथ मिलाकर तत्कालीन ब्रिटिश सरकार की नाक में खासा दम किया. इधर 1920 के दशक में खूब चर्चित रही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी और उसकी सबसे प्रेरक शख्सियत भगत सिंह पर भी काफी लोगों का ध्यान गया है. बंगाल में सुभाष चंद्र बोस हमेशा सबके चहेते रहे हैं लेकिन उनके द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल आर्मी (आईएनए) का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान बहस का मुद्दा बना रहा है.
भारतीय राष्ट्रवाद में अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की चाहे जो जगह हो मगर गांधी की उपलब्धियां न केवल अलग ऊंचाइयां छूती हैं बल्कि इतिहास में भी उनकी एक अति-विशिष्ट जगह है. भारत ने अपनी आजादी की लड़ाई के लिए अलग-अनोखी राह चुकी थी और स्वतंत्रता संग्राम की ऐतिहासिक परंपरा पर विचार करते हुए इसके लिए आपको गांधी और कांग्रेस पार्टी को श्रेय देना ही पड़ेगा. उस दौर में औपनिवेशिक आक्रांताओं से आजादी पाने वाले देशों में भारत काफी अलग था क्योंकि इसने स्वतंत्रता के बाद भी अपने यहां लोकतंत्र की संरचना और आत्मा को जीवित रखा.
पड़ोसी पाकिस्तान में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को ढहाने की कोशिशें 1951 में ही शुरू हो गई थी. 1958 में वहां हुए सैन्य विद्रोह के बाद लगा मार्शल लॉ 1971 तक चला. इसके बाद भी पाकिस्तान ने 1977-88 और 1999-2008 तक मार्शल लॉ के लंबे दौर देखे. वहीं इंडोनेशिया में 1965-66 में कम्युनिस्टों के खिलाफ अमेरिकी मदद से जो कार्रवाई शुरू हुई उसने सेना और डेथ स्क्वाड्स के हाथों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया. उधर, अल्जीरिया में भी रक्तपात हुआ और नतीजे में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 1954-62 तक लंबी खूनी लड़ाई लड़ी.
इंदिरा गांधी के दौर में 1975 में लगे आपातकाल की तरफ इशारा करते हुए कहा जा सकता है कि भारत में भी कुछ ऐसे हालात पैदा किए गए. जब जनता से संवैधानिक अधिकार छीन लिए गए. लेकिन इस तथ्य से कैसे इंकार किया जा सकता है कि जल्दी ही इंदिरा को इसके नतीजे भुगतने पड़े और 1977 में कराए चुनावों में जनता ने उन्हें तथा उनकी पार्टी को गद्दी से उतार दिया. अनुभवी गांधीवादी नेता जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा के विरुद्ध क्रुद्ध जनता के आंदोलन का नेतृत्व किया. वैसे यह नहीं भूलना चाहिए कि जून 1975 में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा अपने विरुद्ध दिए फैसले ने इंदिरा गांधी को विचलित किया था, जिसकी वजह से उन्होंने देश में आपातकाल लगाया था.
वास्तव में हम कह सकते हैं कि आजादी के दशकों बाद भी भारत में अलग-अलग राजनीतिक शक्तियों का अस्तित्व था और हमारी अदालतें भी अपने आप में स्वतंत्र तथा पूरी शक्ति के साथ मजबूत थीं. भारतीय लोकतंत्र में एक और खूबी है, जो औपनिवेशिक आजादी से छूटे दूसरे लोकतंत्रिक देशों में कम ही दिखती है. वह है यहां की सत्ता-व्यवस्था ने सेना को राजनीतिक और नागरिक मामलों से सफलतापूर्वक दूर रखा.
यह राष्ट्र के प्रति गांधी का ही नजरिया था, जिसमें वह सारी ताकत एक हाथ में जाने को संदेह से देखते थे. वह राजनीतिक स्वतंत्रता को तब तक सच्ची मानने के हक में नहीं थे जब तक सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार समान रूप से न दिए जाएं. जेपी का आंदोलन हो या फिर पर्यावरण को बचाने वाला चिपको और महिलाओं को आर्थिक स्वायत्तता दिलाने वाला सेवा (सेल्फ-एंप्लॉय्ड वीमंस एसोसिएशन) आंदोलन, गांधी के ही नजरिये से इन्होंने जनतंत्र में आम लोगों की भूमिका को मजबूत बनाया.
भले ही गांधी अपने जीवन काल में अपने समकालीनों पर छाए नजर आते हैं मगर इसके बावजूद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के आकाश पर मौलाना आजाद, पटेल, नेहरू, कमलादेवी, सरोजिनी नायडु और राजगोपालाचारी जैसे सितारे चमकते हैं. स्वतंत्रता के बाद इनके विचारों और भावनाओं को डॉ. अंबेडकर और संविधान सभा द्वारा निर्मित भारत के संविधान में यथोचित सम्मान और स्थान भी मिला.
संविधान की प्रस्तावाना में भारत का वर्णन ‘संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में किया गया था मगर इसके मात्र 25 बरस बाद, आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा इस प्रस्तावना के शब्द बदल कर भारत को ‘संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य’ के रूप में तब्दील कर दिया गया. यह विचारणीय है कि संविधान निर्माताओं का भारत की बहु-जातीय, बहु-धार्मिक और बहु-भाषी सभ्यता में इतना विश्वास था कि उन्होंने प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’ शब्द को जोड़ना अनिवार्य नहीं समझा. लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां ‘धर्मनिरपेक्ष’ को बाद में शामिल किए जाने का वह मतलब नहीं है, जो पश्चिम में होता है. वहां धर्मनिरपेक्ष का मतलब है ‘चर्च’ से ‘राज्य’ का अलगाव.
हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माता गांधी की उस दृष्टि से प्रेरित थे, जिसके अनुसार अतीत से ही भारत में अलग-अलग धर्मों-जातियों के रोजमर्रा जीवन के कारोबार एक-दूसरे से अंतर-संबधित और अंतर-निहित हैं और इससे वे सहज ही धर्मनिरपेक्ष हो जाते हैं. लेकिन 1976 में जिस तरह से श्रीमती गांधी ने भारत के ‘धर्मनिरपेक्ष’ स्वरूप को स्पष्ट किया, उससे पता चलता है कि वैचारिक पतन की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी. आजादी के मात्र छह महीने बाद 30 जनवरी, 1948 को महात्मा गांधी की हत्या इसी बात की तरफ संकेत करती है. जैसा कि रॉबर्ट पायने ने कहाः निःसंदेह ऐसा ही था. इस ‘हत्या की इजाजत’ थी.
कुछ हिंदू राष्ट्रवादी थे जिनके मन में गहरे न केवल यह बात अंकित थी कि गांधी राष्ट्रद्रोही हैं बल्कि वह उन्हें ‘पाकिस्तान का जनक’ मानते थे. ये लोग मानते थे कि अगर भारत को विश्व में बाहुबली और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरना है तो आधुनिक औद्योगिक सभ्यता की आलोचना करने वाले को सहन नहीं किया जा सकता. श्रीमती गांधी के समय में और 1980 के दशक के अंत तक आते-आते इस वैचारिक सड़ांध ने गहराई तक जाकर सांप्रदायिकता का रूप ले लिया और इसका नतीजा यह हुआ कि भारतीय आदर्शों के मूल्यवान सूत्रों का त्याग कर दिया गया.
आज के भारत में गांधी, नेहरू, स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों और संविधान निर्माताओं के उदात्त विचारों का थोड़ा कुछ भी बाकी है तो इसमें संदेह है. पिछले कुछ वर्षों में न्यायालयों की स्वतंत्रता से भी गंभीर समझौते हुए. इस वक्त जब मैं ये पंक्तियां लिख रहा हूं सर्वोच्च न्यायालय ने देश के प्रमुख अधिवक्ताओं में शामिल प्रशांत भूषण को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी पाते हुए अपने महत्व को और कम कर लिया है. सच्चाई तो यह है कि परिपक्व लोकतंत्र में ‘अदालत की अवमानना’ जैसे मामलों की ओर लक्ष्य ही नहीं किया जाता.
भारत में धर्मनिरपेक्षता के सवाल पर यह साफ है कि यह पश्चिम की तरह नहीं है और इसमें फ्रांसrसी क्रांति और वहां के विद्वान दार्शनिकों के मुद्दे शामिल नहीं हैं. गांधी ने अपनी धर्मनिरपेक्षता को एक धर्मनिष्ठ हिंदू होकर पाया था, ठीक वैसे ही जैसे मौलाना आजाद अपनी धर्म निरपेक्षता का पालन धर्मनिष्ठ मुस्लिम होते हुए करते थे. लेकिन भारतीय संविधान में धर्मनिपेक्षता को स्वीकार कर लेने से कुछ बातें उलझ गईं. जिससे शुरुआती दो-तीन दशकों तक उलझन पैदा होती रही. इसमें से एक विचार साफ था कि राज्य किसी धर्म को प्राथमिकता या दूसरे धर्म पर वरीयता नहीं देगा. साथ ही यह भी कहा गया कि हर धर्म के अनुयायी बिना किसी बाधा या राज्य के पूर्वाग्रह के अपने धर्म के अनुकूल आचरण कर सकते हैं.
प्रधानमंत्री ने अभी-अभी लाल किले की प्राचीर से एक और भव्य भाषण दिया है. यह उनका काम है. देश को लगभग हिंदू राष्ट्रवादियों के हाथों में सौंप दिया गया है. अब यह एक सीधा सरल सवाल नहीं है कि क्या सत्ता में बैठे लोग संविधान की शपथ के विपरीत अपने हिंदू-मतदाताओं की ही सेवा करेंगे.
भारत में यह समस्या गहरे पैठ चुकी और इसका समाधान तब भी नहीं दिखता कि अगले चुनावों के बाद कांग्रेस या कोई भाजपा-विरोधी गठबंधन सत्ता में आ जाए. हालांकि इस समय इसके आसार नगण्य दिखाई देते हैं. देश में ‘हिंदू आवेग’ की बात हो रही है, जिसके बाहर कुछ भी दिख नहीं रहा है. वास्तव में हिंदू राष्ट्रवादियों के लिए काम कर रहे ट्रोल्स और स्ट्रीट गैंग उग्र तेवरों के साथ सामने हैं. वे बताते हैं कि सारा असंतोष खत्म हो गया है. वे रोजमर्रा की जिंदगी में मुस्लिमों को संदिग्ध कहते हैं और इतिहास से हिंदू नायकों की स्मृतियां निकाल कर यह दृढ़ संकल्प दोहराते हैं कि विदेशियों में देश को मुक्त करा के इसे फिर से महान हिंदू भारत बनाएंगे. यह ‘हिंदू आवेग’ अभी निकट भविष्य में कायम रहने की संभावना है.
ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में कहा जाता है कि खुद को पाने से पहले खुद को खोना होता है. मैं कहूंगा कि ऐसे लोग भारत में और खास तौर पर हिंदुओं में है, जिन्हें एक ऐसे देश की तलाश है, जिसे वे अपना कह सकें. इनके पास अपने अतीत के भव्य महल हैं. ये अपनी भव्यता से घबराए और शर्मिंदा होकर एक सभ्यता में कैद हैं, जहां अन्याय और दूसरी कमियां हैं. मुझे लगता है कि इनके पास अपने घर ही नहीं हैं. सामान्य रूप से मैं यही दुखद दृश्य देखता हूं कि ज्यादातर भारतीयों को अपनी तलाश करनी होगी. तभी उनके पास खोने को कुछ होगा. तभी स्वतंत्रता के तमाम वायदों के कुछ मतलब निकलेंगे.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)