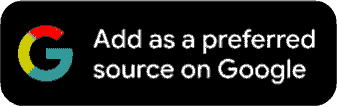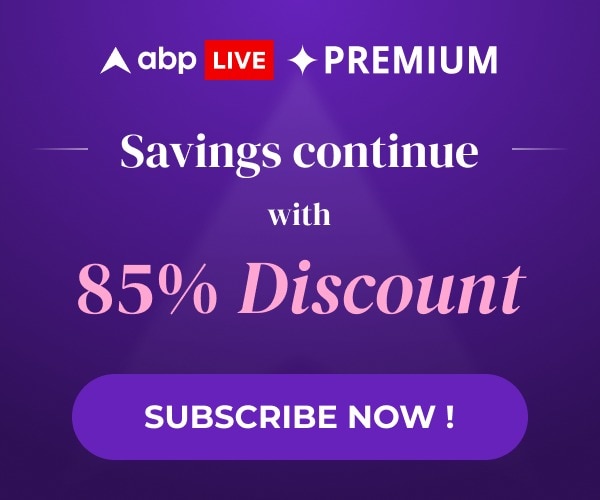BLOG: मायावती को दलित अपराइजिंग के प्रिज्म से देखा जाना चाहिए
मायावती की रैलियों की यह शैली है कि मंच पर कोई जूते पहनकर नहीं चढ़ सकता. बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को धूल से एलर्जी है.

मंदिर में दाखिल होने से पहले जूते-चप्पल स्वतः पैरों से निकल जाते हैं. देवबंद में चुनावी सभा के दौरान रालोद के मुखिया अजीत सिंह ने भी मंच पर चढ़ते समय अपने जूते उतार दिए. लेकिन यह स्वतः नहीं, मायावती के प्रोटोकॉल के चलते हुआ. मायावती की रैलियों की यह शैली है कि मंच पर कोई जूते पहनकर नहीं चढ़ सकता. बताते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो को धूल से एलर्जी है. हालांकि वह खुद मंच पर चप्पल उतारकर नहीं चढ़तीं. उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं. इस गठबंधन ने अपनी पहली चुनावी रैली सहारनपुर के देवबंद में की और यह खबर वहीं से निकलकर बाहर आई.
बहनजी का काम करने का अपना स्टाइल है. आपको उनके साथ काम करना है तो उस स्टाइल को अपनाना ही पड़ेगा. ताकत के आगे झुकना कौन सी बड़ी बात है. राजनीतिक ताकत से बड़ी ताकत, आज कौन सी है. इसे हासिल करने की जद्दोजेहद चुनावी मौसम में सबसे ज्यादा दिखाई देती है. यह ताकत बीएसपी के पास पहले भी थी, अब भी है. भले 2014 में पार्टी के 503 उम्मीदवारों में से एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता था. लेकिन वोट शेयर के हिसाब से बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी थी. उसके 34 उम्मीदवार अपनी-अपनी सीटों पर दूसरे नंबर पर थे. फिर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और उसके सहयोगी स्टार थे. बाकी सारे सितारे फीके पड़ गए थे.
लेकिन फौरी जीत-हार कई बार भविष्य की लड़ाइयों को कमजोर नही करतीं. फिर बीएसपी की लड़ाई, दलितों की अपनी लड़ाई है. मायावती का प्रोटोकॉल अलग ही है. इस जूता प्रकरण की खबर पढ़ने के बाद मध्य प्रदेश के दमोह की ढाई साल पुरानी खबर भी याद आ आई. दमोह जिले के तेजगढ़ थाने के मनका गांव में दर्जन भर दलितों की सिर्फ इसलिए जबरदस्त पिटाई की गई थी क्योंकि ऊंची जाति के दबंगों के घर के सामने से गुजरते समय वे चप्पल पहने रहते थे, चप्पलों को सिर पर नहीं रखते थे. कभी दलितों का चप्पल पहनना भी बहुत बड़ा प्रिवलेज माना जाता था.
केतन मेहता की फिल्म ‘मांझी’ में मुसहर जाति के शख्स को जूते पहनने की सजा उसके पैरों में घोड़े की नाल ठुकवाकर दी जाती है. सो, जिन दलितों को चप्पल के चलते इतनी ज़िल्लत झेलनी पड़ती हो, उन्हें मायावती की यह मुद्रा कितना संबल देती होगी, इसकी कल्पना करना किसी सवर्ण के लिए बहुत मुश्किल है. यूं दलित उत्पीड़न की घटनाओं के प्रति सहानुभूति दिखाना आम बात है लेकिन यह राजनीतिक पाखंड से ज्यादा कुछ है. यह स्वस्फूर्त सहानुभूति नहीं है. सच्चाई तो यह है कि दलितों को नाराज करने की हिमाकत अब कोई राजनैतिक वर्ग नहीं कर सकता.
मायावती का यही महत्व और प्रासंगिकता भी है. वह चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. अपने कार्यकाल में बड़े से बड़े प्रशासनिक अधिकारी को लाइन हाजिर किए रहना उनकी खास अदा रही है. सिक्योरिटी ऑफिसर से सैंडिल साफ करवाने की फोटो तो 2011 में अखबारों ने खूब छापी थी. इसके अलावा उनके तेवर से भी ज्यादातर लोग वाकिफ हैं. और उनकी यह मुद्रा उनके मतदाताओं को खासी लुभाती है. दरअसल, वह उत्तर प्रदेश में अस्सी के दशक में शुरू हुई एक राजनीतिक प्रक्रिया की उपज हैं जिसके जनक कांशीराम थे. यह प्रक्रिया दबे-कुचले वर्गों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा पैदा होने और उसके बाद राजनीतिक गोलबंदी से प्रारंभ हुई. मायावती उसी धारा का नेतृत्व करती हैं. सवर्णों के सांस्कृतिक और राजनीतिक वर्चस्व को जोरदार चुनौती देती हैं. वह वर्चस्व जो कहीं दलितों को बारात में घोड़ी पर चढ़ने नहीं देता है, कहीं मिड डे मील पकाने से रोकता है और कहीं पानी के नल को हाथ लगाने पर पीट-पीटकर अधमरा करता है. मायावती इसी अवसाद को स्वर देती हैं.
मायावती की प्रासंगिकता को लेकर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं. पूछा जाता है कि वह इतने लंबे समय तक प्रासंगिक कैसे हैं. इसके बावजूद कि बीजेपी उनके वोटबैंक में 2014 में जबरदस्त सेंध लगा चुकी है. लेकिन मायावती की राजनीति में कुछ तो ऐसा है जो उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में उन्हें खत्म होने से बचाता है. यह बात और है कि जमाना उनके खिलाफ है. नौकरशारी उनके खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट फरवरी में उनसे कहा चुका है कि वह चुनाव चिन्ह की मूर्तियां बनवाने पर खर्च हुए सार्वजनिक धन को सरकारी खजाने में जमा कराएं.
दलित आज भारतीय जनतांत्रिक राजनीति का सबसे ऊर्जावान तबका है. अगर जनतंत्र का अर्थ ऐतिहासिक अन्याय और गैरबराबरी का मुकाबला है तो उसे इस अर्थ की याद दिलाने वाला समाज भी दलितों का ही है. इसीलिए मायावती को दलित अपराइजिंग के प्रिज्म से देखा जाना चाहिए. इसी प्रिज्म ने गुजरात में जिग्नेश मेवानी जैसा युवा नेता खड़ा किया और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर को लोकप्रिय बनाया. कांशीराम और उसके बाद मायावती ने दलित समुदाय को राष्ट्र की मुख्यधारा में लाने की जो पहल की, उसी का नतीजा ऊना के बाद की घटनाओं में देखने को मिला.
2016 में ऊना में दलितों की पिटाई के बाद गुजरात के शहरों की सड़कों पर गायों के शव बिखेर दिए गए. वह भी उन दलितों ने जो लोगों की नजरों की ओट में मृत गायों का निबटारी किया करते हैं. बाबा साहेब अंबेडकर लोगों की स्मृतियों से वर्तमान में आ गए. नीला रंग जय भीम के साथ जुड़ गया. समाज की वंचित जातियों में यह एहसास हुआ कि उनके बीच का या उनके प्रति हमदर्दी रखने वाला कोई शख्स ऊपर बैठा है. इस अहसास को न तो नापा जा सकता है, न इसका कोई आंकड़ा होता है. इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है.
यह अहसास जब तक है, मायावती की राजनीति तब तक खत्म नहीं हो सकती. इससे अधिक भावुक एहसास कराने वाले नेता का इंतजार है. दलित अस्मिता पर कब्जे की बदहवास कोशिशें दूसरे राजनीतिक दल भी करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे. जिसकी राजनीति ज्यादा लच्छेदार वादे कर पाएगी, उसी की जीत पक्की होगी. तब तक मायावती तमाम आलोचनाओं और ट्रोल्स के बावजूद बनी रहेंगी.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)