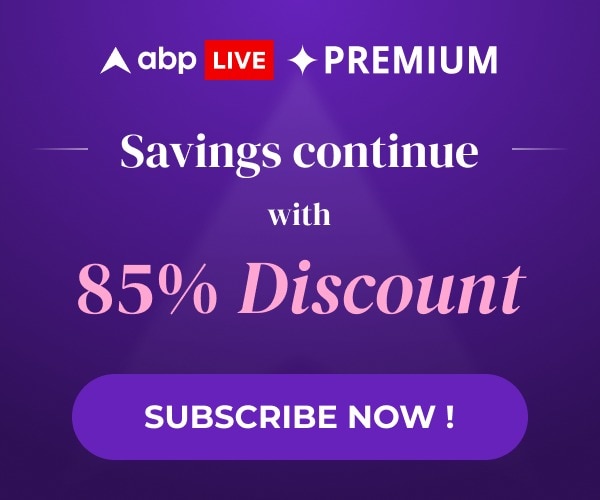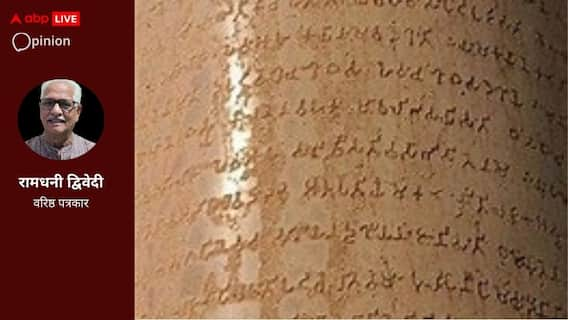चुनावी खर्च बढ़ रहा है, चुनावी अर्थ घट रहा है

कहने को तो भारत आर्थिक तौर पर एक विकासशील (वास्तव में गरीब) देश है, लेकिन चुनावी खर्च के मामले में इस बार यह कई विकसित (जैसे अमेरिका) देशों को पीछे छोड़ने जा रहा है. सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज (सीएमएस) के एक अनुमान के मुताबिक 11 अप्रैल से 19 मई तक सात चरणों में संपन्न होने जा रहे 2019 के लोकसभा चुनाव में 50,000 से 60,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में 35,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था. 'कारनीज एंडोमेंट फोर इंटरनेशनल पीस थिंकटैंक' में सीनियर फेलो और दक्षिण एशिया कार्यक्रम के निदेशक मिलन वैष्णव का कहना है कि 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और कांग्रेस चुनावों में 46,211 करोड़ रुपए (650 करोड़ डॉलर) खर्च हुए थे. जाहिर है, अगर भारत के इस आम चुनाव का खर्च 50,000 करोड़ रुपए के पार गया, तो यह दुनिया का सबसे खर्चीला चुनाव साबित होगा.
आजकल के चुनावों में अनैतिक खर्च का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1952 में हुए पहले आम चुनाव का खर्च 10 करोड़ से भी कम आया था, यानी प्रति मतदाता पर करीब 60 पैसे का खर्च. यह ठीक है कि उस समय यह रकम मामूली नहीं थी, लेकिन गैर-सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आज विभिन्न दलों की ओर से 50-55 करोड़ रुपए मात्र एक संसदीय सीट में बहा दिए जाते हैं. शुरुआती दो-तीन आम चुनावों तक दिग्गज उम्मीदवार भी बैलगाड़ियों, साइकलों, ट्रकों पर प्रचार करते देखे जा सकते थे. फटेहाल नेताजी की आर्थिक मदद खुद कार्यकर्ता किया करते थे. लेकिन आज के नेता हेलीकॉप्टरों या निजी विमानों से सीधे रैलियों में उतरते हैं और करोड़ों रुपए खर्च करके लाखों लोगों की भीड़ जुटाते हैं.
रैलियों में ज्यादा भीड़ जुटाने के साथ भीड़ के खाने-पीने और पत्रम-पुष्पम की व्यवस्था का चलन छोटे शहरों में भी शुरू हो गया है. प्रचार के साथ-साथ ब्रैंडिंग पर ज्यादा जोर देने की वजह से चुनाव में खर्च बढ़ता ही जा रहा है. किस जगह पर कौन-सी ड्रेस पहनें और किस चुनावी क्षेत्र में किस तरह से बात करें, जैसी तमाम चीजों पर नेताओं का मुख्य ध्यान रहता है. दिलचस्प बात यह है कि इस सबमें पार्टी से ज्यादा पैसा उम्मीदवार खर्च करते हैं और इस पर पार्टियों को जरा भी ऐतराज नहीं होता. इसका असर यह होता है कि जिसके पास पैसा नहीं है, उसको पार्टी का टिकट ही नहीं मिलता और लोकतांत्रिक मूल्यों की सीधे हत्या हो जाती है. इस प्रक्रिया में शासन-प्रणाली से साधनहीन जनप्रतिनिधियों की अपने आप छंटनी हो जाती है और विधानसभाएं तथा संसद 'करोड़पति क्लब' बनती चली जाती है.
यह सच है कि तकरीबन छह हफ्ते तक चलने वाले इन चुनावों में 543 लोकसभा सीटों के लिए तकरीबन 90 करोड़ मतदाता हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण के समुद्री तट तक करोड़ों लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे. इस महाचुनाव में वोट डालने के लिए 11 लाख इलेक्ट्रॉ निक वोटिंग मशीन की आवश्याकता होगी और करीब 10 लाख मतदान केंद्र स्थाापित किए जाएंगे. इस विशाल चुनावी कवायद में सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए खर्च होना स्वाभाविक है. लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि जिस देश की 60 फीसदी आबादी रोजाना तीन डॉलर से कम की आमदनी में अपना गुजारा करती है, वहां आम चुनाव में प्रति वोटर आठ डॉलर खर्च होने जा रहा है. इसकी प्रमुख वजहों में सोशल मीडिया, आवागमन, रैलियां और हर तरह के विज्ञापन का बढ़ा हुआ खर्च है. कहा जा रहा है कि विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा सोशल मीडिया पर इस बार 5000 करोड़ रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं, जबकि पिछले लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया पर मात्र 250 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे.
वैसे इस अनुमानित हजारों करोड़ के खर्च को मापने का कोई सटीक और विश्वसनीय पैमाना किसी के पास नहीं है. निश्चित तौर पर यह भी नहीं कहा जा सकता कि कौन-सी पार्टी इसे किस-किस मद में कैसे खर्च करती है. नियम के मुताबिक एक उम्मीदवार लोकसभा चुनाव में 50 लाख से 70 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है. विधानसभा चुनाव के लिए यह सीमा 20 लाख से 28 लाख रुपए के बीच है. यह खर्च उस राज्य पर भी निर्भर करता है जहां से उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है. माना कि लोकसभा की 543 सीटों के साथ-साथ कुछ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी साथ होने जा रहे हैं. फिर भी इनका घोषित खर्च अनुमानित खर्च का 5-7% भी नहीं बैठता. इसे हम कर्नाटक के मई 2018 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव से समझ सकते हैं, जिसमें विभिन्न राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों द्वारा वास्तविक तौर पर 9,500 से 10,500 करोड़ रुपए के बीच धन खर्च किया गया. यानी प्रति मतदाता 2100 रुपए का खर्च!
गैर-सरकारी तौर पर अनुमानित मायावी राशि अनैतिक और बिना खाता-बही वाली ब्लैक मनी ही होती है. चुनाव आयोग ने एक राशि निर्धारित की हुई है, लेकिन असल में खर्च कितना होता है, यह पकड़ पाना आयकर विभाग के वश में भी नहीं है. पुराने जमाने के जनता से सीधे जुड़े कई नेता आपको बताएंगे कि वे तो 1500-2000 रुपए खर्च करके ही चुनाव जीत लेते थे. लेकिन आप आज के किसी दिग्गज माने जाने वाले प्रत्याशी से भी पूछिए कि चुनाव लड़ने में कितना खर्च हो रहा है, तो पता चलेगा कि जो निर्धारित राशि है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा खर्च किया जाना है, फिर भी जीत की कोई गारंटी नहीं है. इसलिए चुनाव में होने वाले घोषित-अघोषित और काले-सफेद खर्च को जब तक नहीं ढूंढ़ा जाएगा, तब तक केवल सरकारी खर्च व प्रत्याशियों द्वारा चुनाव आयोग को बताए गए खर्च को जोड़ने मात्र से असली तस्वीर सामने नहीं आने वाली है.
एक तस्वीर यह भी है कि भारत को हर साल सब्सिडी के लिए लगभग 3 लाख करोड़ रुपए चाहिए होते हैं, जबकि करीब 30 करोड़ लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं मिलती. ऐसे में चुनावों के लिए बेतहाशा पैसा उड़ा कर अमेरिका से आगे निकल जाना किसी अश्लीलता से कम नहीं लगता. मतदाता की नजर में चुनी जाने वाली सरकारें भले ही अर्थवान हों, लेकिन राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आचार-विचार या नीतियों का नहीं, शुद्ध प्रचार का अखाड़ा बन चुका है. कोई कार्यकर्ता नहीं सोचता कि आखिर इतना पैसा कहां से आया? इसका क्या स्रोत है? क्या पार्टियों के फंड में इतना पैसा है? या फिर गलत तरीके से लाए गए धन का इस्तेमाल हो रहा है? यदि ऐसा है तो इसे कैसे रोका जा सकता है? सच्चाई यह है कि यह खर्च गुप्त कॉरपोरेट फंडिग, हवाला कारोबार और अप्रवासी नागरिकों की बेनामी मदद के दम पर किया जाता है, जो सरकार बनने पर देश के नीति निर्धारण में हस्तक्षेप करते हैं. दरअसल चुनाव अब कालेधन की ताकत का खेल हो गया है, जिसे पूरी ईमानदारी से खत्म किया जाना बहुत जरूरी है.
लेखक से ट्विटर पर जुड़ने के लिए क्लिक करें- https://twitter.com/VijayshankarC और फेसबुक पर जुड़ने के लिए क्लिक करें- https://www.facebook.com/vijayshankar.chaturvedi
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस