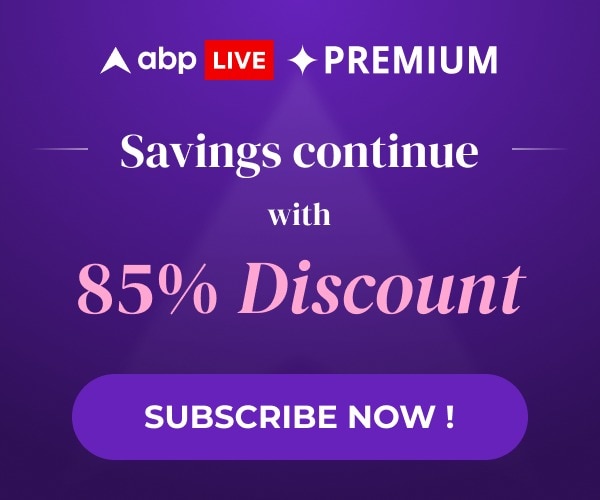(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)
हिंदुत्व की विचारधारा के करीब आ रही है दलित राजनीति

रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस की "मोदी परिवार" में वापसी के प्रतीकात्मक महत्व को नकारना मुश्किल है. समकालीन भारतीय राजनीति गठबंधनों के सहारे आगे की ओर बढ़ रही है. इसलिए सामाजिक ढांचे की सच्चाई अपनी आवाज बुलंद कर रही है. जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समाज के सभी समूहों की भागीदारी होती है तो उस घर में भी दीये जलने लगते हैं जहां सदियों से अंधेरे ने बसेरा कायम कर लिया था.
गठबंधन के सहारे वर्तमान राजनीति
रामविलास पासवान की मृत्यु के पश्चात् लोजपा दो गुटों में बंट गयी. पासवान की राजनीतिक विरासत को जाति और परिवार की सीमाओं में समेट कर नहीं परखा जा सकता. यह सच है कि दलित समाज अपने अंदर एक मध्य वर्ग के उदय से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन दलित राजनीति अब सिर्फ शोषण एवं अत्याचार की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं रही बल्कि अब यह हिंदुत्व की व्यवस्था का अभिन्न अंग बन गयी है.
आजादी के बाद दलित आंदोलन के जरिए देश ने महत्वपूर्ण राजनीतिक करवटें लीं. कांशीराम की बसपा अपने शुरुआती दिनों में सिर्फ बहुजन समाज के कल्याण की बातें करतीं थीं, किंतु समय के दबाव ने पार्टी को संकीर्ण दायरे से बाहर निकलने के लिए विवश कर दिया और मायावती सत्तावादी राजनीति की प्रतीक बन गयीं. जब उत्तर प्रदेश में मायावती के नेतृत्व में बसपा ने अपने बलबूते सरकार का गठन किया तो सामाजिक सोच को एक नई दिशा मिली थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों ने उनके राजनीतिक आभामंडल के विस्तार को बाधित कर दिया. समाजवादी पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को न तो सामाजिक स्वीकार्यता मिली और न ही अपेक्षित मात्रा में वोट मिल सका क्योंकि मध्यवर्ती जातियों के दबंग लहजे में दलित समाज के सदस्यों ने कभी अपनापन नहीं देखा.
दलित-पिछड़ा राजनीति, तलाशती वजूद
देश के अलग-अलग हिस्सों में दलित - पिछड़ा राजनीति समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्षतावाद के साये में अपना वजूद ढूंढ़ती रही है, लेकिन वर्ष 2014 के आम चुनाव ने राजनीति की स्थापित परंपराओं को पूरी तरह बदल डाला. अब दलित समाज को हिंदुत्व की विचारधारा आकर्षित करती है. चिराग पासवान की राजनीतिक शैली में परिपक्वता दिखाई देती है. मंत्री पद से दूर रह कर अपनी पार्टी लोजपा(रामविलास) के लिए पांच सीटें हासिल कर लेना एनडीए के अंदर उनके रुतबे के प्रदर्शन के लिए पर्याप्त है. वे अभी युवा हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सम्मान के मामले में अपने हमउम्र नेताओं की तुलना में अधिक उदार हैं. बिहार के नौजवान उनमें अपना भविष्य देख सकते हैं. तेजस्वी यादव राजद को आधुनिक स्वरूप नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें कुछ नया करना होगा. लोकसभा चुनाव के लिए उनकी पार्टी ने जिन लोगों को उम्मीदवार बनाया है, उससे "जंगल राज" की अवधारणा को ही बल मिलता है. राजद सांसद प्रो मनोज झा ने राज्यसभा में ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता "ठाकुर का कुआं" पाठ कर अपने वाक्कौशल का परिचय तो बखूबी दिया, लेकिन उनकी पार्टी के एक नेता ने इसे अपनी बिरादरी का अपमान माना और परिवार सहित जद(यू) का दामन थामना उचित समझा.
दलित चिंतन और यूरोपीय दृष्टि
कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार राजद की कुटिल नीति के कारण ही बेगूसराय से चुनाव नहीं लड़ पाए. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया की बातों को लोग सुनना चाहते थे. हालांकि इस तथ्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है कि कन्हैया ने वामपंथी विचारधारा को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया. साम्यवाद और धर्मनिरपेक्षता के रूमानी अफ़सानों ने दलित समाज को कितना सशक्त किया है, इस मसले पर चर्चा करने के बजाय कथित मार्क्सवादी विचारक लेनिन एवं स्टालिन की यादों में खो जाते हैं.
ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले के योगदान को समझने के लिए यूरोपीय दृष्टिकोण की जरूरत नहीं है. भारतीय राजनीति की यह दुखद सच्चाई है कि मतदाताओं के लिए विचारधारा नहीं बल्कि नेता महत्वपूर्ण हैं. द्रविड़ राजनीति ने करुणानिधि के परिवार को तमिलनाडु की सत्ता का स्थायी दावेदार बना दिया. "डीएमके" पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद के सपने देखने की इजाजत नहीं है. उदयनिधि मारन जब सनातन धर्म के विनाश की बातों को हवा देते हैं तो उद्देश्य दलित-पिछड़ों का राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होता है.
आंबेडकर हैं एकता के प्रतीक-पुरुष
बाबासाहेब डॉ भीम राव आम्बेडकर ने अपनी विद्वता और राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए देश को एक संवैधानिक सूत्र में बांधने का काम किया. संविधान सभा में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, किंतु बाबा साहेब की उपलब्धि दलीय राजनीतिक विमर्श से परे है. भारतीय जाति व्यवस्था की जड़ता से दुखी होकर अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म अपना लिया था. वे बुद्ध के जीवन दर्शन से प्रभावित थे. उन्होंने समाज को गरीबी और अशिक्षा से मुक्ति दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया था. वर्तमान समय में कई नेता उनकी तस्वीरों का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार कर रहे हैं. साहित्य में भी दलित चेतना का स्वर मुखर है, लेकिन यह स्वानुभूति और सहानुभूति के द्वंद्व में उलझी हुई है. इस स्थिति से बचने की जरूरत है. साहित्य को जातियों में बांट कर नहीं देखा जा सकता है.
हालांकि यह तर्क जायज है कि प्रकृति के सुकोमल कवियों का ध्यान दलितों की दुर्दशा की ओर क्यों नहीं गया. "दलित विमर्श" ने साहित्य एवं राजनीति दोनों को प्रभावित किया है. प्रेरणादायी साहित्य अच्छी राजनीति की जननी होती है. समाज की पीड़ा साहित्य में अभिव्यक्ति पाती है और एक चिंतनशील वर्ग तैयार होता है जो जातियों के दायरे से बाहर निकलने की सामर्थ्य रखता है. समकालीन दलित राजनीति के प्रतिनिधि सनातन धर्म की परम्पराओं से भयभीत नहीं हैं. वे छद्मधर्मनिरपेक्षतावादियों की हकीकत जान चुके हैं.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]
 “ हेमंत सोरेन को मिला माई-माटी का साथ, पीके फैक्टर एनडीए के काम आया, तेजस्वी का ‘पारिवारिक समाजवाद हुआ फेल’
“ हेमंत सोरेन को मिला माई-माटी का साथ, पीके फैक्टर एनडीए के काम आया, तेजस्वी का ‘पारिवारिक समाजवाद हुआ फेल’

ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस