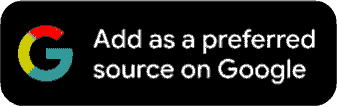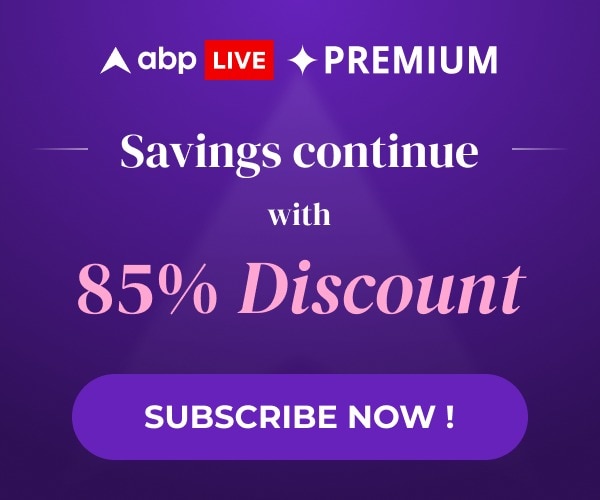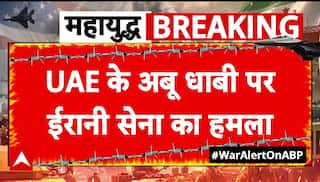क्या भारत को चाहिए नया संविधान, बहस और मायने, नागरिक महत्व के नजरिए से समझने की ज़रूरत

भारत विविधताओं से भरा-पूरा एक ऐसा देश है, जो पिछले 76 साल से इस विविधता को संजोकर पूरी दुनिया में एकता और अखंडता की मिसाल बना हुआ है. हालांकि भारत को हम विवादों पर बहस का देश भी कह सकते हैं. यहां हर दिन किसी न किसी मुद्दे पर विवाद और बहस सुर्खियों में होते ही हैं. ताज़ा बहस और विवाद नए संविधान की ज़रूरत से जुड़ा है.
बिबेक देबरॉय के आर्टिकल पर विवाद
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय 15 अगस्त को एक अख़बार में आलेख लिखते हैं. इस आलेख का शीर्षक "देयर इज़ ए केस फॉर वी द पीपल टू इंब्रेस अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन" होता है. इस आलेख में वो देश के लिए नए संविधान की ज़रूरत पर प्रकाश डालते हैं. इसके बाद उनके इस आलेख पर बहस और विवाद का दौर शुरू हो जाता है. तमाम विपक्षी दलों के नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगती है. राजनीति से इतर सामाजिक संगठनों की ओर से भी प्रतिक्रिया आती है.
नए संविधान की ज़रूरत पर बहस
दरअसल यही आलेख कोई और शख्स लिखा होता, तो शायद इतना विवाद या बहस देखने को नहीं मिलता. बिबेक देबरॉय प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन हैं, इसलिए इसे उस संदर्भ में देखा गया. विपक्ष की ओर से ये सवाल भी खड़ा किया जा रहा है कि क्या ये सब प्रधानमंत्री की मर्ज़ी से हो रहा है.
विवाद बढ़ने पर निजी विचार बताया
हालांकि विवाद बढ़ने पर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद और बिबेक देबरॉय दोनों की तरफ से स्पष्टीकरण आता है. ईएसी-पीएम की ओर से कहा जाता है कि ये बिबेक देबरॉय की निजी राय थी. ये किसी भी तरह से प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद या भारत सरकार के विचारों को नहीं दर्शाता है. बिबेक देबरॉय भी कमोबेश इसी लाइन पर बाद में सफाई देते हैं. उनके स्पष्टीकरण का भी यही आशय है कि इसे उनकी व्यक्तिगत राय मानी जाए. इसका कोई भी सरोकार प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद से नहीं है.
संविधान को अपनाए हुए 73 साल से ज्यादा
भारत को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए 76 साल बीत चुके हैं. इस साल 15 अगस्त को हम सबने अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया. उसके साथ ही भारत के संविधान को लागू हुए भी 73 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है. संविधान सभा में संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था. उसके बाद पूरी तरह से संविधान के सभी प्रावधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुए और ये हमारा गणतंत्र दिवस बन गया. संविधान के लागू होने के साथ ही भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बन गया था. बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा जाता है. यानी इस संशोधन के जरिए संविधान की उद्देशिका (PREAMBLE) में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया जाता है.
बिबेक देबरॉय नए संविधान के पक्ष में
बिबेक देबरॉय ने अपने आलेख में नए संविधान की ज़रूरत को लेकर जिन बिंदुओं या पहलुओं को उठाया है, उनमें सबसे प्रमुख है लंबा वक्त का बीत जाना. संविधान के लागू हुए 73 साल हो गए हैं. बिबेक देबरॉय का आशय है कि इतने लंबे वक्त के बाद किसी भी देश की जरूरतें बदल जाती है और उन ज़रूरतों को सिर्फ़ संविधान संशोधन के जरिए पूरा नहीं किया जा सकता है. बिबेक देबरॉय ने अपने इस तर्क के लिए एक अध्ययन का भी हवाला दिया है, जिसके मुताबिक लिखित संविधान का जीवनकाल सिर्फ़ 17 साल होता है. बिबेक देबरॉय ने मौजूदा संविधान को औपनिवेशिक विरासत कहा है और इसके लिए तर्क दिया है कि मौजूदा संविधान बहुत हद तक भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है.
कार्यपालिका पर लिमिटेशन का मुद्दा
बिबेक देबरॉय ने अपने आलेख में जो एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है, वो है मौजूदा संविधान के संशोधन में कार्यपालिका के ऊपर न्यायपालिका की ओर से लिमिटेशन तय होने का. दरअसल 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर या मूल ढांचे की अवधारणा को लाते हुए ये फैसला दिया था कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसमें संविधान के मूल ढांचे से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केंद्र में जो भी सरकार होती है, उसके लिए संविधान संशोधन में एक तरह का लिमिटेशन लग जाता है.
1973 के फैसले के बाद केंद्र सरकार की ओर से संसद से कई ऐसे कानून पारित कराए गए, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक तौर से अवैध करार दिया गया और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे छेड़छाड़ को आधार बनाया. ताज़ा मामला जो ज्यादातर लोगों के जेहन में है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा संविधान संशोधन कानून है. संसद से 2014 में पारित राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC)कानून और उससे जुड़े संविधान संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 16 अक्टूबर 2015 को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को संविधान के मूल ढांचे में छेड़छाड़ माना था.
मूल ढांचे की अवधारणा और नया संविधान
बिबेक देबरॉय अपने आलेख में सरकार पर लगे इस पाबंदी के मसले को ही प्रमुखता से उठाते हुए ज़ोर देते हैं कि देश को नए संविधान की जरूरत है. वे अपने आलेख में कहते हैं कि 1973 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संविधान का बुनियादी संरचना नहीं बदला जा सकता है. उनका कहना है कि ये फैसला वर्तमान संविधान पर लागू होता, लेकिन अगर नया संविधान ही बन जाए, तो फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट का मूल ढांचे से जुड़ा नियम लागू नहीं होगा. बिबेक देबरॉय का कहना है कि सिर्फ़ चंद संशोधनों से काम नहीं तलने वाला.
संविधान में शामिल मूल्यों से जुड़ा सवाल
बिबेक देबरॉय ने अपने आलेख में एक और अहम मुद्दा उठाया है, जो शायद विवाद का बड़ा कारण भी है. संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्द शामिल हैं. बिबेक देबरॉय अपने आलेख में मौजूदा वक्त में इन शब्दों के होने के मतलब को लेकर सवाल पूछते नज़र आते हैं. इस आधार पर वे नए संविधान की जरूरत बताते हैं.
क्या इसे सरकार की मर्जी के तौर पर देखें?
ये तो हो गई बिबेक देबरॉय के आलेख में उठाए गए बिंदुओं की बात. सबसे बड़ा सवाल उठता है कि बिबेक देबरॉय फिलहाल जिस पद पर हैं, उस पर रहते हुए एकदम से नए संविधान की मांग को उठाते हुए आलेख लिखना कितना उचित है. वे ईएसी-पीएम के चेयरमैन है. ये एक गैर संवैधानिक स्वतंत्र निकाय है, जिसका गठन प्रधानमंत्री करते हैं. ये परिषद प्रधानमंत्री को आर्थिक मामलों में सलाह देने का काम करता है. इस नाते ये परिषद पूरी तरह से सरकार से जुड़ा हुआ है और जब इसके चेयरमैन इतनी बड़ी मांग अपने आर्टिकल के जरिए उठाएंगे, तो स्वाभाविक है कि आम लोगों में ये परसेप्शन बनेगा ही कि क्या ये सरकार की ओर से आने वाला विचार है.
औपनिवेशिक विरासत बताना कितना सही?
बिबेक देबरॉय ने जो औपनिवेशिक विरासत की बात उठाई है, तो ये समझना होगा कि भारत का संविधान पूरी तरह से भारतीयों के अथक योगदान से बना है. संविधान सभा से बना है. ये जरूर हैं कि संविधान को बनाने में संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के तमाम संविधान और कानून का अध्ययन किया. भारत का संविधान करीब 60 देशों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया था. उस वक्त ये कोशिश की गई थी कि इन तमाम संविधानों में शामिल वैसे तत्व जो भारत के भविष्य के लिहाज से तर्कसंगत हो सकते हैं, उन्हें भारतीय सामाजिक जाना-बाना के हिसाब से मॉडिफाई कर संविधान में जगह दी जाए.
जैसे मूल अधिकार की धारणा अमेरिका से प्रेरित है, तो संसदीय शासन प्रणाली यूनाइटेड किंगडम से. उसी तरह राज्य की नीति निदेशक तत्वों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई है., वहीं आपात उपबंधों के लिए जर्मनी के संविधान से प्रेरणा ली गई है. ऐसा नहीं है कि सीधे-सीधे उन प्रावधानों को शामिल कर लिया गया था, बल्कि भारतीय समाज और प्रशासनिक ज़रूरतों को ध्यान में रखकर उनमें बदलाव के साथ शामिल किया गया था.
भारत शासन अधिनियम, 1935 का बड़ा हिस्सा
ये भी सही है कि भारत के संविधान का एक बड़ा हिस्सा भारत शासन अधिनियम, 1935 से लिया गया है. उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि संविधान निर्माता संविधान में प्रशासनिक ब्यौरा भी चाहते थे. उनको इस बात की चिंता थी कि भारत नया-नया आज़ाद हुआ है और मौजूदा हालात में प्रशासनिक ब्यौरा को संविधान में जगह नहीं दी गई या प्रशासन के रूप को स्पष्ट नहीं किया गया, तो भविष्य में सरकार में रहने वाले लोग सत्ता को बरकार रखने और राजनीतिक लाभ के लिए संविधान में बड़ा बदलाव कर सकते हैं.
संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. भीम राव अंबेडकर ने इसके महत्व को समझते हुए कहा भी था कि प्रशासन के रूप में परिवर्तन किए बिना संविधान का दुरुपयोग करना बिल्कुल संभव है. आज़ादी और प्रशासनिक-संवैधानिक अनुभवों के लिहाज़ से नवजात होने की वजह से संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान में प्रशासन का पूरा खाका हो. बाकी देशों के संविधान में इतने प्रशासनिक ब्यौरे शामिल नहीं है. चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो.
प्रशासनिक ब्यौरे की वजह से उस वक्त 1935 के कानून के प्रावधानों से यहां के लोग परिचित थे और यही कारण था कि 1935 के कानून के बड़े हिस्से को कुछ बदलाव के साथ भारत के संविधान में अपनाया गया. हालांकि धीरे-धीरे भारतीय समाज की ज़रूरतों के हिसाब से पिछले 73 साल में उनमें काफी बदलाव भी किया गया है. संविधान सभा ने जो संविधान स्वीकार किया, उसमें पिछले 73 साल के दौरान संविधान रूपी गंगा में काफी पानी बह चुका है.
ये तथ्य है कि अब तक भारत के संविधान में 105 बार संशोधन हो चुके हैं. ये संशोधन भारत और भारत के लोगों की बदलती ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही किए गए हैं. इंदिरा गांधी सरकार के दौरान 1976 के 42वें संविधान संशोधन कानून और मोरारजी देसाई सरकार में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 के जरिए तो संविधान में काफी बदलाव किया गया. 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की व्यापकता को देखते हुए उसे मिनी या लघु संविधान भी कहा जाता है.
सिर्फ ये कहना कि संविधान सभा ने उस वक्त जिस संविधान को तैयार किया, उसमें 1935 के कानून का बड़ा हिस्सा शामिल किया और इस दलील के आधार पर भारत के संविधान को औपनिवेशिक विरासत करार देना, ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है.
मूल ढांचे की अवधारणा से जुड़े फैसले का महत्व
बिबेक देबरॉय ने अपने आलेख में नए संविधान के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के 1973 के मूल ढांचे की अवधारणा से जुड़े फैसले का तर्क दिया है. 1973 के फैसले को समझने के लिए उस वक्त की सरकार के रवैये को समझना होगा. उस समय इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थीं. सुप्रीम कोर्ट से 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भराती मामले में फैसला आता है. इंदिरा गांधी 24 जनवरी 1966 को देश की प्रधानमंत्री बनी थीं. केशवानंद भारती केस में फैसले से पहले इंदिरा गांधी इस दौरान बतौर प्रधानमंत्री 13 बार संविधान संशोधन कर चुकी थीं. 30वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1972 के जरिए तो इंदिरा गांधी ने संसद से पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने अपीलीय अधिकार को ही सीमित कर दिया था.
कार्यपालिका की निरंकुशता से है संबंध
उससे पहले इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद से 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 बनवाया. इस अधिनियम के जरिए सरकार ने अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया. दरअसल अनुच्छेद 13 में ही सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार है कि वो संसद के किसी भी कानून की न्यायिक समीक्षा कर सके, जब मामला मौलिक अधिकार की कटौती या उसे कम करने से जुड़ा है. इंदिरा गांधी सरकार ने 24वें संशोधन अधिनियम से ये व्यवस्था बना दी कि संसद को मौलिक अधिकारों को सीमित करने और किसी भी मौलिक अधिकार को वापस लेने की शक्ति है और ऐसा कोई भी कानून अनुच्छेद 13 के दायरे में आने वाला कानून नहीं माना जाएगा. इस तरह से इसके जरिए इंदिरा गांधी की सरकार ने मौलिक अधिकार में कटौती या वापसी से जुड़े हर तरह के कानून को सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा के दायरे से ही बाहर कर दिया.
राजनीतिक फायदे के लिए नहीं बने कानून!
केशवानंद भारती केस में आदेश के जरिए मूल ढांचे की अवधारणा को लाकर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भविष्य में कोई भी सरकार संविधान संशोधन के नाम पर राजनीतिक फायदे के लिए नागरिक अधिकारों में कटौती या उनसे खिलवाड़ नहीं करे. किसी भी देश के संविधान के लिहाज़ से नागरिक और नागरिक अधिकार से बढ़कर कुछ नहीं होता है.
अगर संसदीय व्यवस्था में सरकार का रवैया तानाशाही जैसा होने लगेगा, तो ये संविधान के मूल सिद्धांतों और आदर्शों के लिए खतरा साबित हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा लाकर भविष्य में इस खतरे की संभावना को खत्म कर दिया था. अब अगर नया संविधान आ जाए और उसके जरिए मूल ढांचे का लिमिटेशन सरकार पर लागू नहीं हो, तो फिर ये भारत के लोगों और भारतीय संसदीय प्रणाली के लिए सहीं नहीं होगा. सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचे की अवधारणा के जरिए कार्यपालिका की निरंकुशता की संभावना को खत्म करने का प्रयास किया था. अब नया संविधान होने पर उस निरंकुशता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.
संविधान में शामिल मूल्य और आदर्श भारत की ताक़त
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे मूल्य किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का आधार होता है. बिबेक देबरॉय के आलेख में मौजूदा वक्त में इन शब्दों की प्रासंगिकता को लेकर भी बात रखी गई है. भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ. आज़ादी के वक्त भारत के पास धार्मिक, जातीय, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता से जड़ी एक समृद्ध विरासत थी. नए-नए आज़ाद हुए देशों के लिए यही विविधता उसके खंडित होने का कारण बन जाते हैं, लेकिन भारत के मामले में ये विविधता हमारी ताकत बन गई. इसका जीता जागता सबूत ये है कि आज़ादी के 76 साल बाद भी भारत एकजुट है और वैश्विक पटल पर उन्नति की नई इबारत लिख रहा है.
इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह संविधान में निहित मूल्य हैं. समाजवादी, पंथनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, न्याय, स्वतंत्रता और समानता ही वे मूल्य हैं, जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है और उस वजह से हम आज भी पूरी अडिगता के साथ एक राष्ट्र के तौर पर मजबूत पहचान के साथ अस्तित्व में हैं. अगर नए संविधान में इन मूल्यों को उतना महत्व नहीं मिला, जितना मौजूदा संविधान में है, तो फिर देश की एकजुटता, राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ बंधुता को सुनिश्चित करना इतना आसान नहीं रह जाएगा.
संविधान समीक्षा आयोग और विवाद
ऐसा नहीं है कि देश में संविधान की समीक्षा की कोशिश नहीं हुई है. संशोधन के जरिए बदलाव तो कई हुए हैं, इसके साथ ही संविधान समीक्षा के लिए आयोग भी बने हैं. फरवरी 2000 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग बनाया. 11 सदस्यीय इस आयोग के अध्यक्ष पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एम एन वेंकटचलैया बनाए गए. हालांकि विपक्ष के एतराज के बाद वाजपेयी सरकार ने आयोग के विषय क्षेत्र को सीमित कर दिया. आयोग को अपनी सिफारिशों में इस बात का ध्यान रखना था कि उससे संविधान के मूल ढांचे पर असर नहीं पड़े.
तीन कार्यकाल विस्तार के बाद इस आयोग ने 31 मार्च 2002 को अपनी रिपोर्ट सौंपी. 1979 पेज और दो वॉल्यूम में बनी इस रिपोर्ट को उस वक्त कानून मंत्री अरुण जेटली ने आयोग से रिसीव किया. हालांकि विपक्ष के साथ ही देश के अलग-अलग तबकों से मिली आपत्तियों की वजह से उस वक्त सरकार ने आयोग की रिपोर्ट पर आगे बढ़ने का विचार त्याग दिया.
नागरिक महत्व लिहाज़ से हो बदलाव
ये बात सही है कि बिबेक देबरॉय ने विवाद बढ़ने के बाद इसे निजी विचार बताया और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने भी इस पर सफाई दी. लेकिन ये भी उतना ही तथ्यपूर्ण हैं कि नया संविधान भले ही न बने, लेकिन जिन मूल्यों और आदर्शों को लेकर संविधान का निर्माण किया गया था, क्या आज़ादी के 76 साल बाद भी हम उनको हासिल कर पाए हैं या हासिल करने के करीब पहुंच पाए हैं, इसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए.
'हम , भारत के लोग' सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोपरि
भारत के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है और इस प्रस्तावना की शुरुआत..हम , भारत के लोग (WE, THE PEOPLE OF INDIA) से होती है. भारतीय संविधान के मुताबिक हमारे देश में सर्वोपरि अगर कोई है तो यहां के नागरिक हैं, यहां के लोग हैं. संविधान की शुरुआत इसी भावना के साथ होती है. नया संविधान बनाने के पीछे जो भी सोच हो, उससे ज्यादा महत्व की बात ये हैं कि आज़ादी के 76 साल बाद भी ये देखना होगा कि नागरिक सर्वोपरि की भावना व्यवहार में हम कितना उतार पाए हैं. इसकी जरूर समीक्षा होनी चाहिए और इसके लिए संविधान में जो भी बदलाव करना पड़े, सरकार को उस दिशा में जरूर कदम बढ़ाना चाहिए.
सिद्धांत में नहीं, व्यवहार में भी नागरिक ही रहे सर्वोपरि
सैद्धांतिक तौर से आम नागरिक सर्वोपरि हैं, किसकी पार्टी की सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में होगा, ये देश के नागरिक ही तय करते हैं. लेकिन क्या इतने भर से नागरिक व्यवहार में भी सर्वोपरि हो जा रहे हैं, इसे देखना होगा. इस दिशा में न तो कांग्रेस की सरकार, न ही बीजेपी की सरकार और न ही जनता पार्टी की सरकार या फिर नेशनल फ्रंट या यूनाइटेड फ्रंट की सरकार ने संविधान में बदलाव को लेकर ठोस प्रयास किए है. संविधान की नज़र में सैद्धांतिक तौर से हर नागरिक कानून और संविधान के सामने समान है, लेकिन व्यवहार के धरातल पर इसे आज़ादी के 76 साल बाद भी हासिल नहीं किया गया है. इसके लिए संविधान में बदलाव की सख्त दरकार है. अगर उदाहरण से समझें तो वोट देने तक ही देश के नागरिक सीमित हो गए हैं. लोकतंत्र में संसदीय व्यवस्था की संकल्पना को भारत के संविधान में इसलिए जगह दी गई थी, ताकि शासन व्यवस्था में राजशाही और सामंतवादी तत्व की कोई जगह न तो सीधे तौर से हो और न ही अप्रत्यक्ष तरीके से हो.
संविधान में नागरिक से ऊपर कोई नहीं
हालांकि व्यवहार के धरातल पर कुछ और ही होते आया है. नागरिक वोट देकर अपनी जिम्मेदारी पूरा कर लेते हैं. फिर जो पूरा सरकार का तंत्र होता है, विधायिका और कार्यपालिका में जनप्रतिनिधित्व होते हैं, उनका रवैया कुछ अलग ही होते जाता है. संविधान के मुताबिक सरकार के नुमाइंदे जनता के सेवक होते हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे और विधायिका के नुमाइंदे यानी सांसद, विधायक कुछ इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं, जैसे वे आम नागरिक से ऊपर हैं. हम कह सकते हैं कि सामंतवादी रवैया रूप बदलकर संसदीय व्यवस्था में मौजूद नज़र आता है. ये किसी एक पार्टी से जुड़ा मसला नहीं है. चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, या बीजेपी की या फिर अन्य दलों की..इस तरह की प्रवृत्ति हर जगह देखी जाती है. संविधान में इसके लिए तत्काल बदलाव कर प्रावधान किए जाने की जरूरत है कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में नागरिक सबसे बड़ा वीआईपी होगा, सैद्धांतिक तौर से भी और व्यवहार के स्तर पर भी.
न्यायिक व्यवस्था में भी आम-ख़ास का फ़र्क़
उसी तर्ज़ पर न्यायपालिका में भी हम देखते हैं कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च अदालत तक आम आदमी और रसूखदार आदमी के बीच किस प्रकार का गैप बना हुआ है. आम नागरिक की सुप्रीम कोर्ट में पहुंच और रसूखदार आदमी की पहुंच में ज़मीन-आसमान का फ़ासला है. एक उदाहरण के तौर पर समझें तो चूंकि ताजा मामला है, इसलिए राहुल गांधी के मानहानि मामले को ही ले लें. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत आपराधिक मानहानि के मामले में 23 मार्च को दोषी ठहराते हुए दो साल की सज़ा सुनाती है. उसके बाद सूरत की अपीलीय अदालत और गुजरात हाईकोर्ट से गुजरता हुआ मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट मामले के निपटारे तक राहुल गांधी के कन्विक्शन पर रोक लगा देती है. निचली अदालत से सज़ा मिलने के महज़ 4 महीने और कुछ दिनों में राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि केस में फ़ौरी राहत मिल जाती है.
सवाल उठता है कि क्या एक आम नागरिक इसी तरह के आपराधिक मानहानि से जुड़े केस में निचली अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद 4 महीने में सुप्रीम कोर्ट से राहत पा सकता है, क्या आज़ादी के 76 बाद भी हम वैसी न्यायिक व्यवस्था बना पाए हैं, जिसमें आम नागरिक और रसूखदार या कहें वीआईपी लोगों में फ़ासले को मिटा पाए हैं. इसका जवाब हर कोई 'नहीं' में ही देगा. राहुल गांधी का जिक्र सिर्फ़ एक उदाहरण के तौर पर है, क्योंकि ये मामला अभी आम से लेकर ख़ास सबके जेहन में है. ऐसे राहुल गांधी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर मेरी कोई आपत्ति नहीं है, बस न्यायिक व्यवस्था में खाई को दर्शाने के लिए ये उदाहरण इस्तेमाल किया गया है. बाकी पिछले 73 साल में इस तरह के बहुतेरे उदाहरण न्यायिक व्यवस्था में भरे पड़े हैं. ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही बात नहीं है. निचली अदालतों और हाईकोर्ट में आम और ख़ास के बीच का फर्क़ पहुंच के स्तर पर अभी भी दिख जाएगा. संविधान में बदलाव इसके लिए होना ही चाहिए.
'वी द पीपल' के लिए हो बड़ा बदलाव
ये तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका से जुड़े मुद्दे हैं, जिनमें आम नागरिकों को संविधान के 'वी, द पीपल ऑफ इंडिया' की भावना के तहत व्यवहार में सर्वोच्च महत्व मिलने से जुड़ा है. किसी राष्ट्र में नागरिक से बड़ा कोई नहीं हो सकता. न तो संसद, न तो कार्यपालिका और न ही न्यायपालिका. यहीं संविधान की भावना भी है और इसी को पाने की दिशा में संविधान में बड़ा बदलाव करना पड़े, तो उस ओर बढ़ने के बारे में सोचा जाना चाहिए. इस तरह से हम कह सकते हैं कि नए संविधान की जगह भारत के मौजूदा संविधान में उन बदलावों की तत्काल ज़रूरत है, जिसके जरिए सिर्फ़ सैद्धांतिक तौर से नहीं, बल्कि व्यवहार में भी नागरिकों को सर्वोपरि माना जाए.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.]