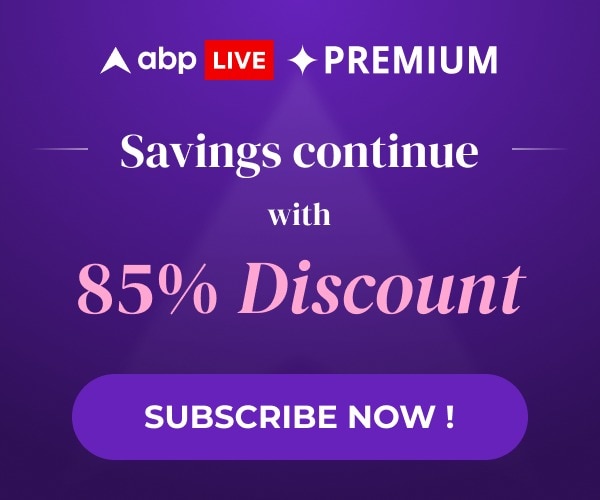इंग्लैंड के अलावा कोई भीः यूरो 2020 फाइनल पर एक भारतीय के कुछ विचार

रविवार की दोपहरें अक्सर विश्राम के लिए होती हैं और खास तौर पर ‘परिवार’ नाम की ‘प्राकृतिक’ सामाजिक संस्था के साथ समय बिताने के लिए. इसके बावजूद कल 11 जुलाई, रविवार को जब इंग्लैंड और इटली यूरो 2020 के फाइनल में एक-दूसरे के सामने थे तो इससे बढ़िया आराम क्या हो सकता था. दोनों टीमें लंबे खिताबी सूखे को खत्म करने के लिए आतुर थीं. इटली ने आखिरी बार ट्रॉफी 1968 में जीती थी और इंग्लैंड ने फुटबॉल का आखिरी अंतरराष्ट्रीय विजय कलश 1966 में चूमा था, जब उसने जर्मनी को विश्व कप फाइनल में 4-2 से हराया था. इंग्लैंड कभी यूरोपीयन कप नहीं जीत सका.
इंग्लैंड कुछ नहीं है अगर यह फुटबॉल खेलने वाला राष्ट्र नहीं है. इस खेल के लिए यहां के लोगों के जुनून की तुलना किसी अन्य देश को लोगों से नहीं हो सकती, मगर इसके दीवाने दुनिया भर में कुख्यात हैं. फुटबॉल को लेकर यहां होने वाले गुंदागर्दी से जैसे उपद्रव पर अमेरिकी पत्रकार बिल बुफोर्ड ने 1990 में किताब लिखी थी, अमंग द ठग्स. जिसमें उनका फोकस मैनचेस्टर युनाइटेड के फैन्स पर था, जिनके साथ बिल ने कई मैचों के लिए लंबी यात्राएं की थीं. उन्होंने पाया कि इन हुड़दंगियों का अपनी टीम के प्रति समर्पण ठीक वैसा ही था, जैसे किसी की धार्मिक भावनाएं होती हैं.
उन्होंने लिखा कि इन उपद्रवियों की टीम के प्रति वैसी ही कट्टर भावनाएं थीं, जैसी इंग्लैंड की राष्ट्रवादी पार्टी द नेशनल फ्रंट के सदस्यों में देखने मिलती हैं. खास बात यह कि वह 1990 में इटली में हुए विश्व कप के दौरान सार्डिनीया में फुटबॉल दंगाइयों के साथ गिरफ्तार किए गए थे और अपने अनुभव से उन्होंने लिखा कि अप्रत्याशित रूप से इस हिंसा में उन्हें ‘आनंद’ मिल रहा था. बुफोर्ड ने लिखा कि यह हिंसा असामाजिकता को नई ‘किक’ देती है, यह भावनाओं को उथल-पुथल कर देने वाला अनुभव है और ऐसा उत्साह-जोश-जुनून पैदा करती है, जो आम तौर पर कृत्रिम ड्रग्स से व्यक्ति हासिल करता है.
लॉस एंजेल्स स्थित घर में बैठ कर रविवार दोपहर को यूरो कप फाइनल देखना, विश्राम के अलावा एक अलग अनुभव था. किसी समय मैं ‘इस खूबसूरत खेल’ की खबरें रखा करता था लेकिन कभी फुटबॉल को लेकर जुनूनी नहीं रहा, जैसे आम तौर पर फैन हुआ करते हैं. मेरे लिए यह खेल कुछ धुंधलके की तरह रहा. मैं समझ नहीं पाता कि कैसे कोई किसी एक टीम का फैन बन जाता है या फिर यह रहस्य ही है कि कैसे कोई इतना डूब जाता है कि वह एक टीम के लिए कर्कश ढंग से चिल्लाने लगता है या दूसरों पर बीयर की बोतलें फेंकते हुए पागलों की तरह लड़ पड़ता है और तोड़फोड़ पर उतर जाता है.
यकीनन कल वेंबले में यही हुआ, जहां हजारों इंग्लिश फैन बिना टिकट स्टेडियम में घुस गए और तोड़फोड़ करते हुए, बेवजह कुछ लोगों से मार-पीट करने लगे, जैसा कि बुफोर्ड ने लिखा है, यह सब केवल इसलिए कि वह मात्र इस बात से उत्तेजित थे कि बस, मैच अब शुरू होने वाला है. निश्चित ही यह उत्साह का वही भाव रहा होगा, जिसने मेरे दोपहर के विश्राम को तीन घंटे के तनाव-पूर्ण माहौल में बदल दिया, जिसमें खेल के तय समय में इंग्लैंड और इटली में कांटे का जोरदार मुकाबला 1-1 से ड्रॉ छूटा.
यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इंग्लैंड को इस फाइनल में होना चाहिए था. मैं ही क्या और भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि सेमी-फाइनल में डेनमार्क के विरुद्ध उसे जो पेनाल्टी किक मिली थी, वहां असल में फाउल था, जिस पर रेड कार्ड दियाखा जा सकता था. मेरे भीतर के हिंदुस्तानी ने आजीवन उपनिवेशवाद का अध्ययन किया है और खास तौर पर भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का. मैं हमेशा सोचता रहा हूं कि इंग्लैंड ने सदा दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया है कि वह ‘ईमानदार’ है और ‘खेल भावना’ को सबसे ऊपर रखता है किंतु सचाई यह है कि 18वीं सदी के दूसरे हिस्से में अपनी बढ़ती हुई ताकत के साथ उसने कभी उन संधियों का सम्मान नहीं किया, जो उसने भारतीय राजाओं से की थी.
तथ्य बताते हैं कि अमेरिका में भी इन गोरों के बंधु-बांधवों ने न केवल स्थानीय लोगों के साथ किए समझौते तोड़े, उनका उल्लंघन किया बल्कि इन लोगों को समूल रूप से नष्ट करने की कोशिशों में भी भरपूर योगदान दिया. अब, जबकि इंग्लैंड को अनावश्यक पेनाल्टी किक मिली थी, यह रेफरी की गलती का नतीजा थी. हालांकि अब इस बारे में परेशान होने का कोई अर्थ नहीं. खैर, जब मैं मैच देखने के लिए अपनी आराम कुर्सी पर लेटा था तो इटली की विजय की उम्मीद बांधे हुए था. हालांकि न तो मैं इटली का फैन हूं और न ही इंग्लैंड का. इस मामले में, जब भी इंग्लैंड और किसी अन्य देश को चुनने की बात आती है तो मैं आम तौर पर स्वर्गीय मार्क मार्केज की शानदार किताब ‘एनी वन बट इंग्लैंड’ (इंग्लैंड के अलावा कोई भी, 2005) के शीर्षक को फॉलो करता हूं. मार्क की यह किताब क्रिकेट, नस्लवाद और राष्ट्रवाद पर है. यद्यपि यहां एक अपवाद है. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैं इंग्लैंड की तरफदारी करता हूं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का नस्लवाद और जातिवाद कहीं अधिक विद्रूप है.
दो मिनिट ही हुए थे और इंग्लिश डिफेंडर ल्यूक शॉ ने इंटरनेशनल मैच में अपना पहला गोल दाग दिया। यूरो फाइनल के इतिहास का यह सबसे तेज गोल था. यह एक बढ़िया गोल था, खूबसूरती से हासिल किया और इंग्लैंड ने पूरी गरज के साथ पूरे टूर्नामेंट की तर्ज पर यहां भी जोरदार शुरुआत की. मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा था लेकिन मैं उपद्रवी फुटबॉल प्रेमी नहीं हूं. यहां तक कि फुटबॉल का साधारण फैन भी नहीं. मैं वेंबले की उस भीड़ और इंग्लैंड के असंख्य पबों की कल्पना कर रहा था, जहां मेरे विचारों की गति से तेज बीयर बह रही थी. मेरे दिमाग में दूसरे खयाल घुमड़ पड़ेः अगर इंग्लैंड जीत जाता है तो ब्रेक्जिट का बचाव करने वाले निश्चित ही दावा करने लगेंगे कि यूरोपियन यूनियन को छोड़ने के बाद इंग्लैंड में फुटबॉल फिर जिंदा हो गया है. फिर से कई लोग आंखें तरेर कर सदियों पुरानी बात दोहराने लगेंगे कि इंग्लैंड आखिर इंग्लैंड है और यूरोप अपनी बदहाली के लिए खुद जिम्मेदार है. सच यह है कि सिर्फ डेनमार्क नहीं, पूरे यूरोप में कुछ गड़बड़ है. सवाल यह नहीं कि इंग्लैंड की जीत का ब्रेक्जिट को लेकर चल रही बहस से कोई संबंध है या नहीं. कई लोगों को विश्वास था कि इंग्डैंल की जीत उसकी आंतरिक संरचना को मजबूत करेगी.
इस बीच, पहले आधे घंटे तक इंग्लैंड मैच पर पूरी तरह हावी रहा, मगर इसके बाद धीरे-धीरे वह अपनी बढ़त को बढ़ाने के बजाय उसे बरकरार रखने के इरादे से खेलने लगा, सुरक्षात्मक अंदाज में. वह सोचने लगा कि वह खेल को धीमा कर दे और घड़ी की सुइयों को बढ़ते जाने दे. मेरा मन हुआ कि कोई इंग्लैंड के कोच गारेथ साउथगेट से कहे कि उसके देश ने एक-चौथाई दुनिया में विशाल साम्राज का विस्तार और यूनियन जैक लहराने का काम केवल कुछ जगहें हथियाने के बाद खामोश बैठ कर नहीं किया. साम्राज्य-निर्माण की तरह फुटबॉल भी एक अनिश्चित-अस्थिर खेल है. मैदान में आखिरी दो-तिहाई समय के खेल में मुख्य रूप से इटली हावी हो गया. यहां हालांकि मैं खेल की प्रशंसा के लिए नहीं हूं और न ही आंकड़ों की बात करूंगा. इटली ने लंबे समय तक गेंद पर कब्जा बनाए रखा. यद्यपि इससे हमें फुटबॉल की सांस्कृतिक राजनीति की कोई खबर नहीं मिलती. 67वें मिनट में वेटरन डिफेंडर बोनूसी ने गोल मार कर खेल को 1-1 से बराबर कर दिया. इसके बाद और आगे के आधे घंटे के ओवरटाइम में यही स्कोर रहा। नतीजा यह कि गेम पेनाल्टी शूटआउट मे चला गया.
यूं तो सामान्य समय और ओवरटाइम ही दिल की धड़कनें इतनी तेज कर देता है कि उत्तेजना को बर्दाश्त कर पाना कठिन हो जाता है. ऐसे में इंटरनेशनल फुटबॉल में पेनाल्टी शूटआउट का चरम किसी को भी दिल का दौरा देने के लिए पर्याप्त कारण हो सकता है. ‘पेनाल्टी शूटआउट’ इस शब्द से जितना समझ में आता है और जो मैं कह रहा हूं, उससे अधिक विस्तार से इसकी व्याख्या होनी चाहिए. सांस्कृतिक इतिहासकारों को इसके बारे में और इस तरह की अन्य यूरोपीय गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डालना चाहिए. यह वैसा है, जैसे कि पहले ‘द्वंद्व’ हुआ करते थे. यह समझ में आता है कि पेनाल्टी बॉक्स में किए गए गंभीर फाउल पर रेड कार्ड दिखा कर पेनाल्टी किक दी जाती है लेकिन यह समझ से परे है कि जब ओवरटाइम भी खत्म हो जाता है तो क्यों दोनों टीमों को पांच-पांच किक गोल में मारने को दी जाती है.
इस ‘पेनाल्टी शूटआउट’ से भी बात न बने तो फिर ‘सडन डेथ’ है. ऐसी कोई पेनाल्टी नहीं है जिससे आप किसी खिलाड़ी की प्रतिभा को आंक सकें. अगर पेनाल्टी शूटआउट कुछ है तो खेल को खत्म करने का एक विचित्र और अजीबोगरीब तरीका. एक तरीके से यह पूरे खिलाड़ियों को दंडित करता है कि उन्होंने तय किए गए समय में कोई सुनिश्चित परिणाम नहीं दिया. यहां तक कि दर्शक के लिए भी ‘पेनाल्टी शूटआउट’ सजा है क्योंकि इस स्तर तक आते हुए हर कोई समझ चुका होता है कि वास्तव में अब किस्मत का ड्रॉ ही नतीजे को सामने लाएगा.
यूरो 2020 के फाइनल का पेनाल्टी शूटआउट हाल के वर्षों में अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल के सबसे दिल दहलाने वाले अध्यायों में शामिल रहेगा. पहले हम नतीजा देख लेः इटली 3, इंग्लैंड 2। कोच साउथगेट ने संभवतः इस इरादे के साथ खेल के अंतिम क्षणों में दो सब्सटीट्यूट्स -मार्कस रेशफोर्ड और जाडन सांचो- को मैदान में उतारा कि इससे वे संभावित पेनाल्टी किक लेने के अधिकारी हो जाएंगे. 19 साल के बुकायो साका को भी 70वें मिनिट के करीब सब्सटीट्यूट के रूप में उतारा गया. इस प्रकार पांच में से पेनाल्टी लेने वाले दो खिलाड़ी ऐसे थे, जिन्हें फुटबॉल की शब्दावली में ‘फ्रेश लेग्स’ कहा जाता है और तीसरा एक किशोर था, जिसने किसी अंतरराष्ट्रीय मैच में कोई पेनाल्टी किक नहीं ली थी. यह सब ऐसे वक्त में हो रहा था जब इंग्लैंड के लिए गौरवशाली क्षण का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था. दो पेनाल्टियों के बाद इंग्लैंड 2-1 से आगे था. लेकिन स्कोर तब बराबर हो गया जब इटैलियन गोलकीपर ने सांचो की पैनाल्टी रोक ली. इसके बाद रेशफोर्ड ने पोस्ट में गेंद मार दी. तब इंग्लैंड का पूरा भार साका के नाजुक कंधों पर आ गया, जबकि इटलीके पेनाल्टी एक्सपर्ट जॉर्गिनो तक इस अहम मौके पर नाकाम साबित हुए.
निःसंदेह इस खेल का स्वभाव ही ऐसा है कि फैन्स दूसरी टीम की भावनाओं की कद्र नहीं करते. न ही वे अपनी टीम की गलतियों को माफ करते हैं. इसके बाद लंबे समय तक साका की अनुभवहीनता की बातें होती रहेंगी, इटली के गोलकीपर के शानदार बचाव पर चर्चाएं होंगी या फिर कोच के द्वारा की गई गलतियों का भी विश्लेषण होगा परंतु यह बात कभी नहीं थमने वाली कि साका ने मौके पर गेंद गोल में नहीं डाली. कोई इस तथ्य पर बात नहीं कर रहा कि अगर साका ने गेंद को नेट में डाल दिया होता तो इंग्लैंड न केवल स्कोर बराबर कर लेता बल्कि खेल को ‘सडन डेथ’ में ले जाता.
वर्तमान दुनिया में मनुष्यता की स्थिति को देखते हुए जो बातें नहीं कही जानी चाहिए, वह बातें अब कही जा रही हैं. रेशफोर्ड, सांचो और साका श्वेत खिलाड़ी नहीं हैं और जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, इंग्लैंड तो इंग्लैंड है, उनका मानना है कि इन खिलाड़ियों को नोटिस दिए जाने चाहिए और नफरत से कुचल दिया जाना चाहिए. इंग्लैंड की पराजय के कुछ मिनट बाद ही तीनों खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां दी जाने लगीं, अपशब्द कहे जाने लगे. साका नाइजीरियन मूल के हैं लेकिन उनका जन्म और लालन-पालन ब्रिटन में हुआ, बावजूद इसके कुछ फैन्स यह कहने से नहीं चूके कि उन्हें वापस नाइजीरिया भेज दिया जाना चाहिए. इंग्लैंड के सोशल मीडिया में इन खिलाड़ियों को बंदर बताती हुई इमोजी की बाढ़ आई हुई है.
इस बीच फुटबॉल एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड ने कड़े शब्दों में वक्तव्य जारी करके इस ‘भेदभाव की निंदा की’ और कहा कि ‘ऑनलाइन मीडिया में हमारे कुछ खिलाड़ियों पर की जा रही नस्लभेदी टिप्पणियों से हैरान हैं. इस घृणास्पद व्यवहार को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता.’ खिलाड़ियों को बंदर कह कर चिढ़ाने की इंग्लैंड समेत पूरे यूरोप के फुटबॉल मैदानों में पुरानी परंपरा है. पूर्वाग्रहों को जड़ से उखाड़ने, नस्लवाद को खत्म करने और जन-विविधता को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभी बहुत काम किया जाना बाकी है. सामान्य उदारवादियों को इस मुद्दे पर साधारण टिप्पणियां करने के बजाय असाधारण ढंग से विचार करने की जरूरत है. यही वजह है कि क्यों जब मैं कह रहा था कि अगर मैं इंग्लैंड की पराजय की कामना कर रहा हूं तो उसी वक्त इटली की जीत की उम्मीद भी नहीं रख रहा था.
ब्राजीलवासियों की तर्ज पर फुटबॉल को कभी-कभी ‘एक खूबसूरत खेल’ कहा जाता है. दुनिया के इस प्रतिष्ठित खेल की अपनी खूबियों के अलावा इसकी विशेषता यह है कि किसी भी टीम में खिलाड़ियों की विविधता संभव है. यह इंग्लैंड के लिए गर्व का विषय है कि उसकी राष्ट्रीय टीम में रेशफोर्ड, सांचो और साका जैसे खिलाड़ियों ने जगह बनाई है. जबकि नीली जर्सी वाली इटली की राष्ट्रीय टीम का स्वरूप मुख्यतः क्षेत्रीय या प्रांतीय जैसा है. 2021 में भी अधिकाधिक मनसिनी, बोनुची, चिएलिनी, लोरेंजो, स्पिनाजोला और बर्नार्डेस्की ही उसमें नजर आ सकते हैं. इटली में भले ही पुनर्जागरण का जन्म हुआ लेकिन उसकी फुटबॉल टीम में प्राचीन परंपरा के अवशेष ही हैं.
फुटबॉल का भविष्य न तो इंग्लैंड से है और न ही इटली से. न ही जर्मनी, स्पेन, डेनमार्क या फ्रांस या किसी अन्य देश की टीम से. अगर हमें सभ्य होना है तो किसी भी खेल का भविष्य इस बात में निहित है कि हम खिलाड़ियों को विजेता या पराजित के रूप में देखना बंद करें. खिलाड़ी जब केवल खेलने के लिए खेलते हैं तो हमारे भीतर सोच की सीमाओं को खत्म कर कर देते हैं. खेल को सीमित उद्यम के रूप में देखने की आदत बदलने में हमें शायद दशकों लगें या इसमें पीढ़ियां लग जाएं, जबकि खेलों में जीवन के विभिन्न आयामों को समझने अपार संभावनाएं छुपी हुई है.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस