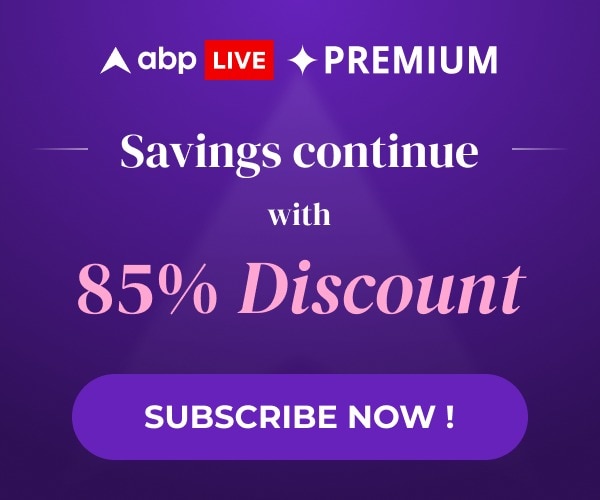रूस और अमेरिका के झगड़े में कैसे बना तालिबान?

तालिबान. इस वक्त दुनिया के सबसे बड़ खतरों में से एक, जो अफगानिस्तान पर हर बीतते दिन के साथ अपना कब्जा बढ़ाता जा रहा है. और हर बढ़ते कब्जे के साथ बढ़ता जा रहा है दुनिया पर खतरा, जिससे निबटने के लिए अब रूस और अमेरिका जैसे देश भी परेशान हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं इस तालिबान को पैदा करने वाले भी रूस और अमेरिका ही हैं, जिनके अफगानिस्तान में हुए आपसी झगड़े में इस संगठन से सिर उठाया था और फिर उन्हीं के लिए बड़ा खतरा बन गया था. आखिर क्या है इस तालिबान का इतिहास, आखिर कौन देता है इस आतंकी संगठन को पैसे, कहां से मिलते हैं इसको हथियार और क्यों अब ये अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं.
साल था 1979. वो वक्त जब दुनिया की दो महाशक्तियां अमेरिका और रूस आपस में शीत युद्ध में उलझे हुए थे. उस वक्त अफगानिस्तान पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान यानी कि पीडीपीए का शासन था. पीडीपीए खुद को रूस के करीब पाता था और उसके इशारे पर चलता रहता था. तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे नूर मोहम्मद ताराकी. और नूर मोहम्मद ताराकी के बाद दूसरे नंबर पर माने जाते थे हफीजुल्ला अमीन. हफीजुल्ला ताराकी के करीबी हुआ करते थे. लेकिन 1979 का आधा साल बीतते-बीतते ताराकी और अमीन के बीच खटपट की खबरें आने लगी थीं. हालांकि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला. इस दौरान सितंबर के दूसरे हफ्ते में ताराकी विदेश दौरे पर गए थे. ताराकी के खास लोगों ने कहा कि उनकी गैरमौजूदगी में अमीन ताराकी की हत्या की प्लानिंग कर रहे थे. ताराकी ने अपने खास चार लोगों से अमीन की हत्या करने का आदेश दे दिया. लेकिन बात लीक हो गई और अमीन बच गए.
इस बीच 11 सितंबर, 1979 को ताराकी मास्को से काबुल लौटे. एयरपोर्ट पर अमीन मौजूद थे. अमीन ने अपनी ताकत को दिखाने के लिए ताराकी के प्लेन को लैंड करवाने में देर कर दी. नाराज तराकी ने अमीन को पद से बर्खास्त करने की कोशिश की. तराकी अड़ गए. कहा कि पद से तो हटना ताराकी को ही चाहिए, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं और शराब के लती हो गए हैं. उस दिन बात खत्म हुई. अगले दिन 12 सितंबर को ताराकी ने अमीन को राष्ट्रपति भवन में खाने पर बुलाया. लेकिन अमीन ने कहा कि वो लंच करने जाने की बजाय इस्तीफा देना पसंद करेंगे. फिर रूस के अंबेसडर पुजनोव की पहल पर अमीन ताराकी के यहां 14 सितंबर को लंच पर गए. वहां सुरक्षाकर्मियों ने अमीन पर फायरिंग कर दी. इस दौरान पुलिस के मुखिया सैयद दाउद तरून मारे गए. हालांकि अमीन बच निकले और उन्होंने सेना को हाई अलर्ट पर कर दिया.
उसी 14 सितंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे सेना के टैंक राष्ट्रपति भवन के सामने राष्ट्रपति ताराकी को बंधक बनाने के लिए तैयार थे. 16 सितंबर की रात 8 बजे रेडियो काबुल ने सूचना दी कि अब राष्ट्रपति ताराकी अब अपनी जिम्मेदारी निभाने में असमर्थ हैं, लिहाजा पोलितब्यूरो ने आमीन को नया नेता चुन लिया है. आमीन को लगता था कि पूरा सोवियत यूनियन उसके साथ है, लिहाजा उसने ताराकी को गिरफ्तार कर लिया और फिर 8 अक्टूबर, 1979 को तीन लोगों ने तकिए से गला दबाकर ताराकी की हत्या कर दी. आमीन के दबाव में मीडिया ने कहा कि बीमारी की वजह से ताराकी की मौत हो गई है.
लेकिन इस पूरे प्रकरण से यूएसएसआर के मुखिया लियोनिड ब्रेखनेव गुस्सा हो गए. उन्हें इस दौरान ये सूचना मिली कि हफीजुल्ला अमीन अमेरिका के पाले में जाने को तैयार है. सोवियत यूनियन के सामने ये भी साफ ही था कि अफगानिस्तान में सत्ताधारी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान कमजोर हो गया है. ऐसे में ताराकी की हत्या के करीब तीन महीने बाद 24 दिसंबर, 1979 को सोवियत यूनियन की 40वीं आर्मी बटालियन को बॉर्डर पार करके अफगानिस्तान में दाखिल होने का आदेश दे दिया. सोवियत सेनाएं अफगानिस्तान पहुंची और फिर हुआ ऑपरेशन स्टॉर्म 333. इस ऑपरेशन के तहत सोवियत सेनाओं ने हफीजुल्ला अमीन की हत्या कर दी. इस दौरान करीब 300 से ज्यादा अफगान सैनिक मारे गए और 1700 से ज्यादा सैनिकों ने सोवियत सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया. सोवियत सेनाओं ने बाबराक कमाल को अफगानिस्तान का नया राष्ट्रपति बना दिया.
लेकिन अफगानिस्तान में दाखिल हुए सोवियत यूनियन की वजह से वैश्विक समीकरण बदल गए. शीत युद्ध के दूसरे छोर पर काबिज अमेरिका ने इसे सोवियत यूनियन के खिलाफ मौके के तौर पर लिया. अमेरिका के साथ पाकिस्तान, सऊदी अरब और चीन जैसे देश भी आ गए, जिन्होंने उन अफगानी लड़ाकों से हाथ मिला लिया, जो सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे. इस लड़ाई में अमेरिका और उसके सहयोगियों ने उन मुजाहिदीन और अरब-अफगानियों का साथ दिया, जो सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहे थे. इनमें से एक बड़ा नाम ओसामा बिन लादेन का भी था, जिसकी अमेरिका सिर्फ इसलिए मदद कर रहा था, क्योंकि वो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेनाओं के खिलाफ लड़ रहा था. और इन्हीं मुजाहिदिनों में एक और ग्रुप था, जो सोवियत सेनाओं से लड़ाई ले रहा था. इस ग्रुप का नाम था तालिब.
जनवरी 1980 में 34 इस्लामिक देशों के विदेश मंत्रियों ने सामूहिक तौर पर मांग की कि सोवियत यूनियन की सेनाओं को अफगानिस्तान से बाहर जाना होगा. और आपको पता है कि उस वक्त भारत किसके साथ खड़ा था. भारत तब सोवियत यूनियन के साथ खड़ा था और अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के दाखिल होने को सही ठहरा रहा था. लेकिन अमेरिका, चीन, पाकिस्तान और दूसरे देशों ने हथियारों के साथ ही पैसे से भी मुजाहिदिनों और अरब-अफगानियों की मदद करनी शुरू कर दी. अमेरिकी एजेंसी सीआईए ने पाकिस्तान की आईएसआई से हाथ तक मिला लिया. और नतीजा ये हुआ कि मुजाहिदीन अफगानिस्तान में मज़बूत होते गए.
सोवियत यूनियन का इरादा था कि वो छह महीने-एक साल के अंदर अफगानिस्तान में हालात काबू में कर लेगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सोवियत सेनाएं करीब 9 साल तक अफगानिस्तान में फंसी रहीं. इस बीच जब सोवियत में सत्ता बदली और मिखाइल गोर्बाचोव का शासन आया तो उन्होंने कहा कि वो धीरे-धीरे करके अफगानिस्तान से अपनी सेनाओं को वापस बुला लेंगे. सबसे पहले गोर्बाचोव ने अफगानिस्तान में कारमाल को सत्ता से हटाया और अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद नजीबुल्लाह. तारीख थी 30 सितंबर, 1987.
दोनों ही देशों में सत्ता बदल चुकी थी और अब बारी थी शांति बहाली की कोशिश की. इस लड़ाई में पांच लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे और 60 लाख से ज्यादा लोग अपने घर बार छोड़कर पाकिस्तान और ईरान जा चुके थे. लिहाजा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मामले में दखल दिया. अमेरिका ने कहा कि अगर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान से अपनी फौज हटा लेगा, तो अमेरिका पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान के मुजाहिदिनों की मदद नहीं करेगा. दोनों देशों ने इस बात पर राजी होने के लिए करीब तीन साल का वक्त लिया. फाइनली 14 अप्रैल 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय जेनेवा में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिका और रूस के भी प्रतिनिधि मौजूद थे. रूस ने अपनी सेना को वापस बुलाने की शुरुआत कर दी, तो अमेरिका ने भी मदद रोकने की बात कर दी. सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकलने में करीब एक साल का वक्त लगा.
लेकिन अफगानिस्तान में शांति नहीं हुई. अफगानिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह ने खुद को और अपनी सरकार को कम्युनिजम से ज्यादा इस्लाम के करीब दिखाने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिदिनों और मोहम्मद नजीबुल्लाह सरकार के बीच संघर्ष चलता ही रहा. सोवियत सेनाएं फरवरी 1989 तक अफगानिस्तान के बाहर चली गईं और तब मार्च में मुजाहिदिनों के समूह ने अफगानिस्तान में हमले की कई कोशिशें की, जो नाकाम हो गईं.
इस बीच दिसंबर, 1991 में सोवियत संघ रूस के टुकड़े हो चुके थे. अब वो यूएसएसआर नहीं बल्कि सिर्फ रूस था. वो कमजोर पड़ चुका था. जब वो खुद की मदद नहीं कर सकता था, तो अफगानिस्तान की कहां से कर पाता. लिहाजा अफगानिस्तान में राष्ट्रपति मोहम्मद नजीबुल्लाह अलग-थलग पड़ गए. उन्हें रूस से मिलने वाली मदद भी बंद हो गई. अफगानिस्तान की सरकार और सेना को रूस की आदत पड़ी हुई थी. जब मदद बंद हो गई तो सेना और सरकार दोनों ही कमजोर पड़ गए. अफगानिस्तानी एयरफोर्स के पास तो फाइटर प्लेन में भरने के लिए तेल भी नहीं बचा. वहीं जेनेवा समझौते के बाद भी पाकिस्तान अफगानिस्तानी मुजाहिदिनों की मदद करता ही रहा. नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान के बड़े-बड़े शहर मुजाहिदिनों के कब्जे में आ गए. और फिर 18 मार्च, 1992 को नजीबुल्लाह ने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी. अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख मेंअंतरिम सरकार के गठन की बात शुरू हो गई. नजीबुल्लाह संयुक्त राष्ट्र संघ की सात लोगों की काउंसिल को अफगानी सत्ता सौंपने के लिए राजी हो गए. अभी ये होता, उससे पहले ही मुजाहिदिनों ने काबुल पर कब्जा कर लिया और नजीबुल्लाह को इस्तीफा देना पड़ा. वो संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बेस में जाकर छिप गए. अब पूरे अफगानिस्तान पर मुजाहिदिनों का कब्जा था.
लेकिन ये मुजाहिदीन भी कई गुटों में बंटे हुए थे. हेज्ब-ए-इस्लामी (गुलबुदीन), हेज्ब-ए-इस्लामी (खालिस), जमीयत-ए-इस्लामी, इस्लामिक दवाह ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान, नेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर अफगानिस्तान, नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इस्लामिक रिवोल्यूशन मूवमेंट ये सात संगठन मुख्य रूप से काम कर रहे थे. अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इन सातों मुजाहिदीन ग्रुप्स के लीडर पाकिस्तान के पेशावर में इकट्ठा हुए ताकि आगे की रणनीति बनाई जा सके और सरकार का गठन करके इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनाया जा सके. लेकिन गुलबुदीन हेकमतयार की हेज्ब-ए-इस्लामी ने इसका विरोध कर दिया और काबुल पर चढ़ाई कर दी. नतीजा ये हुआ कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से लड़ाई के हालात बन गए, जिसमें आमने-सामने थे मुजाहिदीन गुट, जो अफगानिस्तान से कम्युनिस्ट सरकार को उखाड़ने के लिए एक साथ आ गए थे.
मई, 1992 में जब गुलबुदीन हेकमतयार की हेज्ब-ए-इस्लामी ने काबुल पर हमला किया, तो उसे पाकिस्तान का समर्थन मिल गया. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खुले तौर पर गुलबुदीन हेकमतयार की हेज्ब-ए-इस्लामी के साथ आ गई. ये हमला इतनी जल्दबाजी में हुआ था कि नए नए इस्लामिक स्टेट बने अफगानिस्तान को संभलने का मौका ही नहीं मिला. गुलबुदीन हेकमतयार के खिलाफ मोर्चा संभाला जमीयत-ए-इस्लामी और जुंबिश-ए-मिली ने. और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल लड़ाई का अखाड़ा बन गई. हर तरफ से गोली-बारी, हर तरफ से बमबाजी, हर तरफ लाशों के ढेर. ये तस्वीर बन गई थी काबुल की. किसी चरमपंथी गुट की मदद पाकिस्तान कर रहा था तो किसी की मदद ईरान और किसी की सऊदी अरब. और सब एक दूसरे से लड़ रहे थे. इन सात बड़े गुटों के अलावा एक और भी गुट था, जो अफगानिस्तान में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था. इस गुट का नाम था तालिब.
उसने सोवियत के खिलाफ लड़ाई में अपनी एक आंख गंवा चुके मुल्ला मोहम्मद ओमर को अपना नेता चुन लिया, जो सोवियत संघ से खत्म हुई लड़ाई के बाद एक छोटी सी मस्जिद का इमाम बन गया था. लेकिन तालिब मुजाहिदिन के ग्रुप ने उसे अपना नेता बना दिया. और फिर एक नए संगठन ने अफगानिस्तान में जन्म लिया, जिसका नाम था तालिबान. अफगानिस्तान के कांधार के रहने वाले मुल्ला मोहम्मद ओमर ने 50 हथियारबंद लड़कों के साथ मिलकर तालिबान बनाया. उसका मानना था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के दखल के बाद यहां का इस्लाम खतरे में था और मुजाहिदिनों के अलग-अलग ग्रुप्स मिलकर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन स्थापित करने में फेल हो गए थे. उसकी ये सोच अफगानिस्तान में आग की तरह फैल गई. इस बीच गठन के कुछ ही दिनों के बाद उसने स्पिन बुलदाक पर अपना कब्जा जमा लिया. स्पिन बुलदाक वो जगह थी, जहां पर सोवियत यूनियन के सिपाहियों ने गुफाओं में अपने हथियार छिपा रखे थे. अब सोवियत यूनियन के छिपाए हुए वो हथियार तालिबान के कब्जे में आ गए थे.
एक महीने के अंदर ही करीब 15,000 लड़ाके तालिबान के साथ जुड़ गए. वहीं मुल्ला ओमर में पाकिस्तान को अपना फायदा नज़र आने लगा. उसने मुल्ला ओमर के तालिबान को मदद करनी शुरू कर दी. हथियार से और पैसे से, ताकि जब मुल्ला ओमर अफगानिस्तान पर कब्जा कर ले तो पाकिस्तान उसका फायदा उठा सके. इसके लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई काम पर लग गई. इन सबकी मदद 3 नवंबर, 1994 को तालिबान ने कांधार शहर पर हमला किया. दो महीने के अंदर ही तालिबान ने अफगानिस्तान के 12 राज्यों में अपना कब्जा जमा लिया. इस दौरान जो मुजाहिदीन आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे पर हमला करते रहते थे, उन्होंने भी तालिबान के आगे सरेंडर कर दिया. 1995 की शुरुआत में ही अपनी सफलता से उत्साहित तालिबान ने काबुल पर बमबारी शुरू की. लेकिन तब इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान के सैनिक मुखिया रहे अहमद शाह मसूद की सेनाओं ने तालिबान को मात दे दी और काबुल से खदेड़ दिया. करीब डेढ़ साल की तैयारी के बाद तालिबान ने फिर से हमला किया. शुरुआत हुई 26 सितंबर, 1996 से. और एक दिन के बाद ही 27 सितंबर, 1996 को काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया. और इसके साथ ही अफगानिस्तान के और भी बुरे दिन शुरू हो गए.
तालिबान ने करीब पांच साल तक अफगानिस्तान पर अपना कब्जा जमाए रखा. वो अफगानिस्तान में शरिया लागू करने की कोशिश करता रहा. इस दौरान अफगानिस्तान की हालत बेहद खराब हो गई. न पीने के लिए साफ पानी था और न ही सड़कें. न बिजली, न अस्पताल और न ही स्कूल. आम लोगों पर सख्त कानून थोप दिए गए. हत्या और रेप के लिए सार्वजनिक तौर पर फांसी दी जाने लगी. चोरी करने पर अंग-भंग किया जाने लगा. पुरुषों के लिए दाढ़ी रखना ज़रूरी हो गया. महिलाओं को बिना बुर्के के बाहर निकलना प्रतिबंधित कर दिया गया. टीवी, म्यूजिक और सिनेमा पर भी रोक लग गई. 10 साल या उससे ज्यादा उम्र की लड़कियों की पढ़ाई पर भी रोक लग गई.
करीब 20 साल से देश के अंदर ही लड़ाई झेल रहे आम अफगानियों के लिए कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था. इस बीच साल 2001 में 11 सितंबर को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अलकायदा ने हमला कर दिया और उस इमारत को ज़मींदोज कर दिया. ये वारदात की थी ओसामा बिन लादेन ने. उसी ओसामा बिन लादेन ने, जो जब 1979-80 में अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सेना के खिलाफ लड़ रहा था तो अमेरिका उसकी मदद कर रहा था. अब उसी लादेन ने अमेरिका पर आतंकी हमला किया तो अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश का खून खौल उठा. 20 सितंबर को जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ऐलान किया कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन गलत है और तालिबान को अलकायदा के सभी नेताओं को अमेरिका को सौंपना होगा.
तालिबान को अमेरिका की बात नहीं ही माननी थी. और वो नहीं माना. उल्टे तालिबान के पाकिस्तान में एंबेसडर अब्दुल सलीम जलीफ ने कह दिया कि लादेन तो इस हमले में शामिल ही नहीं है. नतीजा ये हुआ कि अमेरिका ने 7 अक्टूबर, 2001 को अफगानिस्तान पर बमबारी शुरू कर दी. इसमें अमेरिका को ब्रिटेन, कनाडा और दूसरे देशों का भी साथ मिल गया. अमेरिका की एजेंसी सीआईए की स्पेशल एक्टिविटिज डिविजन अफगानिस्तान में दाखिल हो गई. और फिर शुरू हुई टार्गेट किलिंग. अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने तालिबान के नेताओं को चुन-चुनकर निशाना बनाना शुरू किया. इस पूरे ऑपरेशन को नाम दिया गया ऑपरेशन एंडरिंग फ्रीडम. ऑपरेशन करीब 13 साल तक चलता रहा. आखिरकार 28 दिसंबर, 2014 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने ऐलान किया कि ऑपरेशन एंडरिंग फ्रीडम अब पूरा हो गया है. इस ऑपरेशन के दौरान अब तक करीब एक लाख 75 हजार लोगों की मौत हुई है.
साल 2018 से अमेरिका ने तालिबान के साथ बातचीत की कोशिश की. कोशिश इस बात की कि अब सब पहले ती तरह हो जाए. हिंसा रुक जाए. लेकिन बात पटरी पर नहीं आ सकी. फिर मार्च 2020 में आखिरकार अमेरिका और तालिबान के बीच समझौता हुआ. इसमें कहा गया कि नाटो सैनिक 14 महीने के अंदर-अंदर अफगानिस्तान से बाहर निकल जाएंगे. और फिर नाटो सैनिकों के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो गई. इस बीच अमेरिका में सत्ता बदल गई और जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए. उन्होंने ऐलान किया कि 11 सितंबर, 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सैनिक अपने वतन लौट जाएंगे.
और यहीं से तालिबान ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया. नाटो सैनिकों के दबाव में जो संगठन थोड़ा कमजोर होता दिख रहा था, वो नाटो सैनिकों के अफगानिस्तान से बाहर निकलने के साथ ही बेहद मज़बूती के साथ सिर उठाने लगा है. उसे काबुल और उसके आस-पास के इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया है और अब वो दावा कर रहा है कि अगले कुछ ही दिनों में वो पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेगा. और अगर ऐसा होता है तो ये और किसी के लिए चाहे छोटा झटका हो या बड़ा, लेकिन अमेरिका के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा, क्योंकि उसने लगातार 20 वर्ष तक तालिबान से लोहा लिया है और इसके बावजूद वो तालिबान का खात्मा नहीं कर सका है.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)
 “ महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने की थी कुरुक्षेत्र अष्टकोसी परिक्रमा,अब फिर एक बार जगाने के प्रयास
“ महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने की थी कुरुक्षेत्र अष्टकोसी परिक्रमा,अब फिर एक बार जगाने के प्रयास

ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस