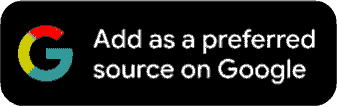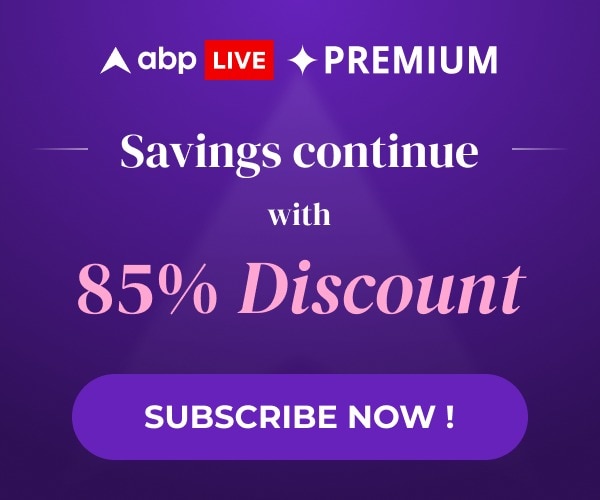BLOG: विपक्ष में है हिम्मत तो करे ऐलान कि सत्ता में लौटे तो सुधारेंगे संविधान!
महाराष्ट्र में भी जनादेश तो कांग्रेस-एनसीपी को विपक्ष में बैठने का मिला है. इन्हें सत्ता पाने से पहले जनता से आदेश क्यों नहीं लेना चाहिए? यदि एक ‘पाप’ है और दूसरा ‘पुण्य’ कैसे हो गया?

नई दिल्लीः महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, जैसे-जैसे हुआ, किसने-किसने और कैसे-कैसे संविधान की भावना में निहित लक्ष्मण रेखा का लांघा? वो सबसे सामने है. लोग ख़ुद ही तय कर रहे हैं कि कौन- कितना कसूरवार है, कितने राजनीतिक शुचिता की लाज़ नहीं रखी? लिहाज़ा, इसकी तह में जाने का कोई तुक़ नहीं है. अलबत्ता, ये वक़्त इस बात की पड़ताल है कि संविधान के प्रावधानों में ऐसी कौन-कौन सी कमज़ोर कड़ियां हैं जिसे पुख़्ता करने का बेहद ज़रूरत है. मसलन, तीन चीज़ों की ख़ामियों को दुरस्त करना ज़रूरी है. हालाँकि, सत्ता में बैठे लोग इन्हें शायद ही दुरुस्त करना चाहें क्योंकि उन्हें ही तो इसका नाजायज़ फ़ायदा मिलता है. लिहाज़ा, यदि विपक्ष में हिम्मत है तो वो ऐलान करे कि जब भी वो सत्ता में आएगी तो इन्हें दुरुस्त करके दिखाएगी.
बदलते वक़्त ने संविधान की उस दसवीं अनुसूची में अनेक सुराग़ कर दिये हैं, जिसका ताल्लुक दलबदल से है. लेकिन इससे पहले निर्वाचन से सम्बन्धित जन प्रतिनिधित्व क़ानून को भी दुरुस्त करना होगा. सबसे पहले तो ये तय करना ज़रूरी है कि किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने के बाद कम से कम कब तक दलबदल प्रतिबन्धित रहेगा? इसे साल-दो साल की सीमा में तो बांधा ही जाना चाहिए. ये भी तय होना चाहिए कि चुनाव पूर्व गठबन्धन और चुनाव बाद गठबन्धन के लिए क्या-क्या उपयुक्त है और क्या-क्या वर्जित रहेगा? क्योंकि, जनता ने यदि बीजेपी-शिवसेना के चुनाव पूर्व गठबन्धन को जनादेश दिया तो जनता की इजाज़त के बग़ैर शिवसेना अपने गठबन्धन से छिटक कैसे सकती है? क्या उसने छिटकने से ही अपने मतदाताओं से अनुमति प्राप्त की?
भारत में जनता किसी पार्टी को नहीं बल्कि उसके उम्मीदवार को वोट देती है. चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार से अपेक्षित है कि वो अपने और अपनी पार्टी के घोषणापत्र को लागू करके दिखाए. महाराष्ट्र के सन्दर्भ में शिवसेना की ये जबाबदेही क्यों नहीं होनी चाहिए कि क्या उसके गठबन्धन ने चुनाव से पहले ऐलान किया था कि वो 50-50 फ़ॉर्मूले से चलेगी? यदि ये बात बाक़ायदा लिखा-पढ़ी में नहीं थी, तो क्या इस दावे का कोई प्रमाण है? बग़ैर सबूत के जनता ये कैसे तय करे कि किसने वादाख़िलाफ़ी की? महाराष्ट्र से पहले बिहार में भी इसी तरह चुनाव पूर्व गठबन्धन के उसूलों के पीठ में छुरा भोंका गया. साझा जनादेश मिला आरजेडी-कांग्रेस और नीतीश कुमार को, लेकिन सत्ता की मलाई
खाने के लिए नीतीश उस बीजेपी से जा मिले, जिसे जनता ने विपक्ष में बैठाया था. यदि महाराष्ट्र में जनादेश से विश्वासघात हुआ तो क्या बिहार में नहीं हुआ? महाराष्ट्र में भी जनादेश तो कांग्रेस-एनसीपी को विपक्ष में बैठने का मिला है. इन्हें सत्ता पाने से पहले जनता से आदेश क्यों नहीं लेना चाहिए? यदि एक ‘पाप’ है और दूसरा ‘पुण्य’ कैसे हो गया? क्या संविधान को इस गुत्थी को हमेशा-हमेशा के लिए सुलझाना नहीं चाहिए? ये भी हमेशा-हमेशा के लिए तय होना ज़रूरी है कि राज्यपाल का विवेकाधिकार आख़िर क्या है? यदि ये अराजनीतिक पद है तो फिर इसे राजनीति का हिस्सा बनने की छूट क्यों हासिल है? राज्यपाल किसकी ताजपोशी करेंगे, कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, कितने वक़्त में ‘फ़्लोर टेस्ट’ होना चाहिए? इन सवालों से जुड़ी मनमानी को भी हमेशा-हमेशा के लिए ख़त्म करने किया जाना चाहिए या नहीं? क्या ये संविधान-सम्मत है कि राज्यों में वही होगा जो दिल्ली चाहेगी? यदि नहीं, तो संविधान में अपेक्षित सुधार क्यों नहीं होना चाहिए? राज्य और केन्द्र सम्बन्ध से जुड़े सरकारिया आयोग की सिफ़ारिशों की धज़्ज़ियाँ कब तक उड़ती रहेगी? कब तक बात-बात पर सुप्रीम कोर्ट का बेशक़ीमती वक़्त बर्बाद किया जाता रहेगा? यदि रोज़मर्रा की बातें भी सुप्रीम कोर्ट को ही तय करनी हैं तो राज्यपाल और उससे जुड़े अनुच्छेद 164 की ज़रूरत क्यों है?
जो ग़लतियां कांग्रेस अपने लम्बे शासनकाल में करती रही है, वही बीजेपी यदि सत्ता में आकर कर रही है, तो जनता किसे सही माने? महाराष्ट्र ने इतना तो साफ़ किया ही विपक्ष की राजनीति करने वाले किसी भी महारथी ने बिहार, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, अरूणाचल, मेघालय और जम्मू-कश्मीर से अनुभवों और इतिहास से कुछ नहीं सीखा. दूसरी ओर, बीजेपी को अनुच्छेद 164 और 356 के इतिहास के सारे सबक याद हैं, कंठस्थ हैं. बदलते दौर के साथ बीजेपी ने उन सारे सिद्धान्तों में महारथ हासिल कर ली जो कभी कांग्रेस का कॉपीराइट हुआ करती थी.
बीजेपी ने सत्ता में पहुँचने से पहले भारत की मिट्टी से जो कुछ सीखा, उसे ही तो अब ताल ठोंककर और डंके की चोट पर आज़मा रही है. इसीलिए सियासी कुश्तियों में वही बार-बार विजेता बनती है. वो बात अलग है कि कर्नाटक में उसे येदियुरप्पा को दूसरी बार में सत्ता तक पहुँचाने में सफलता मिली. महाराष्ट्र में भी फड़नवीस के साथ ऐसा ही होगा या नहीं, ये तो वक़्त बताएगा. बेशक़, महाराष्ट्र ने बीजेपी और शिवसेना को साझा जनादेश दिया था. लेकिन ये भी सच है कि जनादेश से धोखाधड़ी सिर्फ़ शिवसेना ने ही नहीं की, बल्कि अजीत पवार ने भी तो वही किया. धोखा पकड़ा गया, इसीलिए तो उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा. कौन जाने, कल को माफ़ी माँगकर एनसीपी में भी वापसी कर लें! क्या महाराष्ट्र की जनता ने इन्हें मनमर्ज़ी करने का जनादेश दिया है?
आज सत्ता में बैठी बीजेपी को ये कतई नहीं सोहाएगा कि वो संविधान के लचरपन को दुरुस्त करने के लिए आगे आए. ये काम या तो विपक्षी पार्टियों को ही करना होगा. या, कभी सुप्रीम कोर्ट से ‘बोम्मई-2’ या ‘केशवानन्द भारती-2’ जैसे कोई फ़ैसला आएगा, तभी हालात बदलेंगे. जब ऐसा होगा, तब होगा. इसके होने तक राजनीति की काली-अँधेरी रात ऐसे ही जारी रहेगी. दूसरी ओर, संविधान को चुनाव बाद बनने वाले गठबन्धनों के लिए नियम-क़ायदे तय करने होंगे. जोड़-तोड़ से सरकारें बनेंगी तो ख़रीद-फ़रोख़्त का होना लाज़िमी है. सभी पार्टियाँ ऐसा करने के लिए अभिशप्त हैं. क्या सभी पार्टियों को ऐसे श्राप से मुक्त करने का इन्तज़ाम संविधान को नहीं करना चाहिए?
मौजूदा संवैधानिक प्रावधानों के तहत कोई राज्यपाल साधु नहीं होता. अनुच्छेद 164 और 356 के रहते हो भी नहीं सकता. कांग्रेसी राज्यपाल भी कभी साधु नहीं रहे तो संघी राज्यपाल भला क्यों होने लगे? क्या सिर्फ़ इसलिए कि भगवा ख़ानदान ने कभी चाल-चरित्र-चेहरे की बात की थी? राजनीति तो चीज़ ही बातें बनाने की है. कौन बातें नहीं बनाता? कौन तानाशाही नहीं करता? क्या कांग्रेस ने तानाशाही में कभी कोई कोर-कसर छोड़ी थी. अरे, कांग्रेस तो अर्टिकल 164 और आर्टिकल 356 की बदौलत अपनी पार्टी और अपने मुख्यमंत्री तक की सरकार को भी उखाड़ फेंका है!
कोश्यारी ने वही किया जो ‘ऊपर’ से हुक़्म मिला. हमेशा यही होता रहा है. अब आप देते रहिए दुहाई कि राज्यपाल ने क्या सही किया और क्या ग़लत? देते रहिए मिसाल कि केन्द्र में कब-कब और किन-किन सरकारों ने कैसे-कैसे अनुच्छेद 164 और 356 के ज़रिये लोकतंत्र का चीरहरण किया? बताते रहिए कि कौन ज़्यादा नंगा है और कौन कम? जाइए सुप्रीम कोर्ट और कीजिए संसद का चक्का जाम! किसी का कुछ नहीं बनने-बिगड़ने वाला. किसी की भी सरकार गिरे लेकिन सौदेबाज़ी का सिलसिला नहीं थमने वाला. अभी एनसीपी ने जलजला देखा, कल को शिवसेना और कांग्रेस में भी टूट-फूट हो जाए तो ताज़्ज़ुब मत कीजिएगा. राजनीति अब गाँधी के उसूलों पर नहीं, बल्कि रुपये पर छपी उनकी तस्वीर के पीछे चलती है. याद रखिए, बीजेपी आज ‘तानाशाही’ के जिन सिद्धान्तों पर चल रही है, उसकी पाठशाला का शिलान्यास जवाहर लाल नेहरू ने ही नम्बूदरीपाद की सरकार को गिराकर किया था. वही पाठशाला 70 सालों में देखते ही देखते विश्वविद्यालय में बदल चुकी है. केन्द्र की हरेक सरकार इस विश्वविद्यालय की निरंकुश कुलपति रह चुकी है. अभी तो बीजेपी का कार्यकाल है. उस पर दोष क्यों? कोई अपवाद नहीं है. लिहाज़ा, विधवा-विलाप से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला.
दरअसल, संविधान के निर्माताओं और उसकी व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट की अनुच्छेद 164 और 356 को लेकर चाहे जो धारणा रही हो, लेकिन ये अकाट्य सच है कि इन्हीं दोनों अनुच्छेदों और दसवीं अनुसूची की बदौलत होने वाला सियासी नंगा नाच अब भारतीय राजनीति और संविधान के सबसे बड़े कलंक का दर्ज़ा हासिल कर चुका है. बेशक़, संविधान एक नायाब दस्तावेज़ है. लेकिन अनुच्छेद 164 और 356 तथा दसवीं अनुसूची, इसके ऐसे ‘ब्लैक-होल’ की तरह हैं जो 70 सालों के सफ़र में और स्याह ही होते चले गये. अनुच्छेद 164 की बदौलत ही राज्यपाल किसी को भी मुख्यमंत्री बना देते हैं या कभी भी जल्लाद बनकर किसी भी सरकार का गला दबा देते हैं. उनसे ये काम केन्द्र सरकार अनुच्छेद 356 के तहत करवाती है. इसी तरह, दलबदल को रोकने वाले दसवीं अनुसूची के प्रावधान ही उसके लिए रास्ते बनाते हैं.
भारतीय राजनीति में अनुच्छेद 164 और 356 के बेज़ा इस्तेमाल की बुनियाद भले ही नेहरू युग में कांग्रेसियों ने रखी. लेकिन कालान्तर में दिल्ली में सत्तासीन हुई हरेक सशक्त या लूली-लंगड़ी राजनीतिक शक्ति ने भी अपने सियासी स्वार्थ के लिए इसका अपार दोहन किया. अनुच्छेद 164 और 356 ने ही राजनीति में सुचिता और विचारधारा जैसी सभी बातों को क़िताबी और काल्पनिक बना दिया. संविधान के यही दोनों अनुच्छेद समाज में ‘जिसकी लाठी उसकी भैंस’ वाली उपमा के संवाहक हैं. व्यवहार में इससे ज़्यादा दबंगई, अतार्किकता और मनमानीपूर्ण आचरण और कुछ नहीं है. किसी ज़माने में जिन तर्कों के साथ किसी की बहू-बेटी को घर से उठा लिया जाता था, उसी तरह से संविधान के लागू होने के बाद किसी निर्वाचित सरकार को या तो चुटकियों में ज़मींदोज़ कर दिया जाता है या फिर सारे विधि-विधान को ताक़ पर रखकर किसी की भी ताजपोशी कर दी जाती है.
राज्यपाल को केन्द्र में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर नाचना पड़ता है. वहाँ से मिली उधार की साँसों पर ही जीना पड़ता है. उसे राजभवन की शान-ओ-शौक़त का लुत्फ़ उठाते हुए दिल्ली की ओर मुँह करके बस एक ही मंत्र-जाप करना होता है कि ‘जो तुमको हो पसन्द वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे!’ इस मंत्र को ही राज्यपाल का निजी संविधान या ‘इन्दीवर कोड’ भी कह सकते हैं. 1970 की ‘फ़िल्म सफ़र’ में इसी ‘इन्दीवर कोड’ का शानदार फ़िल्मांकन हुआ. राजनीतिक संगीत की दृष्टि से देखें तो ‘राज्यपाल’ सबसे ढीठ या बेशर्म राग है.
इसके गायन, वादन और नृत्य जैसी विधाएँ किसी व्याकरण या मर्यादा से नहीं बँधी हैं. इसे किसी भी प्रहर में गाया जा सकता है. ये आरोह-अवरोह, ताल, ख़्याल जैसी शास्त्रीय वर्जनाओं से भी सर्वथा उन्मुक्त है. यहाँ तक कि अराजकता का कोई भी दायरा इसकी पैमाइश नहीं कर सकता.
कहने को राज्यपाल अपने राज्य का संवैधानिक मुखिया है, लेकिन उसकी औकात केन्द्र सरकार के चपरासी या अर्दली से ज़्यादा नहीं होती. इसीलिए उसे केन्द्र की कठपुतली, एजेंट या दलाल भी कहते हैं. केन्द्र की सत्ता में रहने वाली हरेक पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तो राज्यपाल में नीति और मर्यादा के तत्व ढूँढ़ती फ़िरती है. लेकिन अपने चुनावी घोषणापत्र या संकल्प-पत्र में कभी ये नहीं कहती कि जब वो सत्ता में लौटेगी तो अनुच्छेद 164 और 356 को कलंक-मुक्त करने का इन्तज़ाम करेगी. ये पुलिस-सुधार जैसा ही राजरोग है. इसका कोई पुख़्ता इलाज़ नहीं करना चाहता.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)