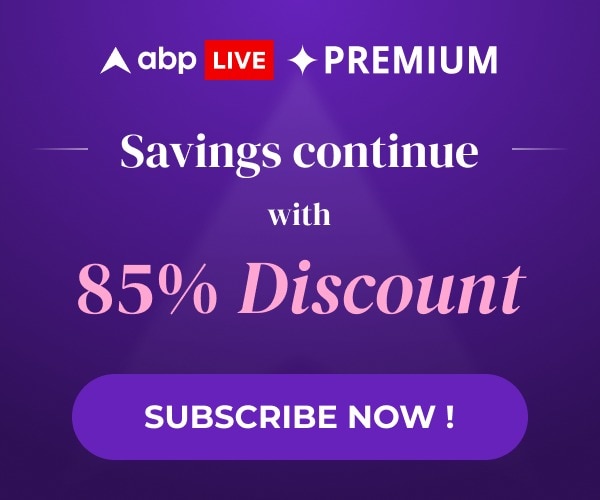तीन राज्यों के चुनाव में स्थापित पार्टियों की गारंटी के सामने निर्दलीय प्रत्याशियों की बढ़ती चुनौती खिलाएगी गुल

हिंदी पट्टी में पड़ने वाले तीनों चुनावी राज्यों के बीच छत्तीसगढ़ में मतदान का पहला चरण बीस सीटों पर मंगलवार को संपन्न हो गया. ये बीस सीटें ज्यादातर आदिवासी बहुल क्षेत्र में हैं जहां आम तौर से माना जाता है कि संसदीय चुनावों के प्रति एक तो वहां का मतदाता कम जागरूक और उदासीन होता है, दूसरे नक्सल प्रभावित होने के चलते मतदान के बहिष्कार का आह्वान यहां मतदान को प्रभावित करता है. इन दोनों धारणाओं को इन सीटों पर उतरे प्रत्याशियों की संख्या और मतदान के प्रतिशत ने इस बार चुनौती दे डाली है.
छत्तीसगढ़ का रंग इस बार अलहदा
राजनीतिक दलों के दांव को छोड़ दें, तो आश्चर्यजनक रूप से पहले चरण की बीस सीटों पर कुल 72 निर्दलीय उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमायी है. यानी, औसतन चार निर्दलीय प्रत्याशी हर सीट पर लड़ रहे हैं. कुछ हॉट सीटों की बात करें, तो अकेले राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के खिलाफ 28 प्रत्याशी खड़े थे जिनमें 18 निर्दलीय थे. खुज्जी सीट पर लड़ रहे कुल 10 उम्मीदवारों में से चार निर्दलीय हैं जबकि डोंगरगांव में एक दर्जन प्रत्याशियों में आधा दर्जन निर्दलीय हैं. इन संख्याओं की अहमियत समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से लेकर 2018 तक हुए तीन चुनावों में कुल 995 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार 430 निर्दलीय मैदान में हैं. आगामी 17 तारीख को होने वाले दूसरे चरण में 70 सीटों पर 358 निर्दलीय उतर रहे हैं. यह प्रति सीट औसत पांच निर्दलीय पड़ता है. इसके अलावा अगर उन दलों के 311 और प्रत्याशियों को जोड़ लें जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं है, तो बिना दल वाले प्रत्याशियों की संख्या 741 हो जाती है.
मध्य प्रदेश और राजस्थान भी उसी राह
निर्दलीयों के मामले में देखें, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यही स्थिति है. मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों के लिए कुल 4287 नामांकन सामने आए थे. निर्वाचन आयोग ने 523 नामांकन खारिज कर दिए. अब 3728 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं. दिलचस्प यह है कि मात्र 230 सीटों के लिए अकेले भारतीय जनता पार्टी से 3000 से ज्यादा दावेदार सामने आए थे. इसका सीधा कारण था पार्टी में टिकट बंटवारे के कारण हुई बगावत. कांग्रेस में यह आंकड़ा और भी अधिक है. पार्टी में 4000 से ज्यादा दावेदारों ने टिकट के लिए आवेदन किए थे. आखिरी वक्त में टिकट कटने की आशंका में अधिकृत प्रत्याशियों के अलावा कई दूसरे दावेदारों ने भी भाजपा और कांग्रेस से नामांकन भर दिए थे. इसी तरह राजस्थान में 6 नवंबर तक 2605 प्रत्याशियों ने 3436 नामांकन पत्र दाखिल किए थे. अगर सीटवार देखें, तो राजस्थान में भाजपा और कांग्रेस को मिलाकर कम से कम 30 सीटों पर बड़े चेहरों ने नामांकन भरा था. नामांकन वापस लेने की तिथि 8 नवंबर को पूरी होने के बाद अंतिम नतीजों को देखने से समझ आता है कि दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व द्वारा मान-मनौव्वल के बावजूद स्थिति बहुत नहीं बदली है. हालत यह थी कि भाजपा से खुद अमित शाह को जाकर राजस्थान के पूर्व मंत्री राजपाल सिंह शेखावत को नामांकन वापसी के लिए मनाना पड़ा, तो मध्य प्रदेश के मांधाता विधानसभा सीट में कैलाश विजयवर्गीय को जाकर भाजपा के तीन बागियों के परचे वापस करवाने पड़े.
इसके बावजूद राजस्थान में सांचौर, चित्तौड़गढ़, शिव, सूरतगढ़, डीडवाना, बयाना, लाडपुरा, खंडेला, झुंझनू, पिलानी, फतेहपुर, कोटपुतली, बस्सी, शाहपुरा, और अनूपगढ़ में भाजपा का आधिकारिक प्रत्याशी उसके बागी से कड़ी चुनौती से झेल रहा है. ऐसे ही राजस्थान की सरदारशहर, मसूदा, हिंडौन सिटी, मनोहर थाना, बड़ी सादड़ी, नागौर, अजमेर दक्षिण, पुष्कर, नगर, शाहपुरा, सूरसागर, सिवाना, राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ की सीटों पर कांग्रेस के आधिकारिक प्रत्याशी के सामने उसके बागी का कड़ा दांव लगा हुआ है.
निर्दलीयों की संख्या देती है ये संकेत
इस मायने में मौजूदा विधानसभा चुनावों को अब तक हुए चुनावों से गुणात्मक तौर पर अलग कहा जा सकता है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में निर्दलीय और बागी प्रत्याशियों की इतनी ज्यादा संख्या कम से कम दो बातों का संकेत देती है. पहली, कि अब पार्टी के साथ वफादारी या अपनी पीठ के पीछे पार्टी की संगठनात्मक ताकत बहुत मायने नहीं रखती है. इसका एक प्रमुख कारण यह है कि चुनाव लड़ने के तरीके और तकनीकें अब बहुत निजी और आभासी यानी वर्चुअल हो चले हैं. पार्टी अगर अपने स्थापित नेता को टिकट नहीं देगी, तो नेता के पास खुद इतने संसाधन हैं कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ के जीत ले. जहां तक मतदाता का सवाल है, अगर उसकी वफादारी अपने नेता के प्रति कायम है तो यह नेता के लिए सोने पर सुहागा का काम करती है. राजस्थान के डीडवाना से लोकप्रिय पूर्व मंत्री यूनुस खान, सिवाना से सुनील परिहार (अशोक गहलोत के करीबी जिन्होंने सिवाना में कांग्रेस को अकेले खड़ा किया था) और राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ से मौजूदा विधायक जौहरीलाल मीणा का अबकी निर्दलीय खड़ा होना इसकी तसदीक करता है. निर्दलीयों की बढ़ती संख्या से दूसरी अहम बात साठ और नब्बे के शुरुआती दशकों के अनुभव से निकल रही है, जब देश के समक्ष बेरोजगारी और मोहभंग की जबरदस्त स्थितियां थीं. आज कालचक्र घूम कर वहीं पर पहुंच चुका है, लेकिन गुणात्मक रूप से स्थिति भिन्न है क्योंकि गांवों तक पैसा पहुंच चुका है. गांव-कस्बों में जमीन के बड़े पैमाने पर हुए अधिग्रहण और बाजार की पहुंच ने चुनावी राजनीति को एक व्यवसाय की शक्ल दे दी है. इसीलिए हर बड़ा-छोटा नेता या समाजसेवी या बेरोजगार कार्यकर्ता चुनाव लड़ने की सोच रहा है. उस पर से देश में पार्टीगत ध्रुवीकरण के चलते चुनावी राजनीति आम लोगों के लिए कानूनी ढाल बनकर भी उभरी है. इसीलिए हम देखते हैं कि 2010 के बाद से बीते दसेक साल में जितने किस्म के सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने राज्यों और आम चुनाव में शिरकत की, ऐसा पहले नहीं था.
हर कोई चाहता है लड़ना चुनाव
इस ट्रेंड की शुरुआत भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से हुई थी. फिर विश्वविद्यालय परिसरों और सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलनों से राजनीतिक दलों में सीधी भर्ती हुई. आज मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि शिक्षामित्र से लेकर अनुदेशकों तक और असंतुष्ट स्वास्थ्यकर्मी से लेकर हर किस्म के सरकारी कर्मचारियों तक चुनाव लड़ने का संक्रमण फैल चुका है. यह बीच के कुछ वर्षों में पार्टी-केंद्रित हो चुकी राजनीति के विकेंद्रीकरण का संकेत है जो 2024 के आम चुनाव में अपने शबाब पर जा सकता है. केंद्र और प्रातों में एक पार्टी के लंबे और सशक्त शासन के बाद पहले भी ऐसी स्थितियां आई हैं जब कुछ समय के लिए चुनावों में निर्दलीयों की भूमिका अहम रही है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपनी पार्टी और राज्य को नेता एक दूसरे का पर्याय मानने लग जाते हैं. मध्य प्रदेश के सागर में इस हफ्ते कांग्रेस के नेता जीवन लाल पटेल का वह भाषण इसका सुबूत है जिसमें वे सरकारी पंचायतकर्मियों को धमकी दे रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो उनके बच्चों को भूखा मार देगी. यही दंभ तब आधिकारिक शक्ल ले लेता है जब राज्य के सार्वजनिक संसाधन को पार्टियां अपने इमदाद के तौर पर बांटने लग जाती हैं. अशोक गहलोत जिन सात गारंटियों को लेकर यात्रा पर निकले हुए हैं, वे गारंटियां राजस्थान विधानसभा द्वारा बाकायदा कानून बनाकर दी गई हैं. यह कांग्रेस का सकारात्मक पक्ष है कि उसने लाभ पहुंचाने के लिए कानून बनाए, ताकि सत्ता परिवर्तन के बाद भी ये लाभ जारी रह सकें. इसका नाकरात्मक पक्ष यह है कि राज्य के बनाए कानून से मिलने वाले लाभ को पार्टी का इमदाद बताकर प्रचारित किया जा रहा है जहां मतदाता को ‘लाभार्थी’ और मुख्यमंत्री को राजा जैसा दिखाया जा रहा है. बिलकुल यही काम उत्तर प्रदेश और केंद्र के स्तर पर भाजपा करती रही है.
पार्टियों से हो रहा जनता का मोहभंग
इसीलिए पार्टियों से लोगों का मोहभंग होता जाता है जबकि राजनीति खरीद-फरोख्त और नापाक गठबंधनों के दौर में पहुंच जाती है. इस मामले में राजस्थान अग्रणी रहा है जहां एक समय में 35 निर्दलीय विधानसभा में चुनकर पहुंचे थे. बहुत संभव है कि इस बार भी राजस्थान में निर्दलीय ही सरकार की किस्मत का फैसला करें. मध्य प्रदेश में भी चुनाव बाद स्थिति देखने लायक होगी जहां बड़े नेताओं, सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है. इन विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपने स्थापित और कामयाब नेताओं के टिकट काटकर भले ही किसी नए किस्म के प्रयोग का दंभ भर रहे हों, लेकिन बागियों को मनाने की उनकी बेचैनी और छटपटाहट अब सबके सामने है. दूसरी ओर मतदाताओं के समक्ष गारंटियों का लॉलीपॉप लेकर घूम रहे उनके आला नेता इस तथ्य की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे हैं कि बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं के मामले में पांच साल तक उनका अनकिया ही उन्हें अब गारंटी देने को मजबूर कर रहा है- वही गारंटी, जो नब्बे के दशक से पहले राज्य की कल्याणकारी भूमिका का अनिवार्य संवैधानिक अंग हुआ करती थी. अब वही काम पार्टियों को करना पड़ रहा है क्योंकि दोनों दलों ने जाने कब का कल्याणकारी राज्य को तिलांजलि दे दी है.
अगर अर्थव्यवस्था खोले जाने के बाद राज्य की कल्याणकारी भूमिका को बचाए रखा गया होता, तो दोनों प्रमुख पार्टियों को आज इमदाद के सहारे चुनाव लड़ने की न नौबत आती, न ही हजारों प्रत्याशियों को अपने दम पर चुनाव लड़कर इन्हें आईना दिखाने की जरूरत पड़ती. अब चूंकि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर वापसी असंभव है, तो स्थापित राजनीतिक दलों को उसकी कीमत किसी न किसी रूप में चुकानी ही होगी. हो सकता है हजारों निर्दलीय और अपंजीकृत दलों के प्रत्याशियों में से दर्जन भर ही जीतकर सदन में पहुंचें, लेकिन आने वाले दिनों में सौदेबाजी की चाबी निर्दलीयों के हाथ में ही रहेगी. स्वाभाविक है यह परिघटना राजनीति को और जटिल बनाएगी.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ़ लेखक ही ज़िम्मेदार हैं.]
 “ Health Day Special: मोबाइल फोन और बच्चों की आंखों की सेहत, बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या और उपाय
“ Health Day Special: मोबाइल फोन और बच्चों की आंखों की सेहत, बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या और उपाय

ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस