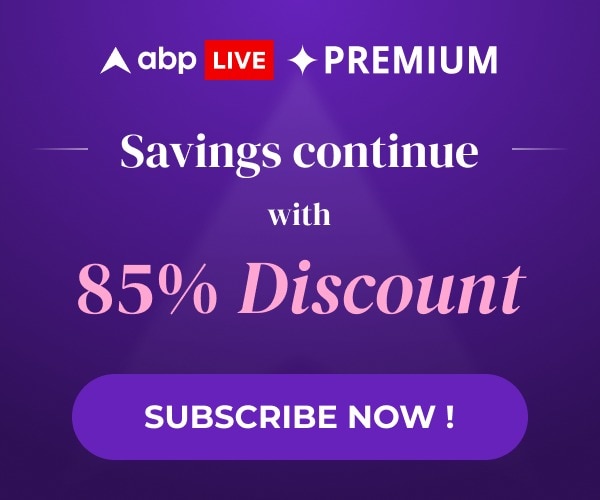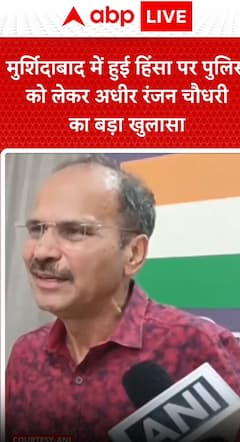एक लंबे समय बाद अपने बारे में सोच रही है जनता, चुनाव है बस एक संयोग की तरह आया

आम चुनाव के लिए मतदान के तीन चरण गुजरने के बाद सत्ता और विपक्ष दोनों को केवल एक सवाल खाये जा रहा है कि इस बार मतदान इतना कम क्यों हो रहा है? पहले और दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े जारी करने में डेढ़ हफ्ते का समय लगाकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने धारणा के स्तर पर राजनीतिक दलों को थोड़ा राहत देने की कोशिश बेशक की है कि मतदान पिछली बार के मुकाबले बहुत नहीं, मामूली ही कम है. यह बात अलग है कि नगालैंड के चार जिलों से पहले चरण में शुरू हुआ चुनाव बहिष्कार अब गुजरात और महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है. यह स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाली बात होनी चाहिए कि गुजरात के 25 लोकसभा क्षेत्रों में दर्ज 4.79 करोड़ योग्य मतदाताओं में से 1.90 करोड़ ने वोट क्यों नहीं डाला?
मतदान की प्रेरणा
इस सवाल को थोड़ा उलट कर देखते हैं और अपनी समझदारी बनाने के लिए एक सवाल रखते हैं- लोकतांत्रिक चुनावों में मतदान करने के लिए मतदाता को आखिर कौन सी चीज प्रेरित करती है? सवाल पर आने से पहले एकबारगी यह भूल जाएं कि मतदान करना राष्ट्रीय कर्तव्य है, जैसा कि चुनाव आयोग से लेकर प्रधान न्यायाधीश और सरसंघचालक तक हर कोई पहले चरण के बाद से जोर देकर कह रहा है. दूसरी बात, यह याद रखें कि मतदान इस देश में अब तक अनिवार्य नहीं किया गया है, स्वैच्छिक ही है. अगर स्वतंत्रेच्छा वाकई कोई चीज है, तो मतदान प्रतिशत यह बताता है कि औसतन 40 प्रतिशत मतदाताओं की मतदान करने की कोई इच्छा नहीं है. चौतरफा सवाल इसी 40 प्रतिशत पर है. सबकी जिज्ञासा भी यही है कि ये वोटर कौन हैं और इनकी अनिच्छा से नुकसान या फायदा किसको हो रहा है. हम इस जिज्ञासा को पलट कर रखेंगे और पूछेंगे कि जो 60 प्रतिशत मतदाता मतदान कर रहे हैं, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं. उन्हें कौन सी चीज मतदान केंद्रों तक ले जा रही है? यह चुनाव क्या किसी मुद्दे पर खड़ा है जो लोगों को वोट डालने को उत्प्रेरित कर सके? अब तक तो किसी भी दल का उठाया मुद्दा स्थायी रूप से काम करता नहीं दिख रहा!
कोई ऐसा राजनीतिक या सामाजिक नैरेटिव भी नहीं बना है जो देश भर में चुनावों को एक सूत्र में बांध सके. इस बार तो 2014 की तरह मोदी जैसे चमत्कारिक शख्स को दिल्ली का ताज पहनाने का सवाल भी नहीं है. या फिर 2019 वाला बालाकोट-जनित उत्साह भी नहीं है जब पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल इलीट कमरों से निकल कर जनता का मुद्दा बन गया था.
चुनाव में मुद्दा और विपक्ष
चुनाव को मुद्दे पर खड़ा करना वास्तव में सत्ता के विपक्ष का काम होता है. विपक्ष इसमें बुरी तरह नाकाम रहा है जबकि सत्ता इस बार विपक्ष के उठाए मुद्दों पर फील्डिंग करती दिख रही है और उसके अपने सकारात्मक मुद्दे चर्चा से गायब हैं- सिवाय उत्तर प्रदेश के, जहां सुधरी हुई कानून व्यवस्था का श्रेय विभिन्न तबकों के लोग मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को देते हैं जो प्रकारांतर से भाजपा के हक में जाता है. तो एक अदद मतदाता क्या सोचकर भीषण गर्मी में बूथ तक वोट डालने जा रहा है? महज नागरिकता-बोध या लोकतांत्रिक कर्तव्यनिष्ठा क्या इसके पीछे हो सकती है? यदि ऐसा होता, तो हमारे दैनंदिन सामाजिक जीवन में भी नागरिकता-बोध कम से कम साठ प्रतिशत झलकता. बीते कुछ वर्षों की बड़ी घटनाओं को एक बार पलटकर देखें, तो हम पाएंगे कि सरकार के लागू किए फैसलों के प्रति अपने-अपने अनुभवों पर ठहरकर सोचने या उनका सुख-दुख मनाने की मोहलत लोगों को कायदे से नहीं मिली. मसलन, पहले 2016 में नोटबंदी कर दी गई. बिल्कुल औचक और अप्रत्याशित. इसी के बाद 2017 में आधी रात इस देश में माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू किया गया. छोटे-बड़े व्यापारियों, दुकानदारों आदि को इससे अभ्यस्त होने में काफी वक्त लगा. जब तक मामला पटरी पर आता, पिछला लोकसभा चुनाव निपट गया. चुनाव के बाद जीवन सहजता की ओर बढ़ रहा था, कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलनों ने दैनिक जीवन को प्रभावित किया. दिल्ली जैसे महानगर में लोग दफ्तर से घर आने के लिए सुगम रास्ते खोजने में ही उलझे रह गए. आंदोलन का पटाक्षेप हुआ तो स्वास्थ्य इमरजेंसी लगा दी गई, यानी लॉकडाउन.
राजनीतिक प्रक्रिया से जन का अलगाव
लॉकडाउन ने अतिगरीब तबकों का तो जो किया सो किया, संतुष्ट मध्यवर्ग को सामाजिक-राजनीतिक प्रक्रियाओं से अलगाव में डाल दिया, जो अब भी इस देश का 40 प्रतिशत तो बनता ही है. दार्शनिक जॉर्जियो आगम्बेन के शब्दों में कहें, तो कोरोना के चलते दुनिया भर की सरकारों द्वारा की गई समाज की तालाबंदी (सोशल डिस्टेंसिंग) ने हमें ‘छूछी देह’ में तब्दील कर डाला, जिसका काम खाने, सोने और मनोरंजन करने तक सीमित रह गया. यह तकरीबन दो साल का जैविक-राजनैतिक (बायोपॉलिटिकल) अनुकूलन था, जिसके आज हम उत्पाद हैं. आगम्बेन पूछते हैं, ‘’जिसके पास अपना वजूद कायम रखने के अलावा कोई मूल्य ही न बचा हो, वह समाज कैसा होगा?” समाज चूंकि वजूद की मुंडेर पर आ खड़ा हुआ था, तो कुछ लोग उस मुंडेर से कूद भी रहे थे. 2021 के बाद राष्ट्रीय अपराध आंकड़ा ब्यूरो (एनसीआरबी) के आत्महत्याओं के आंकड़ों को देखिए- व्यापारी और नौजवान आधुनिक इतिहास में पहली बार किसानों को खुदकशी में पीछे छोड़ चुका है. ये वे लोग थे जिनके पास किसानों की तरह अपने खा लेने भर को उगाने की जमीन तक नहीं थी. ये आत्महत्याएं अब भी जारी हैं. नोएडा में तंगी से जूझ रहे एक मीडियाकर्मी ने कल ही जहर खाकर जान दी है. बीते चार साल में खुदकशी का पैटर्न बदला है- अब लोग अकेले नहीं, परिवारों के साथ जान दे रहे हैं.
जीवन बचाना और छूछी देह बन जाना
जो मुंडेर की इस ओर बच गए, उनका क्या? इस बीच बड़े पैमाने पर निम्नवर्ग और मध्यवर्ग सामाजिक सरोकारों से कट के घर-परिवार, गृहस्थी और खर्चा-पानी जुटाने तक सिमट गया. बाकी सरकार खुद कहती है, कि अस्सी करोड़ लोगों को वह प्रत्येक पांच किलो राशन देकर कूदने से बचाए हुए है. प्रो. अरुण कुमार ने एक अध्ययन में इस आबादी की संख्या 60 करोड़ के आसपास रखी है. मान लेते हैं कि सरकारी राशन पर जी रहे ये लोग पचास करोड़ भी होंगे, तो तकरीबन 99 करोड़ की मतदाता आबादी का ये आधा बैठते हैं. एक के बाद एक विपदाओं से जूझते हुए बच गए ये लोग पिछले कुछ समय से ठहरकर अपने बारे में सोच रहे हैं. अपने अनुभवों को गुन रहे हैं. अपनी हालत पर विचार कर रहे हैं. बहुत लंबे समय बाद इन्हें यह मौका लगा है, बल्कि कहें एक के बाद एक मेगा-इवेंट करवाने वाली इस सरकार ने अनजाने में ही इन्हें इतनी मोहलत दे दी है कि वे अपने बारे में सोच सकें. मध्यवर्ग का एक हिस्सा जो 2021 के बाद कड़ी मेहनत कर के अब सम पर आया है, वह भी शायद सोच रहा है. सत्ताधारी दल के आम कार्यकर्ता भी सोचने लगे हैं. लोग सोच रहे हैं, तो उन्हें पुरानी बातें याद आ रही हैं. वे बेचैन हो जा रहे हैं.
वोट है या प्रतिकार
सीतापुर के जाजपुर गांव में एक अधेड़ पासी मजदूर से मैंने पूछा कि आप वोट क्यों देंगे. उसने कहा कि कोरोना में उसके रिश्तेदारों की मौत हो गई थी. अयोध्या में यही सवाल मैंने एक दुकानदार से पूछा. उसने कहा नोटबंदी के बाद से अब तक पैसा ही नहीं बचा. ऊपर से दुकान बिक रही है. रायबरेली में यही सवाल एक बुजुर्ग से पूछा. उसने कहा, दबंगों ने सरकार की शह पर उसकी जमीन कब्जा ली है, पेड़ काट दिए हैं. हमीरपुर में सत्ताधारी दल के एक पूर्व जिलाध्यक्ष से यही सवाल पूछने पर जवाब आया, ‘’यह आखिरी बार है, केवल इसलिए कि अपनी पार्टी है. इसके बाद बगावत होगी.‘’ क्यों? यह पूछने पर वे बोले, ‘’क्योंकि अपनी पार्टी के राज में सच बोलने और उसके लिए लड़ने की गुंजाइश पहले से भी कम हो गई है.‘’ एक शहरी ‘लाभार्थी’ से मैंने यही सवाल पूछा. उसने कहा, ‘’जिंदगी भर भिखमंगा बनाए रखना चाहती है सरकार.‘’
यानी मामला अब वजूद से आगे जा चुका है. अपने बारे में सोच रहे मुल्क की ये दो-चार बानगी हैं. ऐसे दर्जनों लोगों की गवाहियां मेरे पास दर्ज हैं. जरूरी नहीं कि सोचना हमेशा तात्कालिक कर्म में ही तब्दील हो जाए, लेकिन समाज बरसों बाद अपने बारे में सोच रहा है यही बड़ी बात है. इसी से तो उसे लगातार बीते कुछ वर्षों में दूर रखा गया था. प्रो. राजीव भार्गव लिखते हैं कि लोकतंत्र संवाद में रत एक राष्ट्र होता है. संवाद की पहली शर्त है विचार. विचार करने वाला मनुष्य ही खुद को अभिव्यक्त करता है. सामूहिक अभिव्यक्ति की स्थिति तो अभी दूर है. संवाद में भी समय लगेगा. अभी लोग सोच रहे हैं. और जब आदमी सोचता है, तो उसे अपने साथ हुआ गलत याद आता है और दूसरे के साथ हुए गलत के प्रति सहानुभूति उपजती है.
मतदाता तोल रहा है
संयोग कहें कि अपने कटु अनुभवों को याद करने और दूसरों के साथ हुए अन्याय को समझ पाने की यह मोहलत आम चुनाव की अवधि से टकरा गई है. इतिहास गवाह है कि यह समाज हमेशा कमजोर के साथ खड़ा रहा है. ऐसे में दूसरा संयोग यह है कि मजबूत सत्ता अपना नैरेटिव खड़ा नहीं कर पाई है. घर में बैठ कर सोच रहा एक आम भारतीय मतदाता इन्हीं दो संयोगों के बीच बाहर की धूप को तौल रहा है. इसका नतीजा चाहे जो निकले, लेकिन लंबे समय से अटका समय का पहिया अब घूमना शुरू कर चुका है.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही ज़िम्मेदार है.]
 “ Health Day Special: मोबाइल फोन और बच्चों की आंखों की सेहत, बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या और उपाय
“ Health Day Special: मोबाइल फोन और बच्चों की आंखों की सेहत, बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या और उपाय

ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस