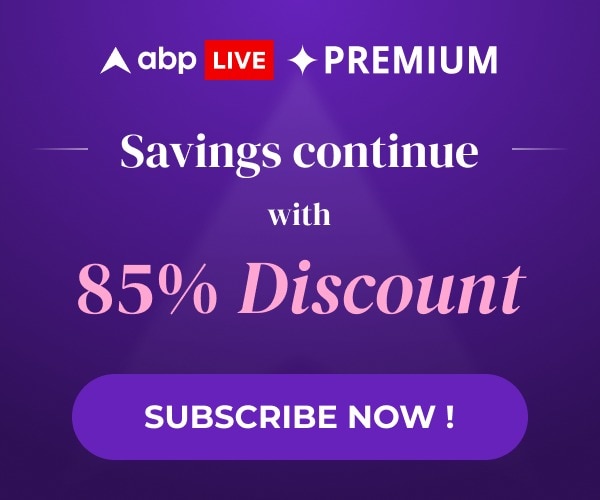वामपंथ के नए कैडर के लिए कहां ठौर ठिकाना

आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सीपीएम ने 22वीं कांग्रेस में पार्टीगत नीतियों को स्पष्ट करते हुए जिस तरह कांग्रेस के साथ किसी गठबंधन के बगैर तालमेल की संभावना को स्वीकार किया है, वह उसकी राजनीतिक परिपक्वता से ज्यादा मजबूरी है. बेशक पार्टी की केंद्रीय समिति ने कांग्रेस से अलग उसकी नजरों में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक माने जाने वाले दलों को एकजुट करने का प्रस्ताव दिया था. मौजूदा हालात में सीपीएम इस हालात में नहीं थी कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती और कुछ राजनीतिक संगठनों को लेकर एक नए धड़े के रूप में दिखती. जिसे सीपीएम की व्यवहारिक सोच कहा जा रहा है वह उसकी मौजूदा समय की मजबूरियां है कि उसे अपने आप भी कामय रखने के लिए भी ऐसे प्रस्ताव को थोड़ा नकार कर उसे लचीला स्वरूप देना पड़ा है. एक तरह से सीपीएम 22वीं कांग्रेस में दोनों पहलुओं के साथ दिखने की कोशिश हुई. जहां एक तरफ केंद्रिय समिति के प्रस्ताव के जरिए यह सोच सामने रखी गई कि भारतीय वामपंथ कांग्रेस से हटकर अपनी एक पहचान रखता है और किसी भी तरह उसका पिच्छलग्गू नहीं हैं, वहीं इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर लचीलापन लाने की कवायद के जरिए राजनीतिक नुकसान को भी आंका गया.
सीपीएम की केंद्रीय समिति जिस प्रस्ताव को लेकर आई उसमें बीजेपी सरकार के सामने विपक्षी एकता बिखर रही थी. कांग्रेस चाहे जिस स्थिति में भी हो लेकिन उनके बिना किसी और विपक्षी गठबंधन को सामने लाने से सरकार के खिलाफ चुनाव में उतरने का तानाबाना नहीं बुनता. खासकर तब जबकि इस मुहिम में सीपीएम को ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस पर भी सोचना होता. और यह भी आकलन करना होता कि विपक्षी एकता की कवायद में वैचारिक नारों के अलावा सीपीएम कितना योगदान दे सकती है. जाहिर है सीपीएम के लिए केंद्रीय समिति का प्रस्ताव का आना और उसे अस्वीकार करने से सीपीएम ने इतना प्रचारिक जरूर कर पाया कि कांग्रेस के साथ चुनावी अभियान चलाया जाए या नहीं इस पर चर्चा की जाए. यानी कांग्रेस से एक दूरी भी जताई गई और तालमेल की संभावना भी खुली रखी गई.
इसमें विचित्र व्याख्या यह भी है कि अपनी सहूलियत और बीजेपी के हिंदुत्व को थामने भले ही अब बीजेपी और आरएसएस को फासीवाद शब्द पर अलग कर देखें, लेकिन बीजेपी आरएसएस जो हैं जैसे हैं अभी फिलहाल अगले कुछ दशकों तक उन्हें अलग करके नहीं देखा जा सकता. किसकी समझ में आएगी सीपीएम की यह नई व्यख्या. चाहे मुद्दा कश्मीर का हो या फिर सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता की अपनी सहूलियत वाली व्याख्याओं का. आखिर जाना तो आपको मतदाताओं के पास है. बार बार की ठेस उपहास देव देवताओ पर व्यंग, हल्के परिहास, भारतीय सेना पर रह रहकर तंज की स्थिति में भारतीय लोगों से मत की अपेक्षा भी किस तरह की जा सकती है. जेएनयू की हलचल देश के युवाओं को कैडर के रूप में नहीं बना पाई इसकी यही वजहें हैं. कांग्रेस ने समय रहते इसे समझ लिया है. खासकर गुजरात के चुनाव के बाद से कांग्रेस एक अलग स्वरूप में है. जो मतदाताओं के एक बड़े वर्ग को चिढा नहीं रहा है.
सीपीएम के ही नहीं बल्कि वामपंथ के बचे आधार को छिनने से बचाने के लिए ऐसी मुहिम के सिवा अब कोई विकल्प नहीं था. भले ही विपक्षी एकता का नाम दिया जाए और सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना कहा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि सपा-बसपा जैसे दलों की तुलना में वामपंथ पार्टियां उस स्थिति में है जहां उसके अस्तित्व पर ही सवाल लग रहे हैं. खासकर त्रिपुरा में वामपंथ का गढ़ ढहने के बाद वामपंथ नारों विचारों सोशल मीडिया, प्रगतिशील साहित्य, कुछ सहयोगी संगठनों जेएनयू की हलचलों में तो अपनी हलचल दिखा रहा है लेकिन राजनीतिक धरातल में उसकी जमीन लगातार छिनती गई है. केरल में भी अब एकाधिकार जैसी स्थिति नहीं रही. पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़ हो गया है. ऐसे में किसी सीपीआई या सीपीएम जैसे वामपंथी संगठन की पहली कोशिश यही है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बदले और उस बदलाव में किसी तरह सीपीएम सीपीआई फारवर्ड ब्लाक तमाम वामपंथ की धाराएं उत्साह का संचार महसूस करे. कहीं सूखती पखुंडियां हिलने लगे. कांग्रेस या किसी भी गठबंधन के सहयोगी के नेतृत्व में आई सत्ता वामपंथी दलों के लिए हवा के झोंके की तरह होगी जिससे वह फिर अपने को तलाश सकती हैं.
लेकिन क्या यह सब इतना सहज और आसान है. सीपीएम या सीपीआई ने अपने जनाधार को केवल निरंतर राजनीतिक पराजयों से नहीं खोया. बीजेपी का धीरे धीरे पूरे देश में बढता आधार भी वामपंथ के हाशिए का कारण नहीं बना. सीपीएम ने पंश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता खोई. बेशक त्रिपुरा में बीजेपी के स्थानीय प्रभावी संगठनों के साथ मेलजोल या गठबंधन करने का नतीजा हो पर यहां भी सीपीएम का ढाई दशक पुराना किला ठह गया. केरल मे अपने अस्तित्व को बचाते हुए वामपथियों की चिंता अब यूडीएफ के ज्यादा बीजेपी संघ की गतिविधियों से होगी. पहली बार बीजेपी ने वहां विधानसभा में प्रवेश किया है. वामपंथ के खासकर सीपीएम के सीमित होते जाने की वजह बीजेपी के विस्तार से ज्यादा दूसरे और कारणों से हैं. उसमें सबसे असल कारण नए कैडर का विस्तार न कर पाना है. वामपंथ ने जेएनयू की गतिविधियों से सुर्खियां तो ली, कुछ मुद्दों पर सक्रिय होना फिर लो हो जाना वह पार्टी के लिए धरातल पर कैडर नहीं जोड़ पाया. वापंपंथ के संगठन अपने अंदर उच्च प्रभावी केंद्रिय समिति हाईकमान के प्रभाव को लेकर तो चिंतित रहा लेकिन ग्रास रूट पर पार्टी के विस्तार के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ. वामपंथी संगठनो के जो देश भर में जगह जगह इलाके थे जहां उनका प्रभाव था वो कब कमजोर होकर ढह गए पता भी नहीं चला. भारतीय वामपंथ पिछले खासकर दो दशक से दो स्तरं पर अपने को चर्चा में रखता आया. या तो पार्टी के अंदर उच्च स्तर पर चर्चा रही या फिर वामपंथ प्रगतिशील कही जाने वाली कोई धारा है वह कुछ छात्र संगठनों या दूसरे संगठनों के आयोजनों में रही. खासकर जेएनयू की हलचलों को प्रयाप्त कर्म मान लिया गया. टीवी की डिबेट या सोशल मीडिया पर जवाबी हुकांरे भरते लोग तो दिखे पर इन सबसे पार्टी का आधार नहीं बढा. इसके लिए जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए था.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जिन बातों को अपना सबल मानती है उसे छोडना नहीं चाहिए था. धीरे धीरे मजदूर श्रम के नारे भी लोग भूलने लगे. कम्युनिस्ट पार्टी को भी मजा आने लगा कि कोई कन्हैया है जो अपनी तरह से सुर्खियों में है. कम्युनिस्ट पार्टी ने इसी में राहत की सांस ली कि गुजरात में कोई हार्दिक पटेल है जो बीजेपी को तंग करने की स्थिति में दिख रहा है. यह सब कम्युनिस्टों को आंतरिक सुख दे सकता है लेकिन इससे भारतीय वामपंथ का उभार होता या उसे देश भर में स्वीकारने की स्थिति बनती यह संभव नहीं था. भारतीय वामपंथ देश के जनमानस में बैठी उस अवधारणा को नहीं तोड़ पाया कि कहीं न कहीं उसके नेता या पार्टी संगठन कुछ आग्रहों के साथ अपनी रणनीतियां बनाते हैं. भारतीय वामपंथ इस देश के जनमानस में अपनी भूमिका को बहुत स्पष्टता से सामने नहीं रख पाया. कहीं न कहीं उनके बढते कदमों के साथ सवाल भी उठते रहे. भारतीय जीवन में वामपंथ जिस तरह अपन आग्रहों के साथ दिखा, या फिर नीतिगत व्यवहार में फसंता हुआ दिखा उसने युवाओं के एक छोटे से वर्ग को छोड़कर नया कैडर नहीं बनने दिया. जिन पहलुओं में भारतीय भावुक होते हैं वहां वामपंथ तर्क के बजाय उपहास और मन को कचौटती शैली के साथ प्रस्तुत हुआ उससे उसे नया आधार कहां मिलता. केवल जेएनयू जैसी संस्था या एक खास सोच वाली बौद्धिक विरादरी का साथ वामपंथ को सुर्खिया ही दे सकता था. हालात यही हैं कि तीन राज्यों को छोडकर वामपंथ को चुनाव मं पोलिंग बूथ पर कार्यकर्ता नहीं मिलते. हालात यह है कि किसी समय कांग्रेस सपा राजद आदि के लिए प्रचार करती कम्युनिस्टों की टोलियां भी अब नजर नहीं आती. उप्र या बिहार में बडे दलो से दो या तीन सीटों की गुजारिश करने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ने दक्षिणपंथी केंद्र या राज्य सरकार की चूल हिलाने के लिए रणनीतियां तो खूब बनाई लेकिन अपने विस्तार या भविष्य के लिए रणनीतियां नहीं बनाई. उनकी आतिशबाजी इसी बात पर होती रही कि कभी सपा-बीजेपी को हरा देती है तो कभी लालू चुनौती देते हैं.
भारत की वामपथी शक्तियां आज तक समझ नहीं पाईं कि वास्तव में उन्हें कांग्रेस जैसे अखिल भारतीय संगठन से किस कोण पर रहना है. कांग्रेस को वामपंथ का साथ किसी न किसी तरह मिलता ही रहा और उसका फायदा भी मिला. लेकिन वापमंथ संघटनों की अपनी तैयारी इतनी ही थी कि जैसे ही कांग्रेस देश भर में कमजोर हुई वामपंथ हाशिए से भी परे चला गया. यहां तक कि बीजेपी ही नहीं कांग्रेस से क्षेत्रीय आधार पर लड़ने वाली शक्तियों सपा, राजद, बसपा आदि ने भी कम्युनिस्ट दलों को बैठकों में तो बुलाया लेकिन उनका रसूख नहीं बढाया. नए महासचिव बने सीताराम येचुरी फिर घूमकर उसी बिंदु पर आए हैं कि कांग्रेस की पीठ पर थपकी देकर किसी तरह केद्र और राज्यों में बीजेपी को कमजोर किया जाए उससे सत्ता ली जाए. लेकिन वामपंथी पार्टियां का जतन इस तरफ नहीं है कि कैसे एक विचारधारा की दो बड़ी पाटिर्यों के अस्तित्व को संवारा जाए. हालत यह है कि सीपीएम, सीपीआई एम का तो जिक्र हो भी जाता है, सीपीआई एमएल फारवर्ड ब्लाक एसयूसीआई (सी) को राजनीति के मानचित्र पर खोजना पड़ता है. दिक्कत यही है कि वामपंथी पार्टियों न लोगों का भरोसा जीतने के बजाया या एक नियोजित संकल्पों पर चलने वाली पार्टी के बजाय इन्हें केवल तरह तरह के विविदों को जन्म देने या बहस तूल देने वाली एक पार्टी के तौर पर ही माना. बदलते समय में भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टियों को अपने आप में भी काफी बदलना चाहिए था. इसलिए बीजेपी या संघ पर उसके प्रहार उतने स्वभाविक नहीं लगे जितना कांग्रेस के या लालू यादव की पार्टी के.
भारतीय क्म्युनिस्ट पार्टियों ने बेशक अपने को प्रगतिशील कहा लेकिन अपनी राजनीतिक ऊर्जा के लिए उसने केवल तमाशों और विपक्षियों को छिछालेदर करने की प्रवृतियों पर ही विश्वास किया. इससे वह संजीदगी से अपना आकार नहीं गढ पाई. अनेकों बार अलग अलग प्रसंगों में उसका विचलन भी दिखा. कांग्रेस से अपने संबंधों को लेकर कोई स्पष्ट व्याख्या उसके पास नहीं रही. उसके लिए समझाना मुश्किल हुआ कि जिस वामपंथ के लोग कांग्रेस को भर भर कर कोसते हैं उसी दल से कोई समझौते का गलियारा कैसे निकल सकता है. और अगर ऐसा संभव है तो वह वापमंथ के समझौते हैं उस खाचें से जनमानस को कैसे संतुष्ट करेंगे. कैसे एक प्लेटफार्म बनेगा जिसमें वह ममता बनर्जी के साथ खडे दिखेंगे. वामपंथ पार्टियां आज तक आर्थिक या नीतिगत पहलुओं पर लोगों को समझा नहीं पाई कि कैसे वह किसी राजद से हाथ बढा सकती है और कैसे उसकी आर्थिंक चिंतन कांग्रेस के अनुरूप है या विपरीत.
सबसे असल बात यही है कि कांग्रेस या दूसरी सभावित सहयोगी पार्टियों के लिए वामपंथी पाटियों का साथ जुडना भले इन पार्टियों को फायदा न दे लेकिन वामपंथी ऐसी किसी मुहीम से अपने लिए तिनके का सहारा ढूंढ रहे हैं. देखा गया कि जिस अपनी साहित्य धारा, थियेटर, सेमीनार आदि से वामपंथी पार्टियों को संजीवनी मिलती थी वह समय अब बदल गया. वोट लेने और देने की शैलियां बदल गई. सेमीनार साहित्य संगोष्ठियां अब शायद राजनीतिक प्रचार का बडा माध्यम नहीं रह गई है. सीपीएम की 22वीं कांग्रेस का यह प्रस्ताव भले ही उनकी अपनी सोच में व्यवहारिक हो लेकिन जब तक वह अपने कैडर का विस्तार नहीं करते तब तक ये दल छिटके हुए ही रहेंगे.
बेशक सत्ता के बदलाव हो लेकिन वामपंथी ताकत उभरती नहीं दिखेगी. क्योंकि भले ही वामपंथ धारा मानती हो कि उसकी प्रतिद्वदिता बीजेपी या संघ से हैं लेकिन उसकी अस्तित्व की लड़ाई सपा, बसपा कांग्रेस और राजद से भी उतनी ही प्रबल रूप से है. वामपंथियों को सबसे खुद की जड़ता से बाहर आना होगा. दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों का हाल यही है कि सर्वोच्च स्तर पर कुछ नेताओं के नाम सुर्खियों में रहते हैं लेकिन नीचे के कैडर में कोई नाम कहीं नहीं सुनाई देता. टीवी की डिबेट में वामपंथी पार्टियों के प्रवक्ता अपनी पाटियों के बजाय कांग्रेस राजद या सपा के प्रवक्ता की तरह बोलते दिखते हैं. वमपंथी पार्टियों के आग्रह सोच स्पष्टता के ऱखने की कवायद नहीं आती. मुद्दों पर भाकपा या माकपा की बंधी बधाई शैली युवाओं को जोड नहीं पा रही. अकेले जेएऩयू के भरोसे वामपंथ कब तक सांस लेगा. काश वामपंथ की 22 कांग्रेस में कहीं इस मंथन पर भी होती. कितना सन्नाटा है कि कार्ल मार्कस की दूसरी जन्मशति यू हीं निकलती गई. जब दुनिया से माक्सर्वादी किले ढहते गए हैं तब भारत में वह कहीं टिका हुआ दिखता रहे इसके लिए बड़े जोड़ जतन की जरूरत है. बहुत कुछ खंगालने और छिपे आवरण को बदलने की जरूरत है.
(नोट- उपरोक्त दिए गए विचार व आंकड़े लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.)
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस