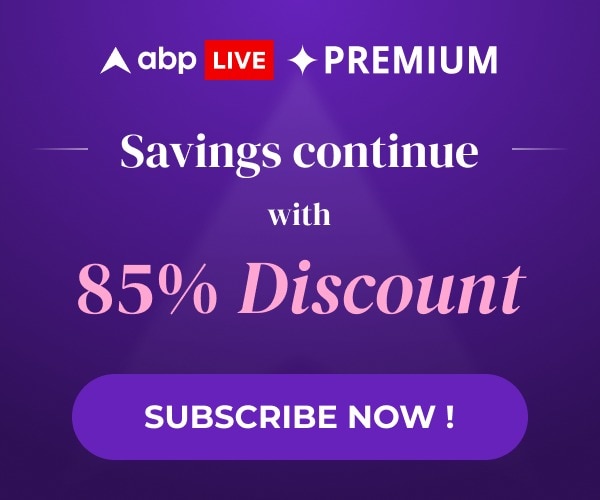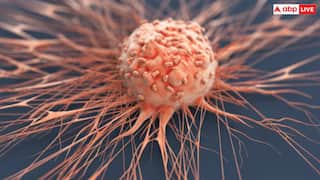यमुना से लेकर शहरों-कस्बों के छठ घाट तक की दुर्दशा, मरती सामूहिक चेतना का प्रतीक

अभी पिछले हफ्ते दीपावली का त्योहार संपन्न हुआ है और अब समूचा पूर्वी भारत छठी माई की पूजा के लिए तैयार है. बरसात के बाद से ही पर्वों का सिलसिला शुरू होकर अगले दो महीने तक लोकपर्व को समर्पित रहता है, जिसमें पितृपक्ष, नवरात्रि, दुर्गा पूजा, शरद पूर्णिमा, पांच दिवसीय दीपोत्सव, छठ पूजा शामिल हैं, जिसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के स्नान के साथ होता है. ध्यान से देखें तो ये सारे त्योहार प्रकृति के तमाम मूर्त-अमूर्त अव्ययों के प्रति हमारी कृतज्ञता की लोक अभिव्यक्ति है.
लोकपूजा का यह पर्व प्रकृति को समर्पित
पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को प्रकृति प्रदत्त स्वरूप के रूप में पिंड अर्पित करते हैं, तो नवरात्रि में प्रकृति के सृजन क्षमता के अनेक स्वरूप जिसमें पर्वत, वन्य जीवन, पेड़-पौधों, नादियां आदि शामिल हैं, उसमें देवी के मूर्त स्वरूप को समझते हैं. वही पांच दिवसीय दीपोत्सव हमारे कृषि और श्रम अर्जित समृद्धि का उत्सव है, यहां तक कि राम के वनगमन को सम्पूर्ण भारत और सुदूर लंका तक कृषि विस्तार से भी जोड़ के देखते हैं. और छठी माई की पूजा तो प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का चरम ही है, जलवायु, मौसम और देश काल के अनुसार अन्न, फल-फूल को जीवन यिनी जल से ऊर्जा के अमिट स्रोत 'सुरूज देव' को अर्पित करते हैं. लोकोत्सव के मौसम का समापन नदी, तालाब, झील में पवित्र स्नान के साथ अपनी फसल की कटाई के लिए निमित्त होते हैं. ये सभी लोकपूजा के उपादानों में पानी के प्रति आभार एक ज़रूरी अव्यय है. चाहे वो शैलपुत्री की पूजा हो या यम द्वितीया के दिन कच्छप सवार यमुना नदी स्नान के साथ उनका आह्वान हो, पानी में खड़े हो कर अस्तचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पण हो या कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी, तालाब और झील का वंदन हो. ये हमारी जल संस्कृति की सभ्यतागत सशक्त अभिव्यक्ति है जो लोकप्रवृत्ति और लोकाचार में आज भी दृष्टिगोचर होती रहती है.
वहीं, दूसरी तरफ आज सवाल है कि पानी के प्रति सदियों से देवता समान आस्था रखने वाला समाज, क्या आज भी पानी, नदी, तालाब, झीलों के प्रति संवेदनशील है? क्यों पानी के प्रति हमारा समाज इतना सतही हो चला है? क्यों हम श्रद्धा के नाम नदी,पोखर, तालाब को पूजा की सामग्री से गंदा कर उसी गंदी नदी की पूजा का स्वांग रचते हैं? धीरे-धीरे प्रकृति के प्रति सामाजिक श्रद्धा अब पाखंड में बदलती जा रही है और हम उसी पाखंड का सार्वजनिक निरूपण करने को अभिशप्त हैं. दीपावली और छठ के उल्लास में नदी, पानी और पोखर के प्रति हमारे सामाजिक व्यवहार के नज़र से एक त्वरित अवलोकन की ज़रूरत है.
जीवन के लिए जरूरी नदी-विमर्श
पांच दिवसीय दीपोत्सव में हम ना सिर्फ़ समृद्धि की देवी लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की पूजा करते है बल्कि मृत्यु के देवता यमराज और उनकी बहन यमुना की स्तुति करते है. इसी क्रम में यमुना के संदर्भ में नदी विमर्श भी आ जाता है. दीपोत्सव के पहले दिन धनतेरस, समृद्धि का उत्सव होता है, दूसरे दिन अकालमृत्य से बचाव के लिए मृत्यु के देवता यमराज के निमित दीप जलाने का दिन होता है. पूरब में इस प्रथा को 'जमदियरी' कहते हैं. फिर दीवाली के बाद "यमद्वितीया' के रोज यमराज और उनकी बहन यमुना के प्रगाढ़ संबंधों को भाई-बहन के त्योहार के रूप में मनाते हैं. विष्णुपुराण एवं मार्कण्डेय पुराण के अनुसार यम और यमी जुड़वां भाई-बहन हैं, और यमी ही कच्छप पर सवार यमुना नदी हैं. यमुना और यम दोनों भाई-बहनों में से कदर अगाध, प्रगाढ़ प्रेम माना जाता है कि बहन यमुना को भाई यमराज की तरफ़ से वरदान है कि जो भी भाई-बहन यमद्वितीया के दिन श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, निष्ठा, समर्पण भाव से यमुना में स्नान करेगा, यमुना की पूजा-पाठ-ध्यान करेगा, वो यमराज की यातना से मुक्त रहेगा. यानी कि दीपोत्सव के पांच दिनो में ही कम से कम दो बार यमराज की पूजा करते हैं, उनकी बहन देवी यमुना की अर्चना भी करते हैं. पर हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति खोखली और सतही दिखती प्रतीत होती है जब दिल्ली में यमुना के विस्तार और प्रवाह को देखते हैं. यमुना दिल्ली में मृत हो चुकी है जिसमें नदी का कोई गुण मेल नहीं खाता, तभी तो निरी (NEERI) ने बहुत पहले ही इसे प्राकृतिक रूप से मृत नदी घोषित कर दिया है.
यमुना का प्रवाह अस्तित्व के लिए लड़ रहा
मृत्यु के भय से हर साल दीपावली में यमराज और बहन यमुना की अर्चना तो करते है पर हम यमुना नदी की नरक यातना को हर बार भूल जाते हैं. वैसे तो यमुना नदी का पूरा प्रवाह तंत्र ही अस्तित्व की लड़ाई लड़ रह है, दिल्ली में ही यमुना हमारे तथाकथित विकास की बलि चढ़ चुकी है. आज स्थिति यह है कि यमुनोत्री से दिल्ली तक आते-आते यमुना में उसका एक भी पानी का बूंद नहीं बचता, सारा प्राकृतिक प्रवाह उससे चूस लिया जाता है, ताकि पंजाब, हरियाणा, सुदूर राजस्थान के खेत लहलहा उठें, भीमकाय दिल्ली और साथी शहरों की ना मिटने वाली प्यास बुझाई जा सके. और इंतिहा तब हो जाती जब सूख चुकी यमुना को दिल्ली वाले अपने मलमूत्र और फैक्ट्री के बजबजाते पानी से प्रवाहमान करके ही दम लेते हैं.यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकल एक हजार तीन सौ छिहत्तर किलोमीटर का सफर तय करते हुए इलाहाबाद में गंगा में विलीन हो जाती है. इस नदी की सबसे अधिक दुर्गति दिल्ली के वजीराबाद से लेकर ओखला बैराज तक होती है. नदी का यह बाईस किलोमीटर उसके सम्पूर्ण प्रवाह पर भारी पड़ता है.
यमुना की धार्मिक और सामाजिक सरोकार में आए क्षय की बात हो और यमराज के साथ कृष्ण और ब्रज भूमि की चर्चा न हो तो बात अधूरी ही रह जाती है. दिल्ली की मृत और स्याह पड़ चुकी यमुना ब्रज क्षेत्र में प्रवेश करती है. वैसे यमुना का पानी प्राकृतिक रूप नीला है जो श्यामल दिखता है. इसलिए भी इसे कालिंदी कहते हैं. पर अब ब्रज में कृष्ण की प्रेयसी यमुना काली है, प्रदूषित है, अपवित्र है. जहां मथुरा, वृंदावन, बरसाने सहित अनेक तीर्थ स्थल, महत्वपूर्ण स्थान, ताजमहल, तुलसीदास, सुरदास के जन्म एवं कर्मस्थल हैं. यमुना में कृष्ण का खेलना, उसके किनारे कुंजों में बंसी बजाना, कदम्ब के पेड़ पर चढ़ना, छुपना, स्नान करना, उसके आस-पास गाय चराना, मक्खन लूटना, ग्वाल बालों एवं गोपियों के साथ रास रचाना, नाचना, खेलना, लीलाएं करना आदि उनके जीवन की यमुना के साथ अद्भुत घटनाएं हैं.समूचे व्रज क्षेत्र में श्रीकृष्ण की पटरानी के रूप में उसी नालीरूपी यमुना का शृंगार और यह तक हम यमुना आरती भी करने को अभिशप्त हैं. आगरा तक आते-आते यमुना जो थोड़ी बहुत सांस लेने के काबिल बचती है, वहाँ औद्यौगिक दूषित जल से उसका गला रुंध जाता है, भला हो दक्षिण से मिलने वाली चंबल, केन, सिंध, बेतवा सरीखे नदियां जिसके जल से यमुना की धड़कन प्रयागराज में गंगा से मिलते समय तक चलती रह पाती है.
यमुना हमारी सामूहिक चेतना का मापक
नाले में बदल चुकी यमुना हमारी सामूहिक चेतना पर एक स्याह धब्बा है जो बताता है कि हम धार्मिक नहीं धर्मभीरू और आधुनिक नहीं आस्था मिश्रित अराजक हो गए हैं. हमारी आस्था अब कर्मकांड की ग़ुलाम हो चुकी है, और हमारी सामूहिक चेतना में क्षय आधुनिकता के साथ और तेज़ी से बढ़ी है. अब हम यमुना को दूषित कर उसी यमुना की पूजा भी करेंगे और याचना भी करेंगे कि यमुना हमें यमराज के कोप से बचा भी ले. वही ब्रज में कृष्ण भक्ति में लीन रहेंगे, इस बात को दरकिनार कर कि कृष्ण प्रिय यमुना हमारे ही मल-मूत्र से मृतप्राय है. आज नदी-पोखर, तालाब का सवाल हमारे अस्तित्व का सवाल बन चुका है, तो ज़रूरत है कि अपने नदी की, पानी को देवता मानने की आस्था को नए सिरे से टटोल कर विरोधाभास को समझा जाए ताकि हमारी परम्परागत जल संस्कृति को पुनर्जीवन मिले. भारत साधु संतो का देश है पर यमुना की स्थिति देख कर ये कहा जा सकता है कि पिछले कुछ दशकों में जनता के मानस को प्रभावित करने वाला संत समाज अपने कर्तव्य में बुरी तरह विफल रहा है. आज ज़रूरत है कि संत समाज, भक्तजनों को क्यों ना सिर्फ़ समझाए अपितु चेताये कि नदी को गंदा करना, नरक में जाने के बराबर है. शास्त्रार्थ करने वाले समाज उन धर्मग्रंथों की इबारतों को बदल नहीं सकता, जिनमें मूर्तियों से लेकर फूल, पूजा-हवन की सामग्री, और अस्थियों को नदी में प्रवाहित करने का विधान बनाया गया है? नदियों में शव बहा देने की परंपरा को आखिर कौन बदलेगा? आईटीओ पर यमुना नदी के पुल को लोहे की जालियों के घेरो को तोड़ कर पूजा के फूल और प्लास्टिक में लिपटे सारी सामग्री को यमुना में फ़ेक देने वाली प्रवृति पर रोक तो समाज को ही लगानी पड़ेगी.
सभी जलस्रोतों पर हो हमारी आस्था
हमारी आस्था का धर्मभीरू हो जाना केवल यमुना की दुर्दशा तक सीमित नहीं है, इसके शिकार हमारे सभी जल के स्रोत हो रहे हैं. दीपावली का यमुना नर्क अध्याय छठ पूजा तक पूर्वांचल से बंगाल तक अधिकांश पोखर, तालाब और नदी घाट तक पहुँच जाता है. अब हर शहर गाँव की अपनी यमुना है, कहीं नदी के रूप में तो कहीं तालाब के रूप में, जो धीरे-धीरे या तो विलुप्त हो रही है या नाला बन चुकी है. अनेक जगहों पर तो शहरी नदियाँ और तालाब तो सिर्फ अंग्रेजो के जमाने के गजेटियर में ही बचे रह गये हैं. उदाहरण के लिए सुदूर चंपारन के मोतिहारी शहर में नामचीन मोतीझील है जो शहरी अतिक्रमण, प्रशासनिक अकर्मान्यता और अराजक राजनीति के कारण सिकुड़ रही है, मर रही है.मोती जैसे चमकने वाले विशाल झील में ऐसी स्थिति नहीं रही की छठ पूजा निमित व्रती साफ़ पानी का आचमन कर अस्तचालगामी और उगते सूरज को अर्घ्य अर्पित कर सके. यमुना की त्रासदी देखिए कि नाला बन चुकी उसी नदी के किनारे भारतवर्ष की सत्ता निवास करती है, न्याय का दंड लिए उच्चतम न्यालय और ग्रीन ट्राइब्यूनल भी मौजूद हैं, पर सब कई दशकों से दिल्ली वालों द्वारा यमुना को पूजने के साथ-साथ नदी को नाला बनते देखने को मजबूर हैं.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. यह ज़रूरी नहीं है कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ़ लेखक ही ज़िम्मेदार हैं.]
 “ Opinion: निर्मला के बजट से न सिर्फ मिडिल क्लास और उद्योग को फायदा होगा, बाहर जा रहा निवेश भी रुकेगा
“ Opinion: निर्मला के बजट से न सिर्फ मिडिल क्लास और उद्योग को फायदा होगा, बाहर जा रहा निवेश भी रुकेगा

ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस