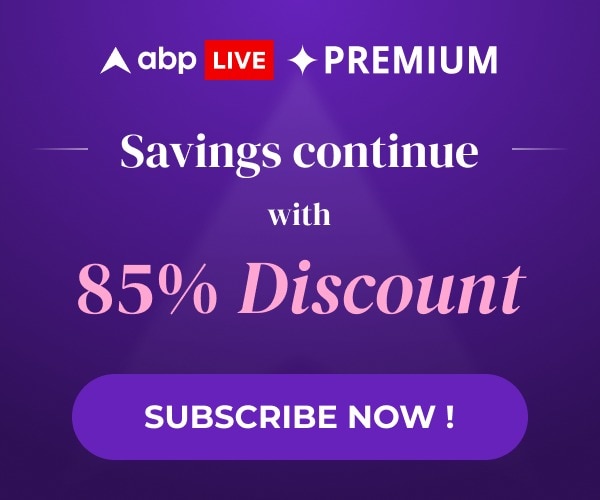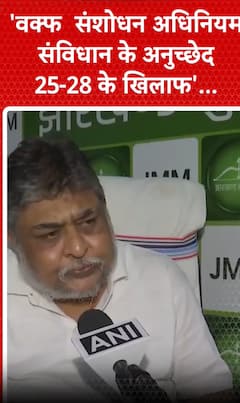यूनिफॉर्म सिविल कोड: मोदी सरकार की मंशा पर सवाल, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का मुद्दा नहीं, समाज कितना है तैयार

जब से 22वें विधि आयोग ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता पर रायशुमारी शुरू की है, तब से इस पर सामाजिक-राजनीतिक बहस काफी तेज़ हो गई है. सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर पक्ष और विपक्ष में तर्क सामने आ रहे हैं.
इस बीच 3 जुलाई को कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक हुई. इस बैठक से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं. ऐसी खबरें आ रही हैं कि बैठक में समिति के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने जोर दिया है कि समान नागरिक संहिता को देश के आदिवासी समुदाय से अलग रखा जामा चाहिए. जैसी खबरें आई हैं, उसके मुताबिक सुशील मोदी का कहना है कि हर कानून का अपवाद होता है और चूंकि आदिवासी समुदाय के लोगों के रीति-रिवाज अलग हैं, इसलिए यूसीसी के दायरे में इन्हें नहीं लाया जाना चाहिए. कहा जा रहा है कि बैठक में सुशील मोदी का मुख्य ज़ोर उत्तर-पूर्व राज्यों के आदिवासियों को इसके दायरे से बाहर रखने पर था.
वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सासंदों ने बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जारी कवायद की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं. इन सांसदों का कहना है कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी इस मुद्दे के जरिए राजनीतिक लाभ लेना चाहती है.
इन सबके बीच नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर भी सवाल उठता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 जून को भोपाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि एक ही परिवार में दो लोगों के लिए अलग-अलग नियम नहीं हो सकते. उन्होंने इतना तक कहा था कि वोट बैंक के भूखे लोगों की वजह से इसमें अड़ंगा लगते रहा है.
संसदीय स्थायी समिति की बैठक में अगर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने ये कहा है कि आदिवासियों को यूसीसी से दूर रखा जाए, तो फिर इससे नरेंद्र मोदी सरकार की 'एक देश एक कानून' की बात में कितना दम रह जाएगा. अगर आदिवासियों को इससे बाहर रखने का मन सरकार बनाती है, तो फिर इससे सरकार की असल मंशा पर भविष्य में और भी सवाल उठेंगे.
2011 की जनगणना के मुताबिक देश में अनुसूचित जनजाति (ST) की संख्या लगभग 10.4 करोड़ है. देश की जनसंख्या में एसटी समुदाय के लोगों की हिस्सेदारी करीब 8.6% है. अब इनकी संख्या और भी ज्यादा होगी. अनुमान के मुताबिक अब इनकी संख्या 13 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत 730 से ज्यादा जातीय समूह अनुसूचित जनजाति के तौर पर अधिसूचित हैं. भारत में फिलहाल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. इनमें से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ को छोड़ दिया जाए, तो हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में आदिवासी समुदाय नोटिफाइड हैं.
भारत में आदिवासियों की संख्या के हिसाब से दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र हैं-सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न एरिया. दो तिहाई से ज्यादा आदिवासी 7 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, झारखंड और छत्तीसगढ़ में रहते हैं. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी इनकी अच्छी-खासी संख्या है. इसके अलावा उत्तर-पूर्व के राज्यों सिक्किम, असम, नगालैंड. मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की हिस्सेदारी काफी है. नगालैंड और मेघालय में तो 86 फीसदी से ज्यादा आबादी अनुसूचित जनजाति है.
अब सवाल उठता है कि अगर इतनी बड़ी आबादी को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बाहर रखा जाएगा, तो फिर पर्सनल लॉ के मामलों में 'एक देश एक कानून' की अवधारणा का औचित्य नहीं रह जाएगा. हालांकि संविधान में ही ये व्यवस्था है कि कई केंद्रीय कानून पूर्वोत्तर राज्यों की सहमति के बिना वहां लागू नहीं होते. लेकिन अगर सचमुच में आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाता है तो फिर चंद राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर तकरीबन पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का अपवाद मौजूदा रहेगा.
अगर ऐसा ही है तो फिर मुस्लिम समुदाय की ओर से भी वहीं आपत्ति जताई जा रही है, जो आदिवासियों को लेकर सुशील मोदी जैसे बीजेपी के कुछ नेताओं की राय है. आदिवासियों को यूसीसी के दायरे से बाहर रखने के विचार के पीछे यही दलील दी जा रही है कि देश में एक तो आदिवासियों के कई अलग-अलग समूह हैं और उन समूहों में भी विवाह और पर्सनल लॉ से जुड़े कई मामलों में अलग-अलग मान्यताएं और रिवाज हैं. उनके नियम रूढ़ी परंपरा के लिहाज से तय होते हैं. कई आदिवासी संगठनों ने कहा भी है कि यूसीसी की वजह से आदिवासियों की पहचान खतरे में पड़ जाएगी.
2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में मुस्लिमों की जनसंख्या 17.22 करोड़ थी और देश की आबादी में उनकी हिस्सेदारी 14.2% थी. अब इनकी संख्या 20 करोड़ से ज्यादा हो गई होगी. यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सबसे सबसे ज्यादा एतराज इसी समुदाय से आ रहा है. इस समुदाय के लोगों का कहना है कि वे सदियों से पर्सनल मामलों में खुद के धर्म के मुताबिक रिवाजों को मानते आए हैं और यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए उनसे इस अधिकार को छीन लिया जाएगा.
अगर आदिवासियों की इतनी बड़ी आबादी को यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाता है, तो फिर मुस्लिम समुदाय के लोग भी उसी पैमाने से खुद को मापने के मुद्दा को भविष्य में और मजबूती से उठा सकते हैं. आदिवासियों के साथ ही मुस्लिम आबादी को मिला दिया जाए, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की करीब 23 फीसदी आबादी को यूनिफॉर्म सिविल कोड से सबसे ज्यादा एतराज है या हो सकता है. ये संख्या इतनी ज्यादा है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बगैर उनकी सहमति से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना देश के सामाजिक ताना-बाना को बिगाड़ सकता है.
ये बात भी सही है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं धर्म के आधार पर चल रहे पर्सनल लॉ की वजह से हिंसा और भेदभाव का शिकार हो रही है. इस समुदाय में महिलाओं को तलाक के अलग-अलग रूपों, बहुविवाह और हलाला जैसी प्रथाओं का दंश झेलना पड़ रहा है. हालांकि बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के भी इन सबसे निपटा जा सकता है. जैसे कुछ साल पहले एक बार में तीन तलाक (तलाक ए बिद्दत) को सुप्रीम कोर्ट से अवैध ठहराए जाने के बाद संसद से कानून बनाकर अपराध घोषित किया गया था.
ये बात सही है कि संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य, भारत के समस्त राज्य क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा. हालांकि ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि समान नागरिक संहिता को संविधान के भाग 3 के तहत मूल अधिकार से जुड़े हिस्से में शामिल नहीं कर राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल किया गया था. इसकी वजह से ये प्रावधान राज्य के ऊपर बाध्यकारी नहीं रह गए.
ये भी तथ्य है कि जब संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा में बहस चल रही थी, तो उस वक्त भी समान नागरिक संहिता पर व्यापक बहस हुई थी. संविधान निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर भी समान नागरिक संहिता के समर्थन में थे. अंबेडकर का तर्क था कि देश में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिहाज से धार्मिक आधार पर बने नियमों में सुधार बेहद जरूरी है. हालांकि उस वक्त देश के हालात को देखते हुए इसे नीति निदेशक तत्वों में शामिल कर सरकार को हर कीमत पर लागू करने की संवैधानिक बाध्यता से बचा लिया गया था.
ऐसा नहीं है कि अब देश में हालात बदल गए हैं. जिन परिस्थितियों की वजह से उस वक्त यूनिफॉर्म सिविल कोड को मूल अधिकार के हिस्से में नहीं रखा गया था, वो हालात आज भी मौजूद हैं. देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू मुस्लिम नेताओं के भारी विरोध के कारण समान नागरिक संहिता पर आगे नहीं बढ़े.
हालांकि 1954-55 में भारी विरोध के बावजूद जवाहर लाल नेहरू हिंदू कोड बिल लेकर आए. हिंदू विवाह कानून 1955, हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण कानून 1956 और हिंदू अवयस्कता और संरक्षकता कानून 1956 लागू हुए. इससे हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख समुदायों के लिए शादी, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे नियम संसद में बने कानून से तय होने लगे. लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसियों को अपने -अपने धार्मिक कानून के हिसाब से शादी, तलाक, उत्तराधिकार जैसे मुद्दे को तय करने की छूट बरकरार रही.
बीजेपी के पार्टी के तौर पर गठन से पहले ही भारतीय जनसंघ ने 1967 के आम चुनाव में अपने घोषणापत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का स्पष्ट जिक्र किया था. अप्रैल 1980 में बीजेपी की स्थापना होती है और जैसे-जैसे पार्टी का दायरा बढ़ता है, समान नागरिक संहिता की मांग भी तेजी से राजनीतिक मुद्दा बनने लगता है. पहली बार 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता को जगह दी. 2014 और 2019 के घोषणापत्र में भी बीजेपी ने इसे शामिल किया. पार्टी गठन के बाद से बीजेपी के लिए तीन बड़े वादे और मुद्दे रहे हैं. इनमें से अनुच्छेद 370 और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का वादा पूरा हो गया है. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा बाकी है.
पिछले डेढ़ साल से बीजेपी राज्यों के जरिए इस मुद्दे को आगे बढ़ा रही थी, लेकिन जिस तरह से पिछले महीने 22वें विधि आयोग ने यूसीसी पर देश की जनता और संस्थाओं से विचार मांगने की शुरुआत की, उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकता है. कर्नाटक में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद अब केंद्रीय स्तर पर यूसीसी को लेकर कोशिशें आगे बढ़ाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 27 जून को भोपाल में इस पर बयान देने से भी ऐसा ही संकेत मिल रहा है. ये एक ऐसा मुद्दा है, जिसकी काट खोजना विपक्षी दलों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है.
अब सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से क्या सिर्फ़ आदिवासियों, मुस्लिमों, ईसाइयों और पारसियों से जुड़े निजी कानूनों पर ही असर पड़ेगा. इसका सीधा सा जवाब है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. जब सही मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश और हर नागरिक के लिए लागू किया जाएगा तो उससे हिन्दुओं से जुड़े विवाह कानून, उत्तराधिकार कानून, उत्तराधिकार और गोद लेने से जुड़े कानूनों में भी बदलाव करना होगा.
नरेंद्र मोदी सरकार का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद देश में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में किसी धर्म, लिंग या लैंगिक झुकाव के बिना हर नागरिक पर एक तरह का कानून लागू होगा. हालांकि सरकार की ओर से अभी ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि वो कानून कैसा होगा, उसमें क्या-क्या प्रावधान होंगे.
21वें विधि आयोग ने भी इस मुद्दे पर देशभर के अलग-अलग लोगों और संस्थाओं से चर्चा कर. अगस्त 2018 में जारी परामर्श पत्र में कहा था कि फिलहाल देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की जरुरत नहीं है. आयोग ने कहा था कि मौजूदा वक्त में यूनिफॉर्म सिविल कोड न तो जरुरत है और न ही वांछनीय.
अब 22वां विधि आयोग इस मसले पर रायशुमारी तो जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी ओर से भी उस रायशुमारी के फॉर्मेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड के किसी भी तरह की रूपरेखा का जिक्र नहीं है. आयोग ने संबंधित पक्षों और देश के लोगों से अपने मनमुताबिक राय देने को कहा है. अब आम नागरिक विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने की जटिल प्रक्रिया में आमूलचूल बदलाव से जुड़े यूनिफॉर्म सिविल कोड पर किस तरह से अपना विचार रख पाएंगे और रखेंगे भी तो कानूनी लिहाज से उसकी कितनी सार्थकता होगी, इस पर गंभीरता से विचार करने से जरूरत है.
शायद यही वजह है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के साथ ही अलग-अलग समुदाय के संगठनों की ओर से भी नरेंद्र मोदी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. अगर केंद्र सरकार सही मायने में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर गंभीर है और उस पर देश की जनता और अलग-अलग समुदायों का राय जानना चाहती है, तो होना ये चाहिए था कि सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत क्या-क्या रहेगा, उसका कोई मसौदा तैयार करना चाहिए था. उसके बाद ही उस बारे में जनता और अलग-अलग समुदायों से उनकी राय जाननी चाहिए थी.
धार्मिक मामलों से जुड़े होने के कारण ये मुद्दा काफी संवेदनशील है और कानूनी पहलू से जुड़े होने के कारण ये मुद्दा जटिल भी है. इसलिए यूसीसी का मसौदा सामने रहने पर उस पर राय देना ज्यादा सार्थक होता. अभी जो भी विचार या सलाह विधि आयोग को मिल रहे हैं, उसका आधार यूसीसी के हर पहलू को समझने से ज्यादा देश में राजनीतिक और धार्मिक तरीके से बने माहौल पर टिका नज़र आ रहा है.
अगर सचमुच पर्सनल मामलों, फैमिली लॉ में एकरूपता लानी है, तो इसके लिए व्यापक सहमति बनाने की जरूरत है. देश के हर नागरिक पर इसका असर पड़ने वाला है. धार्मिक और पारिवारिक पहलुओं से जुड़े मामलों में कानूनी तरीके से एकरूपता लाना यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद होता है.
अगर देश के अलग-अलग समुदायों में इस पर सहमति बनाए बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू भी कर दिया जाता है, तो हमारे सामने कई ऐसे उदाहरण हैं, जो ये बताते हैं कि सिर्फ कानून बनाकर ही सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं को नहीं बदला जा सकता है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो यही है कि हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत लड़कियों के लिए शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों के लिए न्यूनतम उम्र 21 साल निर्धारित है, इसके बावजूद अभी भी हिंदुओं में भी बड़े पैमाने पर लड़के और लड़कियों दोनों की इससे कम उम्र में विवाह हो रहा है और कानूनी तौर से उन विवाहों को अवैध भी नहीं माना जाता है.
इस तरह के कई उदाहरण भरे पड़े हैं. हिन्दुओं में एक पत्नी के रहते दूसरी शादी पर रोक है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, जिन्होंने दो शादियां की हैं. कानूनन ये अपराध है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऐसे मामले सामने आते रहे हैं. उसी तरह से दहेज की बुराई भी विवाह से ही जुड़ी हुई है और कानूनन ये अपराध है, इसके बावजूद भारतीय समाज के अलग-अलग हिस्सों में अभी भी इसका चलन है. उसी तरह से दक्षिण भारत के कुछ हिन्दू समुदाय में रिश्तेदारों के बीच शादियों का चलन है, जबकि हिन्दू मैरिज एक्ट के तहत दोनों पक्षों की कुछ पीढ़ियों के बीच इस तरह के विवाह पर रोक है.
उसी तरह से 2005 के बाद से हिन्दुओं में महिलाओं को संपत्ति में कानूनन तो समान अधिकार हासिल है, लेकिन व्यवहार के स्तर पर ये कितना लागू है, ये हम सब जानते हैं. हिन्दुओं के पास हिन्दू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family)के तौर पर अलग कानूनी और टैक्स इकाई बनाने का अधिकार है. इस सुविधा का धड़ल्ले से इस्तेमाल टैक्स बचाने के लिए होता आ रहा है. यानी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने से देश का हर नागरिक पर्सनल मामलों में उसे माने ही.
यूसीसी से चुनाव में तो ध्रुवीकरण को बढ़ावा मिल सकता है, जैसा कि कई राजनीतिक विश्लेषक बार-बार कह भी रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर्सनल लॉ में भेदभाव खत्म करने से जुड़ा मुद्दा है. ऐसे में सभी समुदाय को भरोसे में लेकर ही इस पर आगे कदम बढ़ाने की जरूरत है. इसे बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है.
ये सिर्फ़ राजनीतिक सहमति बनाने या संसद में किसी तरह से कानून पारित कराने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए. इस नजरिए से सत्ताधारी दलों के साथ ही विपक्षी दलों की भूमिका भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है. ऐसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा वास्तविक है, लेकिन जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है और इस मसले पर ध्रुवीकरण हो रहा है, उसको देखते हुए ये मुद्दा वास्तविक से ज्यादा सियासी नज़र आ रहा है.
[नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज़ ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.]
 “ Health Day Special: मोबाइल फोन और बच्चों की आंखों की सेहत, बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या और उपाय
“ Health Day Special: मोबाइल फोन और बच्चों की आंखों की सेहत, बढ़ती स्क्रीन टाइम की समस्या और उपाय

ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस