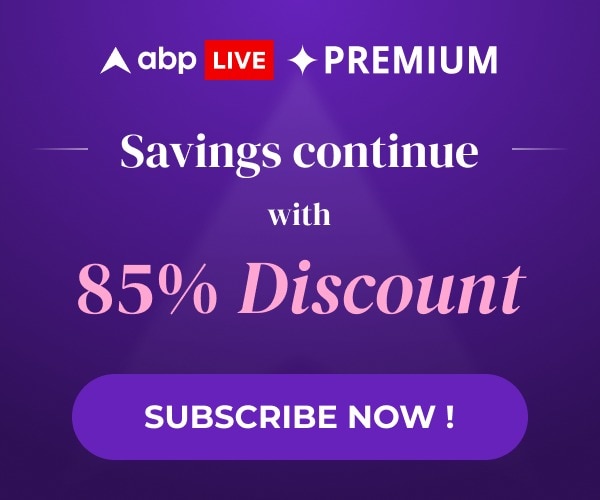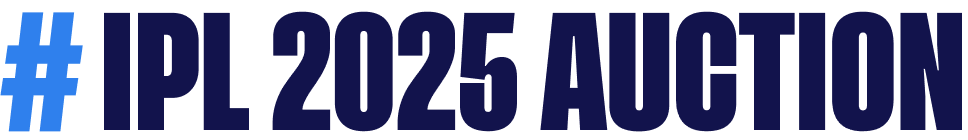चुनावों से पहले ही आखिर क्यों सजती है, नफ़रत फैलाने की मंडी?

कभी आपने सोचा है कि जब देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव सिर पर होते हैं,तब उन प्रदेशों में अमन व भाईचारे की बहती फ़िज़ा में अचानक कौन नफ़रत और सांप्रदायिकता का ज़हर घोल देता है?आख़िर वे कौन-सी ऐसी ताकतें हैं,जो नक़ाब या मुखौटे ओढ़कर सिर्फ अपनी सियासत की ख़ातिर एक पूरी कौम को ही खलनायक साबित करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं? इसके लिए किसी एक समुदाय के लोगों को ही पूरी तरह से क़सूरवार ठहराना उचित इसलिये नहीं होगा कि नफ़रत की इस चिंगारी को दोनों तरफ़ से ही समान रुप से भड़काया जा रहा है.इसके लिए किसी खास धर्म या मज़हब की बहुमत जनता को भी क़सूरवार नहीं मान सकते क्योंकि वो कभी भी ऐसी हिंसा करने वालों की न हमदर्द बनती है और न ही उनका साथ ही देती है,भले ही वे किसी भी धर्म से नाता रखते हों.
गौर करने वाली बात ये है कि किसी एक प्रदेश में वही चिंगारी अल्पसंख्यकों के लिए शोला बनकर सामने आ रही है,तो कहीं बहुसंख्यकों को इस आग में झुलस जाने का खतरा नज़र आ रहा है.लिहाज़ा,सियासत की इस शतरंजी चाल में फंसे मासूम व बेगुनाह लोग तो ये भी नहीं जानते कि आखिर वे किसका मोहरा बन रहे हैं और इससे उनकी ज़िंदगी पहले के मुकाबले और ज्यादा बेहतर या खुशहाल कैसे हो जायेगी?
हालांकि हमारे देश में किसी भी चुनाव से पहले धार्मिक तुष्टिकरण का कार्ड खेलकर सत्ता में आना या फिर उसे बचाकर रखने का सियासी शग़ल बहुत पुराना है,लिहाज़ा इसके लिए किसी भी एक राजनीतिक पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता. देश के विभाजन के बाद हुए पहले आम चुनाव को छोड़ दें,तो दूसरे लोकसभा चुनाव के वक़्त से ही अल्पसंख्यकों को लुभाने और उनके वोट बटोरने के लिए तुष्टीकरण की शुरुआत हो गई थी.अगले कई चुनावों में भी ये तिकड़म कामयाब हुई और देश की सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में बरकरार रहने का लगातार रिकॉर्ड बनाती रही.
लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में धार्मिक ध्रुवीकरण की आड़ में एक नई शुरुआत ये हुई है कि अल्पसंख्यकों को न सिर्फ हर तरीके से डराया-धमकाया जाए बल्कि बहुसंख्यक समुदाय में उनके ख़िलाफ़ नफ़रत का ऐसा जहर भी घोला जाए कि शिक्षित हिन्दू वर्ग भी उनसे घृणा करने लगे.वे कहते हैं कि सियासत का ये औजार किसी एक खास पार्टी के लिए फायदेमंद साबित तो हो रहा हैलेकिन इसके दूरगामी नतीजे बेहद विस्फोटक हो सकते हैं,जिसकी कल्पना हम आज नहीं कर सकते हैं. कुल मिलाकर भारत जैसे उदारवादी,सहिष्णु और सेक्युलर राष्ट्र की सेहत के लिए इसे शुभ संकेत नहीं माना जा सकता. सियासी इतिहास में 1989 ऐसा साल था,जब कांग्रेस से बग़ावत करके जनता दल बनाने वाले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सत्ता हासिल करने के लिए कोई धार्मिक
कार्ड नहीं बल्कि समूचे समाज को वर्ग और जातियों में बांट देने वाला आरक्षण का ऐसा ब्रहमास्त्र निकाला कि उन्हें पीएम की कुर्सी तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाया.हालांकि तब अटल-आडवाणी वाली बीजेपी ने उस सरकार को बाहर से समर्थन देकर वीपी सिंह के उस सपने को पूरा किया था.लेकिन थोड़े वक़्त बाद ही उस जमाने के बीजेपी के दिग्गजों को समझ आ गया कि अगर वीपी सिंह सरकार की नीतियों का ऐसा ही समर्थन करते रहे,तो फिर बीजेपी तो केंद्र की सत्ता में ही नहीं आ पायेगी.
उसके बाद ही बीजेपी ने 'मंडल बनाम कमंडल' का नारा देते हुए देश के बहुसंख्यक समुदाय को एकजुट करने का संकल्प लिया और राम मंदिर निर्माण के आंदोलन को धार देने के लिए पार्टी के दिग्गज़ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली.देश के राजनीतिक इतिहास में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने की वो पहली और सबसे बड़ी कोशिश थी.बेशक 1991 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली लेकिन पार्टी अपने उस एजेंडे से जरा भी नहीं भटकी और 1996 के आम चुनाव में वह लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरी.अगर एक सहयोगी दल के सदस्य ने गद्दारी न की होती,तो तब महज़ एक वोट से 13 दिन में ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार
न गिरी होती,बल्कि शायद पांच साल का कार्यकाल पूरा करती.लेकिन पुरानी कहावत है कि किसी बैसाखी के सहारे कोई भी सत्ता बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं टिकती.वही कड़वा स्वाद अटलजी को भी चखना पड़ा लेकिन न उन्होंने और न ही पार्टी ने हिम्मत हारी और 1998 के आम चुनाव के बाद बीजेपी फिर सबसे बड़ी पार्टी तो बन गई लेकिन 13 महीनों के भीतर ही उन्हें अन्नाद्रमुक नेता और तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने धोखा दे दिया और अटल सरकार दोबारा गिर गई. लेकिन 1999 में जब वो तीसरी बार सत्ता में आई,तो 2004 तक हुकूमत में रहते हुए और उसके बाद हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने वोटों के ध्रुवीकरण की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया. उसके सत्ता से बाहर की एक वजह ये भी हो सकती है लेकिन इसके अलावा भी और कई वजहें रही थी
लेकिन साल 2014 से राजनीति में नए प्रयोग होने की जो शुरुआत हुई, वो देश की बहुसंख्यक आबादी को रास भी आ रही है और वे इसका खुलकर समर्थन भी कर रही है.लिहाज़ा, किसी भी देश का मीडिया ये कभी तय नहीं कर सकता कि वहां के लोग नफ़रत भरा समाज आखिर क्यों बनाना चाहते हैं और उसमें जिंदगी जीना उन्हें क्यों मंजूर है? मीडिया तो अपनी जनता के लिए सिर्फ वही भूमिका निभाता है कि वो एक प्यासे घोड़े को किसी नदी-तालाब तक तो ले जा सकता है लेकिन वह उसे जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकता. बदकिस्मती से हमारे देश का भी आज कुछ वही हाल है!
नोट- उपरोक्त दिए गए विचार लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं. ये जरूरी नहीं कि एबीपी न्यूज ग्रुप इससे सहमत हो. इस लेख से जुड़े सभी दावे या आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक ही जिम्मेदार है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस