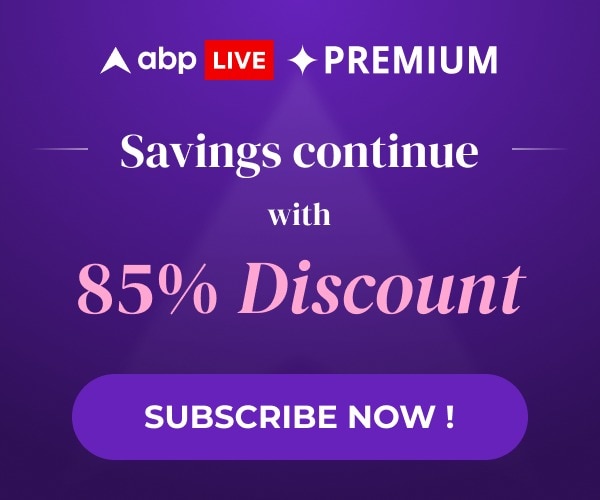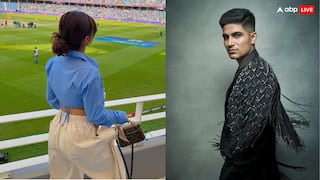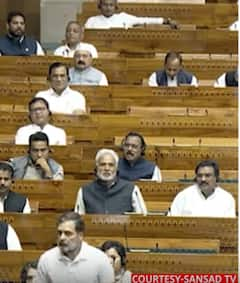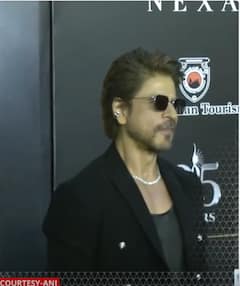कहीं लिव-इन रिलेशन, तो कहीं मेले में प्यार का इजहार...,आदिवासियों की परंपराओं में कैसे फिट होगा UCC
आदिवासी समाज में कई ऐसी प्रथाएं हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती हैं. यही कारण है कि कई आदिवासी संगठन ऐसे भी हैं जो केंद्र के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की यात्रा से लौटने के बाद ही समान नागरिक संहिता को देश भर में लागू करने की वकालत करनी शुरू कर दी थी. जिसके बाद विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं आने लगीं और कुछ ही दिनों में यह मुद्दा देश भर में बहस का मुद्दा बन गया है.
केंद्र के इस कदम का सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समाज और आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं. कई आदिवासी संगठन ऐसे भी हैं जो केंद्र के इस कदम का जमकर विरोध कर रहे हैं. उन्हें लग रहा है कि अगर यह कानून लागू होता है तो उनके रीति-रिवाजों पर भी इसका असर पड़ेगा.
दरअसल आदिवासी समाज में भी कई ऐसी प्रथाएं हैं, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में आने से खत्म हो सकती हैं. उदाहरण के तौर पर इस समाज में एक पुरुष एक साथ कई महिलाओं से शादी कर सकता है या एक महिला कई पुरुषों से शादी कर सकती है. इसके अलावा आदिवासी समुदाय में शादी से पहले लिव-इन में रहने की भी प्रथाएं हैं.
हालांकि समान नागरिक संहिता पर बीते सोमवार संसदीय समिति की बैठक हुई थी जिसमें बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने सुझाव दिया था कि अनुसूचित जाति एवं पूर्वोत्तर राज्यों से संबंधित कानून प्रस्तावित यूसीसी के दायरे से बाहर रखे जाएं. ऐसे में इस रिपोर्ट में जानते हैं कि आखिर आदिवासियों की शादियों की परंपरा सामान्य परंपरा से कितनी अलग है और यूसीसी का इनपर क्या असर पड़ेगा
आदिवासी यानी ST होते कौन हैं?
आदिवासी को मूलनिवासी, वनवासी, गिरिजन, देशज, स्वदेशी जैसे अनेक नामों से जाना जाता है. आदिवासी का मतलब है ऐसे वासी जो बहुत शुरुआत से ही यहां रह रहे हैं. सरकारी और कागज़ी तौर पर आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है.
अनुसूचित जनजातियां (एसटी) समूह आमतौर पर मुख्यधारा के समाज से अलग रहते हैं. अनुसूचित जनजातियों का समाज और इनके रीति-रिवाज आम लोगों से काफी अलग होते हैं.
आदिवासी समाज अपने नियम- कानून बनाते हैं और उसे मानते भी हैं. ये समुदाय किसी भगवान को नहीं मानते, उनके लिए प्रकृति ही सब कुछ है. आमतौर पर आदिवासी समाज जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं.
भारत में कुल 705 आदिवासी समुदाय हैं जो देश में सरकारी तौर पर एसटी यानी अनुसूचित जनजातियों के रूप में लिस्टेड हैं. साल 2011 में हुए जनगणना के अनुसार, भारत में आदिवासियों की कुल आबादी 10.43 करोड़ के करीब है. यह देश की कुल आबादी का 8% से ज्यादा है. इनमें से कुछ ज्यादातर आदिवासी समुदाय छत्तीसगढ़ तो कुछ झारखण्ड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान में रहते हैं.
आदिवासी समुदाय में क्या है शादी की परम्परा
आदिवासी समुदायों के रीति रिवाज और उनकी भाषा क्षेत्र दर क्षेत्र बदलती रहती है. जिसके कारण आदिवासी समुदायों में होने वाली शादियों की रस्में भी क्षेत्र के हिसाब से बदल जाती है.
भील जनजाति
गुजरात और राजस्थान में रहने वाले आदिवासी समुदायों के जोड़े शादी के वक्त उल्टे फेरे लेते हैं. इस रस्म के पीछे की वजह है धरती का उल्टा घूमना. उनका मानना है कि क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी को प्रकृति के अनुसार जाते हैं इसलिए रस्में भी प्रकृति के सम्मान में ही निभाई जानी चाहिए.
भील जनजाति के लोग किसी अन्य जनजाति, जाति, धर्म में शादी तो कर सकते हैं लेकिन अपने गोत्र में शादी करना बिल्कुल मना है. ऐसा करने पर उन्हें जनजाति से बाहर कर दिया जाता है. इन लोगों का शादी की सूचना देने का तरीका भी बहुत ही अलग है.
दरअसल यहां अगर किसी के घर में शादी होने वाली है तो वह परिवार अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर चावल और गेहूं के कुछ दाने रख देते हैं. इन दानों को देखकर लोग अपने आप ही समझ जाते हैं कि इस घर में किसी का रिश्ता तय हो गया है. भील जनजाति में शादी की रस्में 3 से 4 दिनों के बीच पूरी हो जाती है.
यह अनोखी रस्म भी है प्रख्यात
आदिवासी समुदाय में “चांदला” रस्म भी काफी लोकप्रिय है. इसमें आदिवासी समुदाय के लोग शादी वाले घर में यानी लड़के और लड़की के घर वालों को पैसे देकर उनकी आर्थिक मदद करते हैं.
दरअसल समुदाय के सारे लोग अपने हिसाब से कुछ रुपये देकर शादी वाले परिवार की आर्थिक मदद करते हैं. वहीं लड़की और लड़के के घर वाले इन सारी राशियों को एक जगह लिख लेते हैं ताकि जब उनके घर कोई शादी हो तो वह भी उनकी मदद कर सकें. इस तरह से आदिवासियों की शादी में दहेज नहीं होता, बल्कि दोनों परिवार मिलकर सभी तैयारियां करते हैं.
मीणा जनजाति
राजस्थान की मीणा जनजातियों में सांस्कृतिक तौर पर एक मेला लगाया जाता है. इस मेले में उसी समुदाय के लड़के और लड़कियां पहुंचते हैं. मेले में युवक- युवती एक दूसरे के साथ कई तरह के खेल खेलते हैं. आपस में मिलते-जुलते हैं और इसी क्रम में अगर वह एक-दूसरे को पसंद आ गए, तो दोनों की शादी करवा दी जाती है.
हालांकि इस रिवाज में भी अंतिम फैसला घर के बड़े यानी माँ-बाप का ही होता है. शादी से पहले और मेले में पसंद कर लेने के बाद, लड़का कुछ दिनों तक लड़की के घर में ही रहता है, ताकि लड़की के पिता बेटी के होने वाले पति की योग्यताओं को देख लें परख लें. इस बीच अगर घर वालों को किसी कारण से लड़का पसंद नहीं आ रहा हो, तो वह दोनों शादी नहीं कर सकते हैं.
मीणा जनजाति में फेरे के वक्त समय, लड़की के माता-पिता मंडप पर नहीं बैठ सकते. इसके पीछे मान्यता है कि यह जोड़े की खुशी के लिए ज़रूरी है. ताकि उनका दांपत्य जीवन सुखी रहे.
छत्तीसगढ़ में शादी से पहले होती है ‘लीव इन रिलेशन’ जैसी रस्में
भारतीय संस्कृति में शादी से पहले एक साथ रहना या सम्बन्ध बनाना आम बात नहीं है. लेकिन छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों की माड़िया जाति शादी से पहले घोटुल नाम के रस्म को निभाता है. घोटुल में आने वाले लड़के-लड़कियों को अपना जीवनसाथी चुनने की छूट होती है.
इस रस्म में लड़का-लड़की शादी से पहले एक साथ एक घर में रह सकते हैं और शारीरिक सम्बन्ध भी बना सकते हैं. इस रस्म को खास तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और साउथ के कुछ इलाकों में मनाया जाता है. इस रस्म को करने के लिए 10 से अधिक उम्र होनी चाहिए.
इस रस्म के दौरान अगर किसी लड़के को किसी लड़की को अपनी तरफ आकर्षित करना होता है, तो वह उसके लिए एक कंघी अपने हाथों से बनाता है.
झारखंड में शादी करने के 12 तरीके
झारखण्ड की एक जनजाति है संताल. यहां पूरे 12 तरीकों से शादियां हो सकती हैं. उनमें से एक तरीके का नाम है “सादय बपला". इस तरीके से शादी करने में दोनों परिवारों की रज़ामंदी बेहद जरूरी होती है. दूसरे तरह के विवाह को “घरदी जवाय” कहा जाता है. इस तरीके से शादी तभी होती है जब लड़की का भाई नाबालिग हो. लड़का अपनी लड़की के भाई के बालिग होने तक लड़की के घर में ही रहता है. जिसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौट जाता है.
झारखंड में आदिवासी विवाह के एक और तरीके का नाम है “हीरोम चेतान बापला” है. इस रस्म में लड़का पहली पत्नी के होते हुए दूसरी लड़की या महिला से विवाह कर सकता है. लेकिन ऐसा करने से पहले उसे पहली पत्नी की मंजूरी मिलनी चाहिए. इस समुदाय के नियमों के अनुसार पुरुष तब ही दूसरी शादी कर सकता है जब पहली पत्नी से कोई संतान न हो और अगर हो भी तो सिर्फ लड़की हो.
यूनिफॉर्म सिविल कोड का आदिवासी विरोध क्यों कर रहे हैं?
शादी की रस्मों के अलावा भी असम, बिहार और ओडिशा की कुछ जनजातियां उत्तराधिकार के परंपरागत कानूनों का पालन करते हैं.
इसके अलावा मेघालय में कुछ जनजातियों में मातृसत्तात्मक सिस्टम है. इस नियम के अनुसार माता पिता की कुल संपत्ति सबसे छोटी बेटी को विरासत में मिलती है. ऐसा ही एक समुदाय है गारो जनजाति. इसमें शादी के बाद पुरुष लड़की के घर पर ही रहता है. वहीं कुछ नगा जनजातियों में महिलाओं को संपत्ति विरासत में देने या जनजाति के बाहर शादी करने पर प्रतिबंध है.
आदिवासियों को डर है कि अगर यूसीसी के तहत सभी जाति, समुदायों के लिए एक कानून बनता है तो आदिवासियों की सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में नहीं रखा जाएगा.
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार आदिवासियों का कहना है कि उनके कानून संवैधानिक रूप से संहिताबद्ध नहीं हैं और उन्हें इस बात का डर है कि देश में अगर यूसीसी लागू होता है तो उनकी प्राचीन पहचान को कमजोर कर देगा. भारत में रहने वाले 750 आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक विविधता के लिए खूब जाने जाते हैं.
सर्व आदिवासी समाज के प्रमुख आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि आदिवासी समुदाय, भविष्य की रणनीति के लिए बैठक करने की तैयारी कर रहा है. साल 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की 32 प्रतिशत आबादी आदिवासी समुदाय है, जो कुल 2.55 करोड़ में से 78 लाख लोग हैं. बिना उनका पक्ष लिए, इस कानून पर चर्चा गलत है.
समान नागरिक संहिता क्या है?
समान नागरिक संहिता एक देश एक कानून के विचार पर आधारित है. यूनिफॉर्म सिविल कोड आने के बाद देश के हर धर्म, समुदाय के लोगों के लिए एक ही कानून होगा. यूसीसी में संपत्ति के अधिग्रहण और संचालन, विवाह, तलाक और बच्चा गोद लेने जैसे नियम भी सभी धर्म और समुदायों के लिए एक समान होंगे. भारतीय संविधान में आर्टिकल-44 के तहत सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कानून बना सकती है.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस