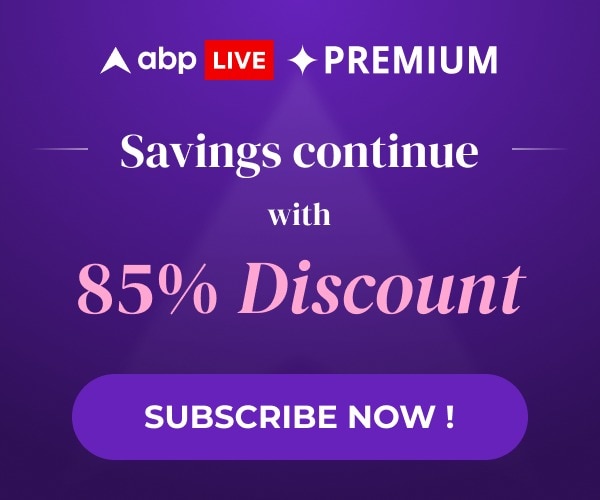Delhi: दिल्ली में तीनों नए आपराधिक कानून लागू, ये IPC-CRPC और एविडेंस एक्ट से कैसे हैं अलग?
New Criminal Law Delhi: तीनों नए कानून भारतीय दंड संहिता (IPC), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की जगह लेंगे.

New Criminal Law Latest News: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार (एक जुलाई 2024) से तीन नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं. इसके लिए दिल्ली पुलिस पहले से ही तैयारियों में जुटी हुई थी. पिछले कई महीनों से पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा था. अब तक करीब 25 हजार पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है. अब पुलिसकर्मियों को नए कानून के मुताबिक ही काम करना होगा.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक तीनों नए कानून वर्तमान में लागू ब्रिटिश काल के भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) की जगह लेंगे. इन नए कानून के नाम भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) हैं. इस साल फरवरी महीने में इन तीनों आपराधिक कानूनों को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था. नए कानूनों के लागू होने से कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे.
14 सदस्यीय समिति गठित
दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘नए कानूनों को समझने के लिए उचित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया. प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को नए कानूनों को समझने के लिए पुस्तिका दी गई हैं." जनवरी में कानूनों का अध्ययन करने और पुलिसकर्मियों के लिए अध्ययन सामग्री तैयार करने के लिए स्पेशल सीपी छाया शर्मा के नेतृत्व में एक 14 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था. समिति ने अध्ययन सामग्री तैयार करने के अलावा फरवरी महीने में चरणबद्ध तरीके से पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण को शुरू किया. बीते 15 दिनों में पुलिसकर्मियों ने परीक्षण प्रक्रिया के दौरान ‘डमी एफआईआर’ भी दर्ज की है.
दुष्कर्म के दोषियों को फांसी तक की सजा
नए आपराधिक कानून के अंतर्गत नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषियों को फांसी की सजा तक दी जा सकती है. वहीं, नाबालिग के साथ गैंगरेप करने को नए अपराध की श्रेणी में रखा गया है. जबकि, राजद्रोह को अब अपराध नहीं माना जाएगा. इन नए कानून में मॉब लिंचिंग के दोषियों को को भी सजा के प्रावधान हैं. जब पांच या उससे ज्यादा लोग जाति या समुदाय के आधार पर किसी की हत्या करते हैं तो उन्हें उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी.
भारतीय न्याय संहिता
भारतीय न्याय संहिता (BNS) 163 साल पुराने आईपीसी (IPC) की जगह लेगा. इस कानून के सेक्शन 4 के अंतर्गत सजा के तौर पर दोषी को सामाजिक सेवा करनी होगी. शादी का धोखा देकर यौन संबंध बनाने पर 10 साल की सजा और जुर्माना का प्रावधान है. साथ ही नौकरी या अपनी पहचान छिपाकर शादी के लिए धोखा देने पर भी सजा होगी. संगठित अपराध जैसे अपहरण, डकैती, गाड़ी की चोरी, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, आर्थिक अपराध, साइबर क्राइम के लिए भी कड़े सजा का प्रावधान किया गया है. भारतीय न्याय संहिता (BNS) में राष्टीय सरक्षा को खतरे में डालने वाले काम पर भी कडी सजा दी जाएगी.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 1973 के सीआरपीसी (CRPC) की जगह लेगा. इस कानून के जरिए प्रक्रियात्मक कानून में महत्वपूर्ण बदलाव किये गए हैं. इस कानून के मुताबिक अगर किसी को पहली बार अपराधी माना गया तो वह अपने अपराध की अधिकतम सजा का एक तिहाई पूरा करने के बाद जमानत हासिल कर सकता है. ऐसे में विचाराधीन कैदियों के लिए तुरंत जमानत पाना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि, यह कानून आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपराधियों पर लागू नहीं होगा. इस कानून के अंतर्गत कम से कम सात साल की कैद की सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक जांच अब अनिवार्य हो जाएगा. फोरेंसिक एक्सपर्ट्स अपराध वाली जगह से सबूतों को इकट्ठा और रिकॉर्ड करेंगे. वहीं अगर किसी राज्य में फोरेंसिक सुविधा का अभाव होने पर दूसरे राज्य में इस सुविधा का इस्तेमाल किया जाएगा.
भारतीय साक्ष्य अधिनियम
भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) 1872 के साक्ष्य अधिनियम की जगह लेगा. इस कानून में कई बड़े बदलाव किये गए हैं. इसमें इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को लेकर नियमों को विस्तार से बताया गया है और द्वितीय सबूत को भी शामिल किया गया है. अब तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जानकारी एफिडेविट तक ही सीमित होती थी. पर अब इसके बारे में कोर्ट को विस्तृत जानकारी देनी होगी. कोर्ट को बताना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत में क्या-क्या शामिल है.
1861 से ही प्रभावी थे ये कानून
औपनिवेशिक काल से चले आ रहे इन तीन कानूनों के बारे में वकीलों, न्यायिक पदाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को करीब-करीब सभी जानकारियां याद थीं. वहीं आम जनता भी इसमें से कई कानूनों के बारे में जानती थी, लेकिन अब कानूनों में हुए नए बदलाव के बाद उन लोगों को नए सिरे से सभी कानूनों को बारीकी से जानना होगा.
ट्रेंडिंग न्यूज
टॉप हेडलाइंस